- Home
- ज्ञान विज्ञान
- नयी दिल्ली. क्या पृथ्वी ब्रह्मांड में अकेला ऐसा ग्रह है, जहां जीवन मौजूद है? कैब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से उम्मीद की किरण जगी है कि संभवत: ऐसा नहीं है और पृथ्वी से करीब 120 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा खगोलीय पिंड हो सकता है, जहां जीवन मौजूद हो सकता है। पिछले सप्ताह ‘एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स' में प्रकाशित अध्ययन में के2-18बी नामक सुदूर ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं। लेकिन खगोलविद इसे लेकर संशय में हैं और उनका कहना है कि अध्ययन के परिणामों और कार्यप्रणाली की अन्य शोधकर्ताओं द्वारा भी जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। शोध के अनुसार, ‘एक्सोप्लैनेट' के वायुमंडल पर डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड अणुओं के निशान पाए गए हैं। पृथ्वी पर, ये अणु समुद्री जीवों द्वारा उत्पादित माने जाते हैं। ‘एक्सोप्लैनेट' वे ग्रह होते हैं, जो हमारे सौर मंडल से बाहर, अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं।दिलचस्प बात यह है कि सबसे आम परिकल्पना यह है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई।खगोल भौतिकी और बाह्यग्रहीय विज्ञान के प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन के नेतृत्व वाली अनुसंधान टीम का दावा है कि यह अध्ययन ‘तीन सिग्मा' के महत्व का साक्ष्य प्रदान करता है कि सौरमंडल के बाहर जीवन के सबसे मजबूत संकेत 99.7 फीसदी तक आकस्मिक नहीं हैं। पिछले सप्ताह मधुसूदन ने कहा कि अध्ययन के निहितार्थों के दायरे को देखते हुए, उनकी टीम भविष्य के शोधों में परिणामों की मजबूती से पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईएसईआर), भुवनेश्वर के पृथ्वी एवं ग्रह विज्ञान स्कूल के रीडर जयेश गोयल का मानना है कि अध्ययन के निष्कर्ष एक बड़ा कदम हैं और ‘‘यह बाह्यग्रहों के वायुमंडल और उनके रहने योग्य होने के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है।'' उन्होंने बताया, ‘‘के2-18बी के वायुमंडल पर किए गए अवलोकनों से यह पता चलता है कि उप-नेप्च्यून या सुपर-अर्थ एक्सोप्लैनेट की इस श्रेणी को किस हद तक चिह्नित किया जा सकता है, क्योंकि इन लक्ष्यों का अध्ययन करना बेहद चुनौतीपूर्ण है।'' अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में नासा सागन फेलो रयान मैकडोनाल्ड ने ‘ बताया, ‘‘यह बाह्यग्रह विज्ञान के सामान्य मानकों के अनुसार 'पता लगाना' नहीं है।'' अमेरिका के राइस विश्वविद्यालय से एक्सोप्लैनेट पर केंद्रित पीएचडी करने वाले खगोल वैज्ञानिक आसा स्टाहल ने कहा कि अध्ययन में दूर स्थित ग्रह के वायुमंडल को देखने के लिए एक ‘‘अत्यंत शक्तिशाली उपकरण'' का उपयोग किया गया है। मधुसूदन ने इस बात पर जोर दिया कि शोधकर्ताओं की टीम अध्ययन के परिणामों पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा, ‘‘जब आपको बड़ी सफलताएं मिलती हैं, तो आप वास्तव में आश्वस्त होना चाहते हैं, क्योंकि यह विज्ञान और समाज के मूल ढांचे को मौलिक रूप से बदल देता है।'' मधुसूदन की टीम भविष्य के अनुसंधान में इस पहलू पर विचार कर रही है, लेकिन अणुओं की उत्पत्ति के उत्तर विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि अध्ययनों में धूमकेतु और तारों के बीच के स्थान में डाइमिथाइल सल्फाइड पाया गया है। गोयल ने कहा कि वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके के2-18बी के और अधिक अवलोकन, साथ ही डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड के प्रयोगशाला स्पेक्ट्रा के विस्तृत अध्ययन से अध्ययन के परिणामों को पुष्ट करने या उन पर सवाल खड़ा करने में मदद मिल सकती है।
-
नयी दिल्ली. रोजाना बादाम खाने से एशियाई भारतीयों जैसी कुछ खास आबादी को रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। एक अध्ययन में इसकी जानकारी दी गयी है। बादाम और कार्डियोमेटाबोलिक स्वास्थ्य पर पहले प्रकाशित शोध का विश्लेषण करते हुए, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने कहा कि बादाम ‘खराब' कोलेस्ट्रॉल को कम करके और आंतों के लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ाकर चयापचय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन का निष्कर्ष सर्वसम्मति से प्रकाशित लेख के रूप में पत्रिका ‘करंट डेवलपमेंट्स इन न्यूट्रिशन' में प्रकाशित हुआ है और यह स्वस्थ हृदय और आंत के अनुकूल भोजन के रूप में बादाम की भूमिका को साबित करता है। शोध के लेखक एवं फोर्टिस सेंटर फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल के अध्यक्ष डॉ. अनूप मिश्रा ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि निष्कर्ष यह भी बताते हैं कि बादाम संभावित रूप से एशियाई भारतीयों जैसी विशिष्ट आबादी को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, जहां कार्डियोमेटाबोलिक बीमारियों की बढ़ती दर चिंता का विषय हैं। मिश्रा नेशनल डायबिटीज ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन के प्रमुख भी हैं।
बादाम खाने से एलडीएल या ‘खराब' कोलेस्ट्रॉल पांच यूनिट तक कम हो जाता है, और डायस्टोलिक रक्तचाप 0.17-1.3 एमएमएचजी महत्वपूर्ण मात्रा में कम हो जाता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि प्री-डायबिटीज वाले एशियाई भारतीयों के लिए, रोजाना बादाम खाने से खाली पेट रहते समय रक्त शर्करा और एचबीए1सी को कम करने में मदद मिल सकती है। अध्ययन में कहा गया है कि विश्लेषण से पता चलता है कि बादाम के सेवन से वजन नहीं बढ़ता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और डायस्टोलिक रक्तचाप में थोड़ी कमी आती है, साथ ही कुछ आबादी (यानी एशियाई भारतीय) में ग्लाइसेमिक प्रतिक्रियाओं में सुधार होता है।'' मिश्रा ने कहा, ‘‘ये लाभ ऊर्जा के स्तर को स्थिर करने और भूख में उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद करके वजन घटाने के प्रयासों में सहायता करते हैं। संतुलित पोषण और शारीरिक गतिविधि के साथ, बादाम खाना वजन घटाने में सहायक होता है। - आज हम मोबाइल से सिर्फ एक स्कैन में पेमेंट कर लेते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन वेरिफाई कर लेते हैं। यह सब मुमकिन हो पाया है QR कोड की मदद से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का अविष्कार आज से 31 साल पहले हो गया था? आइए, जानते हैं QR कोड के बनाने के पीछे किसका दिमाग था…किसने बनाया QR कोड?QR कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड को 1994 में जापान के इंजीनियर मसाहिरो हारा ने बनाया था। वह जापान की होसेई यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और उस समय Denso Wave नाम की कंपनी में काम कर रहे थे। यह कंपनी टोयोटा ग्रुप की एक इकाई है।गो गेम से आया आइडियामसाहिरो हारा को QR कोड बनाने का आइडिया एक पारंपरिक जापानी बोर्ड गेम ‘गो गेम’ खेलते समय आया। इस खेल में 19×19 के ग्रिड पर काले और सफेद पत्थरों से चालें चली जाती हैं। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह के ग्रिड में पत्थर रखकर एक गेम खेला जा सकता है, तो इसी तरह एक ग्रिड में बहुत सारी जानकारी भी स्टोर की जा सकती है, जिसे अलग-अलग एंगल से भी पढ़ा जा सके।इसके बाद मसाहिरो ने अपनी टीम के साथ मिलकर QR कोड की शुरुआत की। सबसे पहले इसका उपयोग गाड़ियों के पार्ट्स की पहचान के लिए किया गया। QR कोड में लोकेशन, पहचान और वेब ट्रैकिंग से जुड़ा डेटा रखा जा सकता था। धीरे-धीरे QR कोड का इस्तेमाल बढ़ता गया। अब इसका उपयोग पेमेंट, टिकट, कॉन्टैक्ट शेयरिंग और यहां तक कि आधार वेरिफिकेशन तक में हो रहा है। खास बात यह है कि हर QR कोड यूनिक होता है, यानी कोई भी दो QR कोड एक जैसे नहीं होते।
-
नयी दिल्ली. अमेरिका ने उसके बाजारों में आने वाले भारतीय सामानों पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क या आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क भारतीय सामानों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर बनी हुई है जिन्हें उनसे अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा। इन मुद्दों तथा अमेरिकी कदम के निहितार्थों को कुछ प्रश्न व उतर से समझें-
प्रश्न. शुल्क क्या हैं?
उत्तर. ये वस्तुओं के आयात पर लगाए गए सीमा शुल्क या आयात शुल्क हैं। आयातक को सरकार को यह शुल्क देना होता है। आम तौर पर, कंपनियां इनका बोझ उपयोगकर्ताओं पर डालती हैं।
प्रश्न: जवाबी शुल्क क्या हैं?
उत्तर: ये शुल्क व्यापारिक साझेदारों के शुल्कों में वृद्धि किए जाने या उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए देशों द्वारा लगाए जाते हैं..यह एक तरह के प्रतिशोधात्मक शुल्क हैं।
प्रश्न: अमेरिका ने भारत पर कितना शुल्क लगाया है?
उत्तर: भारत से आने वाले इस्पात, एल्युमीनियम और वाहन व उसके घटकों पर पहले ही 25 प्रतिशत शुल्क लगा है। शेष उत्पादों पर भारत पर पांच से आठ अप्रैल के बीच 10 प्रतिशत का मूल (बेस लाइन) शुल्क लगेगा। फिर नौ अप्रैल से शुल्क 27 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इन कदमों से 60 से अधिक देश प्रभावित होंगे।
प्रश्न: अमेरिका ने इन शुल्कों की घोषणा क्यों की है?
उत्तर: अमेरिका का मानना है कि इन शुल्कों से अमेरिका में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार घाटे में कमी आएगी। अमेरिका को कुछ देशों, खासकर चीन के साथ भारी व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। भारत के साथ अमेरिका का 2023-24 में 35.31 अरब अमरेकी डॉलर का व्यापार घाटा था।
प्रश्न: इन शुल्कों से किन क्षेत्रों को छूट दी गई है?
उत्तर: आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई)के विश्लेषण के अनुसार दवा, सेमीकंडक्टर, तांबा और तेल, गैस, कोयला व एलएनजी जैसे ऊर्जा उत्पाद जैसे आवश्यक एवं रणनीतिक वस्तुओं को इन शुल्कों के दायरे से बाहर रखा गया है।
प्रश्न: इन शुल्कों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: एक सरकारी अधिकारी के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 27 प्रतिशत जवाबी शुल्कों के प्रभाव का आकलन कर रहा है। हालांकि, यह भारत के लिए कोई झटका नहीं है। निर्यातक संगठनों के महासंघ फियो का कहना है कि भारत पर लगाया गया अमेरिकी शुल्क निःसंदेह घरेलू निर्यातकों के लिए चुनौती है, लेकिन भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर है। निर्यातकों ने कहा कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता घरेलू उद्योग को इन शुल्कों के संभावित प्रभाव से उबरने में मदद करेगा। जीटीआरआई ने कहा कि कुल मिलाकर अमेरिका की संरक्षणवादी शुल्क व्यवस्था भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण से लाभ उठाने के लिए मुख्य स्रोत का काम कर सकती है। हालांकि, इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को अपने व्यापार को आसान बनाना होगा, लॉजिस्टिक्स व बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा और नीति स्थिरता बनाए रखनी होगी।
प्रश्न: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता क्या है?
उत्तर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फरवरी में अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के उद्देश्य से इस समझौते पर बातचीत की घोषणा की थी। वे इस वर्ष की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहे हैं।
प्रश्न: व्यापार समझौता क्या है?
उत्तर: ऐसे समझौतों में दो व्यापारिक साझेदार या तो सीमा शुल्क को काफी कम कर देते हैं या अधिकतर वस्तुओं पर उन्हें समाप्त कर देते हैं। वे सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी आसान बनाते हैं।
प्रश्न: अमेरिका ने भारत के प्रतिस्पर्धी देशों पर क्या शुल्क घोषित किए हैं?
उत्तर: चीन पर 54 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत और थाइलैंड पर 36 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।
प्रश्न: क्या ये पारस्परिक शुल्क डब्ल्यूटीओ के अनुरूप हैं?
उत्तर: अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ अभिजीत दास के अनुसार ये शुल्क स्पष्ट रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह एमएफएन (सबसे तरजीही राष्ट्र) दायित्वों तथा बाध्य दर प्रतिबद्धताओं दोनों का उल्लंघन करते हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश को इन शुल्कों के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र का रुख करने का पूरा अधिकार है।
प्रश्न: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है?
उत्तर: वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है। भारत का 2023-24 में अमेरिका के साथ वस्तुओं में 35.32 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष (आयात व निर्यात के बीच का अंतर) था। यह 2022-23 में 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर, 2021-22 में 32.85 अरब अमेरिकी डॉलर, 2020-21 में 22.73 अरब अमेरिकी डॉलर और 2019-20 में 17.26 अरब अमेरिकी डॉलर था। अमेरिका को भारत के मुख्य निर्यात में 2024 में दवा निर्माण तथा जैविक (8.1 अरब अमेरिकी डॉलर), दूरसंचार उपकरण (6.5 अरब अमेरिकी डॉलर), कीमती व अर्ध-कीमती पत्थर (5.3 अरब डॉलर), पेट्रोलियम उत्पाद (4.1 अरब डॉलर), सोना तथा अन्य कीमती धातु के आभूषण (3.2 अरब डॉलर), सहायक उपकरण सहित सूती तैयार वस्त्र (2.8 अरब डॉलर) और लोहा व इस्पात के उत्पाद (2.7 अरब डॉलर) शामिल है। आयात में कच्चा तेल (4.5 अरब डॉलर), पेट्रोलियम उत्पाद (3.6 अरब डॉलर), कोयला, कोक (3.4 अरब डॉलर), तराशे व पॉलिश किए गए हीरे (2.6 अरब डॉलर), इलेक्ट्रिक मशीनरी (1.4 अरब डॉलर), विमान, अंतरिक्ष यान तथा कलपुर्जे (1.3 अरब अमेरिकी डॉलर) और सोना (1.3 अरब डॉलर) शामिल हैं। -
वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस (अमेरिका). नासा की नवीनतम अंतरिक्ष दूरबीन को मंगलवार को प्रक्षेपित किया गया जो पूरे आकाश का अध्ययन करेगी। यह शुरुआत से लेकर अब तक करोड़ों आकाशगंगाओं और उनकी साझा ब्रह्मांडीय चमक (कॉस्मिक ग्लो) का व्यापक अध्ययन करेगी। स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया से स्फीरेक्स वेधशाला को प्रक्षेपित किया। सूर्य का अध्ययन करने के लिए सूटकेस के आकार के चार उपग्रह भी साथ में भेजे गए। कुल 48.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्फीरेक्स मिशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि अरबों वर्षों में आकाशगंगाएं कैसे बनीं और विकसित हुईं तथा कैसे ब्रह्मांड का इतनी तेजी से विस्तार हुआ। स्फीरेक्स उन तारों के बीच बर्फीले बादलों में पानी और जीवन के अन्य तत्वों की खोज करेगा जहां नए सौर मंडल उभर रहे हैं। ‘कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' के मिशन के मुख्य वैज्ञानिक जेमी बॉक ने कहा कि ब्रह्मांडीय चमक ब्रह्मांड के इतिहास में अब तक जितना भी प्रकाश उत्सर्जित हुआ है, उसे अपने अंदर समेटे हुए है। उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मांड को देखने का एक बहुत ही अलग तरीका है, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि अतीत में प्रकाश के कौन से स्रोत छूट गए थे। बॉक ने कहा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सामूहिक चमक का अवलोकन करके वे शुरुआती आकाशगंगाओं से प्रकाश संबंधी जानकारी जुटा सकेंगे तथा यह जान सकेंगे कि वे कैसे बनीं।
-
नयी दिल्ली. चंद्रयान-3 मिशन के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के अध्ययन से पता चला है कि पूर्व के अनुमानों की तुलना में चंद्रमा के ध्रुवों पर अधिक स्थानों पर सतह के ठीक नीचे बर्फ मौजूद हो सकती है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संकाय सदस्य एवं प्रमुख लेखक दुर्गा प्रसाद करणम ने कहा कि सतह के तापमान में बड़े, लेकिन अत्यधिक स्थानीय परिवर्तन सीधे बर्फ के निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं और इन बर्फ कणों को देखने से ‘‘उनके उद्गम एवं इतिहास के बारे में अलग-अलग कहानियां सामने आ सकती हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘इससे हमें यह भी पता चल सकता है कि समय के साथ बर्फ कैसे जमा हुई और चंद्रमा की सतह पर कैसे पहुंची, जिससे इस प्राकृतिक उपग्रह की शुरुआती भूगर्भीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है।'' इससे संबंधित निष्कर्ष पत्रिका ‘कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट' में प्रकाशित हुआ है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा बेंगलुरु से प्रक्षेपित चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ‘सॉफ्ट लैंडिंग' की थी। इसके तीन दिन बाद 26 अगस्त को ‘लैंडिंग' स्थल का नाम ‘शिव शक्ति पॉइंट' रखा गया। चंद्रमा पर बर्फ के पानी में बदलने की संभावना के बारे में करणम ने कहा, ‘‘चंद्रमा की सतह पर अत्यधिक उच्च निर्वात के कारण तरल रूप में पानी मौजूद नहीं रह सकता। इसलिए, बर्फ तरल में परिवर्तित नहीं हो सकती, बल्कि वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाएगी।'' करणम ने कहा, ‘‘वर्तमान समझ के अनुसार, चंद्रमा पर अतीत में रहने योग्य स्थितियां नहीं रही होंगी।'' - क्या आपने कभी "रेपो रेट" (Repo rate) के बारे में सुना है और सोचा है कि इसके बारे में आप और क्या जानते हैं? वित्त और अर्थशास्त्र (Finance and economics) की दुनिया में रेपो रेट एक महत्वपूर्ण अवधारणा हैं और इसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस ब्लॉग में, हम सरल शब्दों में बताएंगे कि रेपो दर (Repo rate) क्या है और यह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है।रेपो रेट के बारे में जानेंसबसे पहले, आइए "रेपो रेट" (Repo rate) शब्द के मतलब को स्पष्ट करें। रेपो "पुनर्खरीद समझौते" (Purchase agreement) का संक्षिप्त रूप है और रेपो रेट (Repo rate) वह ब्याज दर है जिस पर कमर्शियल बैंक (Commercial bank) केंद्रीय बैंक (Central bank) से पैसा उधार ले सकते हैं। कई देशों में, केंद्रीय बैंक धन आपूर्ति को नियंत्रित करने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।इसलिए, जब कमर्शियल बैंकों (Commercial bank) को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने या अपने भंडार का प्रबंधन करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, तो वे धन उधार लेने के लिए केंद्रीय बैंक (Central bank) से संपर्क कर सकते हैं। जिस ब्याज दर पर वे यह पैसा उधार लेते हैं वह रेपो रेट है।रेपो रेट कैसे काम करता है?कल्पना कीजिए कि आप एक कमर्शियल बैंक (Commercial bank) हैं, और आपको अपने ग्राहकों को भुगतान जैसी अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। आप किसी से उधार नहीं ले सकते; आप केंद्रीय बैंक (Central bank) जाएं. केंद्रीय बैंक आपको पैसा उधार देने के लिए सहमत है, लेकिन आपको बाद की तारीख में उतनी ही राशि, ब्याज सहित वापस करने का वादा करना होगा। यहीं पर रेपो रेट (Repo rate) काम आता है।रेपो दर के (Repo rate) ंद्रीय बैंक से पैसे उधार लेने की लागत की तरह है। यदि केंद्रीय बैंक उच्च रेपो रेट निर्धारित करता है, तो कमर्शियल बैंकों के लिए पैसा उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है। इसके विपरीत, कम रेपो रेट का मतलब है कि उधार लेना अधिक किफायती है।अर्थव्यवस्था पर रेपो रेट का प्रभावअब, आइए देखें कि रेपो दर (Repo rate) व्यापक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है:1. ब्याज दरों पर प्रभाव: रेपो रेट का पूरी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ता है। जब केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, तो कमर्शियल बैंक अक्सर उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए लोन के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सभी के लिए उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे घर, कार और निवेश जैसी चीज़ों पर खर्च कम हो जाता है।2. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना: केंद्रीय बैंकों द्वारा रेपो रेट (Repo rate) का उपयोग करने का एक प्राथमिक कारण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। जब अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो और कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हों, तो केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ा सकता है। इससे उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे खर्च धीमा हो सकता है और मुद्रास्फीति कम हो सकती है। दूसरी ओर, यदि अर्थव्यवस्था सुस्त है और मुद्रास्फीति (Inflation) बहुत कम है, तो केंद्रीय बैंक उधार लेने और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए रेपो रेट कम कर सकता है।3. बचत पर असर: रेपो रेट (Repo rate) में बदलाव का असर बचत पर भी पड़ता है। जब केंद्रीय बैंक(Central bank) रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंक बचत खातों पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश करते हैं, जो बचतकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। इसके विपरीत, जब रेपो रेट गिरता है, तो बचत खाते की ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं, जिससे आपकी बचत पर रिटर्न कम हो सकता है।4. विनिमय दरें: रेपो रेट विनिमय दरों को भी प्रभावित कर सकती है। उच्च रेपो दर अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न चाहने वाले विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है, जिससे देश की मुद्रा की सराहना हो सकती है। इसके विपरीत, कम रेपो रेट विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और कमजोर मुद्रा को जन्म दे सकती है।5. निवेश और आर्थिक विकास: व्यवसाय अक्सर विस्तार और निवेश के लिए ऋण पर निर्भर रहते हैं। जब रेपो रेट (Repo rate) अधिक होता है, तो उधार लेना महंगा हो जाता है, और व्यवसाय अपने निवेश में देरी या कटौती कर सकते हैं। इसके विपरीत, कम रेपो रेट व्यवसायों को उधार लेने और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है।निष्कर्षरेपो रेट (Repo rate) एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक अपने देश की अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए करते हैं। रेपो रेट में बदलाव करके, केंद्रीय बैंक उधार लेने की लागत, खर्च पैटर्न, मुद्रास्फीति दर और बहुत कुछ प्रभावित कर सकते हैं। यह समझना कि रेपो रेट कैसे काम करता है और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव आपको सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकता है और व्यापक आर्थिक रुझानों पर नज़र रख सकता है जो हम सभी को प्रभावित करते हैं।
-
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों, खेतों और बगीचों में जैसी ही सूरज ढलता है वैसे ही रात के कीड़ों की एक दबी-छिपी दुनिया जीवंत हो उठती है। ज्यादातर पारिस्थितिकी तंत्रों में विशेषकर दुनिया के गर्म हिस्सों में रात के समय कीड़ों की गतिविधियां चरम पर होती हैं। ये रात्रिचर जीव पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और परागण, अपशिष्ट अपघटन और कीट नियंत्रण जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण कीड़ों के बारे में बताया गया हैं, जो अंधेरा होने के बाद बाहर आते हैं। आइए जानते हैं ये कीड़ें क्यों महत्वपूर्ण हैं।
पतंगा: रात्रि पाली का सितारा
चमकीली तितलियां दिन के समय अक्सर मन मोहने का काम करती हैं जबकि पतंगा रात के समय अपनी खूबियों से लोगों का दिल जीतता है। एक अनुमान के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में पतंगा की करीब 22,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से अधिकांश (प्रजातियां) रात के समय अपनी गतिविधियां करती हैं हालांकि कुछ पतंगा प्रजातियां दिन में और कुछ सुबह व शाम को सक्रिय होती हैं। कई प्रजातियां अपने लंबे, 'स्ट्रॉ' जैसे मुंह के अंगों का उपयोग कर फूलों के रस से भोजन प्राप्त करती हैं और उड़ने से पहले फूलों के बीच पराग डालने का काम करती हैं। कुछ पतंगे कई तरह के पौधों पर भोजन करते हैं, वहीं अन्य पतंगों का कुछ विशिष्ट फूलों के साथ अत्यधिक विशिष्ट संबंध होता है। पतंगों के लार्वा, ‘कैटरपिलर' भी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उदाहरण के तौर पर ‘मैली' नामक पतंगों (ओकोफोरिडे) का लार्वा पत्ती के कूड़े में सूखी पत्तियों को खाता है और इसलिए वह कठोर, सूखे पौधों के अपघटन के लिए आवश्यक हो जाता है। अगर ये पतंगे अपनी कड़ी मेहनत से इन जैविक पदार्थों को नष्ट नहीं करते हैं तो इन पत्तियों का ढेर मनुष्यों के लिए एक समस्या के रूप में सामने आ सकता है। पतंगे और उनके लार्वा मनुष्यों सहित कई जानवरों के लिए वसा और प्रोटीन युक्त भोजन स्रोत प्रदान करते हैं।
रात में व्यस्त जुगनू ः
गर्मी के मौसम में रात के समय अंधेरे में नाचते इन जुगनुओं की चमकती रोशनी को देखना एक जादुई अनुभव है। जुगनू वास्तव में लैम्पाइरिडे परिवार के भौरे हैं और ऑस्ट्रेलिया में इनकी 25 प्रजातियां पाई जाती हैं। जुगनू की प्रत्येक प्रजाति संभावित साथियों के साथ संवाद करने के लिए अपनी स्वयं की विशिष्ट रोशनी का उपयोग करती है। जब एक ही प्रजाति के बहुत से जुगनू इकट्ठा होते हैं, तो वे अपने प्रकाश स्पंदनों को मिला सकते हैं, जिससे एक लुभावना दृश्य बनता है। जुगनू की ये विशिष्ट रोशनी ‘ल्यूसिफेरिन' नाम के अणु और ‘ल्यूसिफेरेज' नाम के एंजाइम से जुड़ी एक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिये उत्पन्न होती है। जब जुगनू ऑक्सीजन की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं, तो रोशनी उत्सर्जित होती है।
लेसविंग्स और मेंटिसफ्लाइ
‘लेसविंग्स', कीटों के एक प्राचीन समूह (न्यूरोप्टेरा) से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम उनके पंखों पर नसों के नाजुक जाल के कारण रखा गया है। अधिकांश वयस्क ‘लेसविंग्स' रात में शिकार करते हैं और अपने शिकार से पोषक तत्वों को निकालने के लिए अपने खोखले, कैंची के आकार के मुंह का उपयोग करके छोटे-छोटे कीटों को खाते हैं। कई ‘लेसविंग्स' प्रजातियां प्रभावी कीट नियंत्रक हैं और इनका उपयोग कृषि में ‘एफिड्स' और ‘मीलीबग्स' जैसे कीटों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। ‘मैन्टिसफ्लाई' नाम से मशहूर ‘मैन्टिड लेसविंग्स' मैन्टिस और मक्खी के बीच एक अजीब संकर जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में यह ‘लेसविंग्स' के समान ही है। ‘मैन्टिसफ्लाई' के लार्वा का बहुत कम अध्ययन किया गया है लेकिन अधिकांश प्रजातियों को कीटों का शिकारी माना जाता है हालांकि कुछ मकड़ी के अंडों को खाते हैं। ‘मैन्टिसफ्लाई' अन्य कीटों को खाकर कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं।
रात के समय काम करने वाले इन जीवों की सुरक्षा ः
रात में कृत्रिम रोशनी रात की पाली में काम करने वाले कीटों के लिए गंभीर व्यवधान पैदा कर रही है।
कीट अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और चमकदार रोशनी के इर्द-गिर्द अंतहीन घेरे में उड़ते रहते हैं तथा अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं, जिस कारण वह मर जाते हैं। भ्रम के कारण होने वाली ये थकावट उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है।
रात में कृत्रिम रोशनी कीटों के प्रजनन को भी बाधित कर सकती है। उल्लू और चमगादड़ आदि कृत्रिम रोशनी के इर्द-गिर्द शिकार करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की रोशनी में उनका शिकार अधिक केंद्रित और कमजोर हो जाता है। हम कैसे मदद कर सकते हैं:
रात में अनावश्यक बाहरी लाइटें बंद करें, खासकर गर्मियों के दौरान जब कई कीट प्रजनन कर रहे होते हैं।
प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए ‘मोशन एक्टिवेटेड' रोशनी का उपयोग करना और बगीचों में कीटनाशकों के उपयोग को कम या फिर समाप्त करना। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए रात भर कड़ी मेहनत करने वाले कीटों की रक्षा करने में छोटे-छोटे बदलाव बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। -
बेंगलुरु. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रविवार को कहा कि अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग करने के लिए प्रक्षेपित किए गए दो उपग्रहों को परीक्षण के तौर पर तीन मीटर की दूरी पर लाया गया और फिर सुरक्षित रूप से वापस ले जाया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि ‘डॉकिंग' प्रक्रिया डेटा के विस्तृत विश्लेषण के बाद पूरी की जाएगी।
इसरो ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘पहले 15 मीटर और फिर तीन मीटर तक पहुंचने का प्रयास किया गया। अंतरिक्ष यान को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया जा रहा है। डेटा का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद डॉकिंग प्रक्रिया की जाएगी।' ‘स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट' (स्पेडेक्स) परियोजना पहले ही सात और नौ जनवरी को ‘डॉकिंग' प्रयोगों के लिए घोषित दो समय सीमा को चूक चुकी है। इसरो ने 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी सी60 रॉकेट के जरिये दो उपग्रहों स्पेसक्राफ्ट ए (एसडीएक्स01) और स्पेसक्राफ्ट बी (एसडीएक्स02) को रवाना किया गया था। करीब 15 मिनट बाद 220-220 किलोमीग्राम वाले ये छोटे अंतरिक्ष यान योजना के अनुसार 476 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में दाखिल हो गए थे। इसरो के अनुसार, स्पेडेक्स परियोजना छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में ‘डॉकिंग' की प्रक्रिया के लिए एक किफायती प्रौद्योगिकी मिशन है। स्पेडेक्स में सफलता हासिल करने के बाद भारत उन जटिल प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा जो इसके भावी मिशनों, जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारने के लिए महत्वपूर्ण हैं। - वाशिंगटन. नदियों, झीलों और अन्य मीठे पानी के स्रोतों में रहने वाले लगभग एक चौथाई जीवों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। बुधवार को प्रकाशित नए शोध में यह जानकारी दी गयी। ब्राजील के सेरा संघीय विश्वविद्यालय की जीवविज्ञानी और अध्ययन की सह-लेखिका पैट्रिशिया चार्वेट ने कहा, “अमेजन जैसी विशाल नदियां शक्तिशाली प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन साथ ही मीठे पानी का वातावरण बहुत संवेदनशील होता है।” इंग्लैंड में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की प्राणी विज्ञानी कैथरीन सेयर ने कहा कि मीठे पानी के आवासन क्षेत्र - जिनमें नदियां, झीलें, तालाब, जलधाराएं, दलदल और आर्द्रभूमि शामिल हैं - ग्रह की सतह के एक प्रतिशत से भी कम हिस्से में हैं, लेकिन वे इसकी 10 प्रतिशत जीव प्रजातियों का भरण-पोषण करते हैं। शोधकर्ताओं ने ड्रैगनफ्लाई, मछली, केकड़ों और अन्य जीवों की लगभग 23,500 प्रजातियों का परीक्षण किया, जो पूर्णतः मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं। उन्होंने पाया कि 24 प्रतिशत प्रजातियां प्रदूषण, बांध, जल निकासी, कृषि, आक्रामक प्रजातियों, जलवायु परिवर्तन और अन्य व्यवधानों से उत्पन्न खतरों के कारण विलुप्त होने के खतरे में हैं - जिन्हें संवेदनशील, संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अध्ययन की सह-लेखक सेयर ने कहा, “अधिकांश प्रजातियों के लिए केवल एक ही खतरा नहीं है जो उन्हें विलुप्त होने के खतरे में डालता है, बल्कि कई खतरे एक साथ मिलकर काम करते हैं।” जर्नल ‘नेचर' में प्रकाशित इस शोध के आंकड़े में पहली बार शोधकर्ताओं ने मीठे पानी की प्रजातियों के लिए वैश्विक जोखिम का विश्लेषण किया है। पिछले अध्ययनों में स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों सहित थलीय जीवों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- नयी दिल्ली. कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के परिणामों में पूर्वाग्रह के बारे में चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से आईआईटी-जोधपुर के शोधकर्ताओं ने भारतीय परिवेश में ‘एल्गोरिदम' में उपयोग के लिए 'निष्पक्षता, गोपनीयता और नियामक' पैमाने पर 'डेटासेट' की गणना करने के उ्देश्य से एक रूपरेखा तैयार की है। गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ निर्धारित नियमों को ‘एल्गोरिदम' कहा जाता है।एआई विशेषज्ञों ने एआई-प्रणालियों के विकास में पश्चिमी डेटासेट के उपयोग पर लगातार चिंता व्यक्त की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर के प्रोफेसर और इस रूपरेखा का वर्णन करने वाले शोधपत्र के लेखक मयंक वत्स ने कहा, ‘‘यदि मुझे विशेष रूप से भारत के लिए ‘चेहरा पहचान प्रणाली' बनानी हो, तो मैं केवल पश्चिमी देशों में विकसित डेटासेट पर निर्भर रहने के बजाय, यहां के लोगों के चेहरे की विशेषताओं और त्वचा के रंग की अद्वितीय विविधता को दर्शाने वाले डेटासेट के उपयोग को प्राथमिकता दूंगा।'' प्रोफेसर मयंक वत्स ने कहा, ‘‘पश्चिमी डेटासेट में भारतीय जनसांख्यिकी की बारीकियों को सटीक रूप से ग्रहण करने के लिए आवश्यक विशेषताओं का अभाव हो सकता है। '' डेटासेट, जो डेटा या सूचना का एक संग्रह है, जिसका उपयोग एआई-आधारित एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है, जिसे डेटा में पैटर्न का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘जब हम एक जिम्मेदार एआई-आधारित प्रणाली या समाधान के निर्माण की बात करते हैं, तो इसके डिजाइन में पहला कदम यह पता लगाना होता है कि किस डेटासेट का उपयोग किया जाना है। यदि डेटासेट में समस्याएं हैं, तो यह उम्मीद करना अवास्तविक है कि एआई-मॉडल स्वचालित रूप से उन सीमाओं को पार कर लेगा।'' इस अध्ययन की सिफारिशों में विविध जनसंख्या से संवेदनशील पहलुओं जैसे लैंगिक और जाति आदि से संबंधित डेटा एकत्र करना शामिल था, तथा यह डेटा इस प्रकार प्रदान किया गया कि व्यक्तियों की गोपनीयता सुरक्षित रहे। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह ढांचा, जो यह भी आकलन करता है कि क्या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित है, संभवतः 'जिम्मेदार डेटासेट' बनाने में सहायता कर सकता है और यह एआई के नैतिक मुद्दों को कम करने की दिशा में एक प्रयास है। 'जिम्मेदार एआई' की अवधारणा की परिकल्पना 1940 के दशक में की गई थी और यह मानव समाज द्वारा परिभाषित नियमों और नैतिकता का पालन करने वाली मशीनों पर केंद्रित थी।
- नयी दिल्ली. पृथ्वी पर 15 करोड़ वर्ष पहले विचरण करने वाले सबसे बड़े डायनासोरों में से एक 'वल्केन' के कंकाल की नीलामी 16 नवंबर को पेरिस में होगी। फ्रांसीसी नीलामी कंपनी कोलिन डु बोकेज और बारबारोसा ने घोषणा की कि नीलामी में ‘‘सबसे पूर्ण'' और सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल को रखा जाएगा। नीलामी के लिए जुलाई में पूर्व-पंजीकरण बोली खुलने के बाद से इसकी मूल अनुमानित कीमत 1.1-2.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 92-185 करोड़ रुपये) हो गई है। राजसी एपेटोसॉरस कंकाल की खोज 2018 में अमेरिका के व्योमिंग में की गई थी और इसकी लंबाई 20.50 मीटर है, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत हड्डियां उसी डायनासोर की हैं। कॉलिन डु बोकेज के संस्थापक और नीलामीकर्ता ओलिवियर कॉलिन डु बोकेज ने एक बयान में कहा, ‘‘वल्केन सबसे बड़ा और सबसे पूर्ण डायनासोर है जो इन सभी से ऊपर है। यह जीवन भर की सबसे पुरानी खोज है।
-
बीजिंग/जियुक्वान. चीन ने बुधवार को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर छह महीने के मिशन पर तीन अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक भेजा जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष इंजीनियर भी शामिल हैं। ‘शेनझोऊ-19' अंतरिक्ष यान को उत्तरपश्चिमी चीन में जियुक्वान अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से बुधवार तड़के लॉन्ग मार्च-2एफ रॉकेट से भेजा गया। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के करीब 10 मिनट बाद ‘शेनझोऊ-19' अपने रॉकेट से अलग हो गया और उसने अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश किया। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी (सीएमएसए) ने घोषणा की कि चालक दल के सदस्य अच्छी स्थिति में हैं और यह प्रक्षेपण पूरी तरह कामयाब रहा। चीन को इस आशंका से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से बाहर कर दिया गया था कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम उसकी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद उसने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया था। वह अभी इकलौता देश है जिसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन है।
इस महीने की शुरुआत में चीन ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने समेत अंतरिक्ष कार्यक्रमों के विकास की अपनी योजनाओं की घोषणा की थी। चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के अलावा कई अंतरिक्ष मिशन भी भेजे हैं जिनमें पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्रित करना और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का चंद्र मिशन भी शामिल है। ‘शेनझोऊ-19' के चालक दल में मिशन कमांडर काई शुझे और अंतरिक्ष यात्री सॉन्ग लिंगडोंग और वांग होज शामिल हैं। सीएमएसए ने बताया कि वांग अभी चीन की इकलौती महिला अंतरिक्ष इंजीनियर और अंतरिक्ष में जाने वाली चीन की तीसरी महिला हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले इस नए दल के कार्यों में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुप्रयोग परीक्षण करना, अंतरिक्ष में मलबे के खिलाफ सुरक्षात्मक उपकरण स्थापित करना और अतिरिक्त वाहन पेलोड और उपकरणों की स्थापना और पुनर्चक्रण का प्रबंधन करना शामिल है। सीएमएसए के प्रवक्ता लिन शिकियांग ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि यह चालक दल 86 अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिक अनुप्रयोग करेगा जिसमें अंतरिक्ष जीव विज्ञान, अंतरिक्ष औषधि और नयी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। यह चालक दल करीब छह महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहेगा।
लिन ने बताया कि चीन साझेदार देशों से अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करने और उन्हें प्रशिक्षित करने पर भी चर्चा कर रहा है और अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। पाकिस्तान से करीबी संबंधों पर विचार करते हुए उसका एक अंतरिक्ष यात्री भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन पर जा सकता है। -
नयी दिल्ली. अंतरिक्ष की यात्रा से अंतरिक्ष यात्रियों के पेट के अंदरूनी अंगों में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली एवं चयापचय प्रक्रिया पर असर डाल सकते हैं। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आयी है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि ये नतीजे यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियान अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं की अगुवाई में एक दल ने आनुवंशिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर तीन महीने की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर गए चूहे की आंत, मलाशय और यकृत में परिवर्तनों का विश्लेषण किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा या अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्थापित आईएसएस पृथ्वी की कक्षा में स्थित एक अंतरिक्ष यान है। यह एक विशिष्ट विज्ञान प्रयोगशाला है और अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों का ‘घर' है। अध्ययन के लेखकों ने आंत के बैक्टीरिया में परिवर्तन पाया जो चूहे के यकृत और आंतों के जीन में बदलावों को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष की यात्रा से प्रतिरक्षा प्रणाली पर दबाव पड़ सकता है और चयापचय प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है। पत्रिका ‘एनपीजे बायोफिल्म्स एंड माइक्रोबायोम्स' में प्रकाशित अध्ययन में लेखकों ने लिखा, ‘‘ये अंत: क्रियाएं आंत-यकृत अक्ष पर असर डालने वाले संकेतों, चयापचय प्रणाली और प्रतिरक्षा कारकों में व्यवधान का संकेत देती हैं जो ग्लूकोज और लिपिड (वसा) के विनियमन को प्रेरित करने की संभावना रखते हैं।'' अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन के नतीजे सुरक्षा उपायों को विकसित करने और चंद्रमा पर दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने से लेकर मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने तक भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की सफलता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।
- मैमथ यानी विशालकाय प्राचीन हाथी कैसे खत्म हुए, इस पर विज्ञान जगत में एक राय नहीं है। एक नया शोध बताता है कि उनकी विलुप्ति में सबसे बड़ा हाथ होमो सेपियंस का था।विज्ञान बताता है कि लगभग 20,000 साल पहले, प्राचीन हाथी या मैमथ और उनके रिश्तेदार धरती पर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे. लेकिन लगभग 10,000 साल पहले, ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। जबकि वे लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहे थे। इसकी एक बड़ी वजह जलवायु में हुए परिवर्तन को माना जाता है क्योंकि लगभग 11,000 साल पहले, पृथ्वी पर हिमयुग समाप्त हो गया था, लेकिन एक नए अध्ययन ने पाया है कि धरती का तापमान बढ़ना मैमथ के खत्म होने की मुख्य वजह नहीं था। ‘साइंस अडवांसेज' पत्रिका में प्रकाशित इस नए विश्लेषण के मुताबिक प्रारंभिक प्रोबोसाइडीन यानी हाथी, फर वाले मैमथ और उनके लंबे-नाक वाले रिश्तेदारों के पतन का संबंध इंसानों के आने और बढ़ने से है।स्विट्जरलैंड के फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकीविद् टॉर्स्टन हॉफे की अगुआई में हुए इस शोध के मुताबिक, "होमो सेपियंस के उदय ने विलुप्ति की दर को तेज कर दिया, जबकि क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव कम था।"शोधकर्ता कहते हैं कि उनका मॉडल पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण देता है। एक प्रजाति का विलुप्त होना अक्सर एक ही कारण का परिणाम नहीं होता, बल्कि कई परिस्थितियों का एक क्रम होता है जो किसी विशिष्ट जीव के जीवित रहने में बाधा डालता है।. जीवन के लिए असहज वातावरण, भोजन की कमी और प्रतिस्पर्धा और अन्य प्रजातियों द्वारा शिकार जैसे कारक मिलकर उस प्रजाति की विलुप्ति का कारण बनते हैं।विज्ञान बता चुका है कि आदिमानवों ने मैमथ का शिकार किया था। कई जगहों पर खुदाइयों में इन विशालकाय हाथियों की हड्डियां मिली हैं जिन पर कटने और मांस छीले जाने के निशान हैं. लेकिन शोधकर्ताओं के बीच इस बात पर एकराय नहीं है कि इस शिकार ने इन जानवरों के विलुप्त होने में कितना योगदान दिया।हॉफे और उनकी टीम ने यह जांचने की कोशिश की कि क्या आधुनिक मानवों के आगमन और मैमथ के पतन के बीच कोई संबंध पाया जा सकता है।कैसे हुआ शोधइसके लिए, उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया. उन्होंने एक एल्गोरिदम को प्रशिक्षित किया जो जीवाश्म रिकॉर्ड को स्कैन करता है, प्रोबोसाइडीन प्रजातियों की घटती संख्या को मापता है और इन संख्या को उनके पर्यावरणीय कारकों से मिलाता है।गोल हो गया है इंसान का दिमागमॉडल को 2,118 जीवाश्मों के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया जो 3.5 करोड़ से 10,000 साल पहले तक जीवित थे। इनमें उनके दांतों के आकार जैसे रूपात्मक बदलाव शामिल थे। मॉडल ने 17 संभावित कारकों को देखा जो इन जानवरों की जनसंख्या को प्रभावित कर सकते थे। इनमें जलवायु और पर्यावरणीय डेटा तो शामिल था ही। साथ ही आधुनिक मानवों यानी होमो सेपियंस के विकास से भी तुलना की गई। 1,29,000 साल पहले होमो सेपियंस का आगमन हुआ था।शोधकर्ता कहते हैं कि उनका मॉडल पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण देता है। एक प्रजाति का विलुप्त होना अक्सर एक ही कारण का परिणाम नहीं होता, बल्कि कई परिस्थितियों का एक क्रम होता है जो किसी विशिष्ट जीव के जीवित रहने में बाधा डालता है।जीवन के लिए असहज वातावरण, भोजन की कमी और प्रतिस्पर्धा और अन्य प्रजातियों द्वारा शिकार जैसे कारक मिलकर उस प्रजाति की विलुप्ति का कारण बनते हैं।54,000 साल पहले निएंडरथालों के यूरोप में गए थे हमारे पूर्वजइससे शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रोबोसाइडीन की विलुप्ति में इंसान द्वारा शिकार एक बड़ी वजह हो सकता है।. वे लिखते हैं, "हमारा मॉडल, सभी अन्य कारकों का ध्यान रखते हुए मानवों के प्रभाव को अलग करता है।. यह दिखाता है कि आदिमानवों और होमो सेपियंस के कारण अनुमानित 5 से 17 गुना वृद्धि में अन्य कारकों का प्रभाव नहीं है। "शोधकर्ता कहते हैं कि हमने पाया कि पिछले लगभग 1,20,000 वर्षों में इंसान का प्रभाव सबसे अधिक रहा लेकिन शुरुआती मानवों का प्रभाव भी कुछ हद तक रहा है। यह निष्कर्ष उस सिद्धांत को और मजबूत करता है कि इंसान ने जैवविविधता को बड़ी हानि पहुंचाई है।
- नील आंदोलन (1859-60 ) आजादी के पहले अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। यह मुख्य रूप से किसानों का आंदोलन था।अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू एवं संगठित विद्रोह नील विद्रोह था। 1859-60 ई. में बंगाल में हुये इस विद्रोह ने प्रतिरोध की एक मिसाल ही स्थापित कर दी। यूरोपीय बाजारों की मांग की पूर्ति के लिये नील उत्पादकों ने किसानों को नील की अलाभकर खेती के लिये बाध्य किया। जिस उपजाऊ जमीन पर चावल की अच्छी खेती हो सकती थी, उस पर किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर झूठे करार द्वारा नील की खेती करवायी जाती थी। करार के वक्त मामूली सी रकम अग्रिम के रूप में दी जाती थी और धोखा देकर उसकी कीमत बाजार भाव से कम आंकी जाती थी। और, यदि किसान अग्रिम वापस करके शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास भी करता था तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था।कालांतर में सत्ता के संरक्षण में पल रहे नील उत्पादकों ने तो करार लिखवाना भी छोड़ दिया और लठैतों को पालकर उनके माध्यम से बलात नील की खेती शुरू कर दी। वे किसानों का अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटना, उनकी एवं फसलों को जलाने जैसे हथकंडे अपनाने लगे।नील आंदोलन की शुरुआत 1859 के मध्य में बड़े नाटकीय ढंग से हुयी। एक सरकारी आदेश को समझने में भूलकर कलारोवा के डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का यह आदेश दिया, जिससे किसान अपनी इच्छानुसार भूमि पर उत्पादन कर सकें। बस, शीघ्र ही किसानों ने नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियां देनी शुरू कर दी। पर, जब क्रियान्वयन नहीं हुआ तो दिगम्बर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने विद्रोह कर दिया। जब सरकार ने बलपूर्वक युक्तियां अपनाने का प्रयास किया तो किसान भी हिंसा पर उतर आये। इस घटना से प्रेरित होकर आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने भी उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने तथा नील की खेती करने से इंकार कर दिया।बाद में किसानों ने जमींदारों के अधिकारों को चुनौती देते हुये उन्हें लगान अदा करना भी बंद कर दिया। यह स्थिति पैदा होने के पश्चात नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर दिये तथा मुकदमे लडऩे के लिये धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। बदले में किसानों ने भी नील उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। इससे किसान शक्तिशाली होते गये तथा नील उत्पादक अकेले पड़ते गये। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार-पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया तथा उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे। हरीशचंद्र मुखर्जी के पत्र हिन्दू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया। दीनबंधु मित्र से नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतीकरण किया।स्थिति को देखते हुये सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिये नील आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें किसानों को यह आश्वासन दिया गया किउन्हें निल उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जाएगा तथा सभी सम्बंधित विवादों को वैधानिक तरीकों से हल किया जाएगा। कोई चारा न देखकर नील उत्पादकों ने बंगाल से अपने कारखाने बंद करने प्रारम्भ कर दिये तथा 1860 तक यह विवाद समाप्त हो गया।
- पर्थ। नासा का डीएआरटी मिशन - दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण - मानवता का पहला वास्तविक दुनिया का ग्रह रक्षा मिशन था। सितंबर 2022 में, डीएआरटी अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर एक छोटे क्षुद्रग्रह के साथी "चंद्रमा" से टकरा गया। इस टक्कर का लक्ष्य यह पता लगाना था कि अगर कोई इस तरह हमारी तरफ आ रहा हो तो क्या हम ऐसी चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। क्षुद्रग्रह के हमारी तरफ बढ़ने और इस तरह के टकराव के बाद बहुत सारे डेटा इकट्ठा करने से, हमें यह भी बेहतर अंदाज़ा मिलेगा कि अगर ऐसा कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराता है तो हमें क्या होगा। नेचर कम्युनिकेशंस में आज प्रकाशित पांच नए अध्ययनों में डिडिमोस-डिमोर्फोस दोहरे क्षुद्रग्रह प्रणाली की उत्पत्ति को जानने के लिए डीएआरटी और उसके यात्रा मित्र लिसियाक्यूब e से भेजी गई छवियों का उपयोग किया गया है। उन्होंने उस डेटा को अन्य क्षुद्रग्रहों के संदर्भ में भी रखा है।क्षुद्रग्रह प्राकृतिक खतरा हैंहमारा सौर मंडल ऐसे छोटे-छोटे क्षुद्रग्रहों के मलबे से भरा है जो कभी ग्रह नहीं बन पाए। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के करीब आते हैं उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट (एनईओ) कहा जाता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा जोखिम पैदा करते हैं, लेकिन सबसे सुलभ भी हैं। इन प्राकृतिक खतरों से ग्रहों की रक्षा वास्तव में उनकी संरचना को जानने पर निर्भर करती है - न कि केवल वे किस चीज से बने हैं, बल्कि वे एक साथ कैसे रखे गए हैं। क्या वे ठोस वस्तुएं हैं जो मौका मिलने पर हमारे वायुमंडल में घुस जाएंगी, या वे मलबे के ढेर की तरह हैं, जिन्हें बमुश्किल एक साथ रखा जा सकता है? डिडिमोस क्षुद्रग्रह, और इसका छोटा चंद्रमा डिमोर्फोस, एक द्विआधारी क्षुद्रग्रह प्रणाली के रूप में जाना जाता है। वे डीएआरटी मिशन के लिए एकदम सही लक्ष्य थे, क्योंकि टकराव के प्रभावों को डिमोर्फोस की कक्षा में परिवर्तन में आसानी से मापा जा सकता था। वे पृथ्वी के भी करीब हैं, या कम से कम एनईओ हैं। और वे एक बहुत ही सामान्य प्रकार के क्षुद्रग्रह हैं जिन्हें हमने पहले अच्छी तरह से नहीं देखा था। यह भी सीखने का मौका मिला कि द्विआधारी क्षुद्रग्रह कैसे बनते हैं, यह सोने पर सुहागा था। बहुत सी द्विआधारी क्षुद्रग्रह प्रणालियों की खोज की गई है, लेकिन ग्रह वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं है कि वे कैसे बनते हैं। नए अध्ययनों में से एक में, अमेरिका में जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के ओलिवियर बार्नौइन के नेतृत्व में एक टीम ने सतह के खुरदरापन और क्रेटर रिकॉर्ड को देखकर सिस्टम की उम्र का अनुमान लगाने के लिए डीएआरटी और लिसियाक्यूब की छवियों का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि डिडिमोस लगभग एक करोड़ 25 लाख वर्ष पुराना है, जबकि इसका चंद्रमा डिमोर्फोस 300,000 साल से भी कम समय पहले बना था। यह भले बहुत बड़ा लगे, लेकिन यह अपेक्षा से बहुत छोटा है।पत्थरों का ढेरडिमोर्फोस भी कोई ठोस चट्टान नहीं है जैसा कि हम आम तौर पर कल्पना करते हैं। यह पत्थरों का एक मलबे का ढेर है जो मुश्किल से एक साथ बंधे हुए हैं। इसकी कम उम्र के साथ, यह दर्शाता है कि बड़े क्षुद्रग्रहों के टकराव के मद्देनजर इन मलबे के ढेर वाले क्षुद्रग्रहों की कई "पीढ़ियाँ" हो सकती हैं। सूरज की रोशनी वास्तव में क्षुद्रग्रहों जैसे छोटे पिंडों के घूमने का कारण बनती है। जैसे ही डिडिमोस एक लट्टू की तरह घूमने लगा, उसका आकार पिचक गया और बीच में उभर आया। यह बड़े टुकड़ों के मुख्य ढेर से लुढ़कने के लिए पर्याप्त था, कुछ के तो निशान भी छूट गए। इन टुकड़ों ने धीरे-धीरे डिडिमोस के चारों ओर मलबे का एक घेरा बना दिया। समय के साथ, जैसे-जैसे मलबा आपस में चिपकने लगा, इससे छोटे चंद्रमा डिमोर्फोस का निर्माण हुआ। अमेरिका में ऑबर्न विश्वविद्यालय के मौरिज़ियो पाजोला के नेतृत्व में एक अन्य अध्ययन में इसकी पुष्टि के लिए बोल्डर वितरण का उपयोग किया गया। टीम ने यह भी पाया कि मनुष्यों द्वारा देखे गए अन्य गैर-बाइनरी क्षुद्रग्रहों की तुलना में वहां काफी अधिक (पांच गुना तक) बड़े पत्थर थे। एक अन्य नए अध्ययन से हमें पता चलता है कि अब तक जितने भी क्षुद्रग्रह अंतरिक्ष अभियानों (इटोकावा, रयुगु और बेन्नू) पर गए हैं, उन पर पत्थरों का आकार संभवतः एक ही तरह का था। लेकिन डिडिमोस प्रणाली पर बड़े पत्थरों की यह अधिकता बायनेरिज़ की एक अनूठी विशेषता हो सकती है। अंत में, एक अन्य पेपर से पता चलता है कि इस प्रकार के क्षुद्रग्रह में दरार पड़ने की संभावना अधिक होती है। यह दिन और रात के बीच ताप-शीतलन चक्र के कारण होता है: जमने-पिघलने के चक्र की तरह लेकिन पानी के बिना। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ (जैसे अंतरिक्ष यान) इस पर प्रभाव डालती है, तो अंतरिक्ष में बहुत अधिक मलबा गिरेगा। इससे "धक्का" देने की मात्रा भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस बात की अच्छी संभावना है कि सतह पर हमे जो दिखाई दे रहा है, सतह के नीचे वह उससे कहीं अधिक मजबूत है। यहीं पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेरा मिशन कदम रखेगा। यह न केवल डीएआरटी प्रभाव स्थलों की उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियां प्रदान करने में सक्षम होगा, बल्कि कम-आवृत्ति रडार का उपयोग करके क्षुद्रग्रहों के अंदरूनी हिस्सों की जांच करने में भी सक्षम होगा। डीएआरटी मिशन ने न केवल भविष्य के क्षुद्रग्रह प्रभावों से खुद को बचाने की हमारी क्षमता का परीक्षण किया, बल्कि हमें पृथ्वी के पास मलबे के ढेर और बाइनरी क्षुद्रग्रहों के गठन और विकास के बारे में भी बताया।
- बुरंजी असमिया भाषा में लिखी हुईं ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। अहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है। प्रथम बुरंजी की रचना असम के प्रथम राजा सुकफा के आदेश पर लिखी गयी, जिन्होंने 1228 ई में असम राज्य की स्थापना की। आरंभ में अहोम भाषा में इनकी रचना होती थी, कालांतर में असमिया भाषा इन ऐतिहासिक लेखों की माध्यम हुई। इसमें राज्य की प्रमुख घटनाओं, युद्ध, संधि, राज्यघोषणा, राजदूत तथा राज्यपालों के विविध कार्य, शिष्टमंडल का आदान प्रदान आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। राजा तथा मंत्री के दैनिक कार्यों के विवरण पर भी प्रकाश डाला गया है।असम में इनके अनेक वृहदाकार खंड प्राप्त हुए हैं। राजा अथवा राज्य के उच्चपदस्थ अधिकारी के निर्देशानुसार शासनतंत्र से पूर्ण परिचित विद्वान् अथवा शासन के योग्य पदाधिकारी इनकी रचना करते थे। घटनाओं का चित्रण सरल एवं स्पष्ट भाषा में किया गया है; इन कृतियों की भाषा में अलंकारिकता का अभाव है। सोलहवीं शती के आरंभ से उन्नीसवीं शती के अंत तक इनका आलेखन होता रहा।बुरंजी राष्ट्रीय असमिया साहित्य का अभिन्न अंग हैं। गदाधर सिंह के राजत्वकाल में पुरनि असम बुरंजी का निर्माण हुआ जिसका संपादन हेमचंद्र गोस्वामी ने किया है। पूर्वी असम की भाषा में इन बुरंजियों की रचना हुई है।बुरंजी मूलत: एक टाइ शब्द है, जिसका अर्थ है "अज्ञात कथाओं का भांडार"। इन बुरंजियों के माध्यम से असम प्रदेश के मध्य काल का काफी व्यवस्थित इतिहास उपलब्ध है। बुरंजी साहित्य के अंतर्गत कामरूप बुरंजी, कछारी बुरंजी, आहोम बुरंजी, जयंतीय बुंरजी, बेलियार बुरंजी के नाम अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध हैं। इन बुरंजी ग्रंथों के अतिरिक्त राजवंशों की विस्तृत वंशावलियाँ भी इस काल में हुई।आहोम राजाओं के असम में स्थापित हो जाने पर उनके आश्रय में रचित साहित्य की प्रेरक प्रवृत्ति धार्मिक न होकर लौकिक हो गई। राजाओं का यशवर्णन इस काल के कवियों का एक प्रमुख कर्तव्य हो गया।वैसे भी अहोम राजाओं में इतिहास लेखन की परंपरा पहले से ही चली आती थी। कवियों की यशवर्णन की प्रवृत्ति को आश्रयदाता राजाओं ने इस ओर मोड़ दिया।पहले तो अहोम भाषा के इतिहास ग्रंथों (बुरंजियों) का अनुवाद असमिया में किया गया और फिर मौलिक रूप से बुरंजियों का सृजन होने लगा।
-
क्या आप जानते हैं कि एक कीड़े की कीमत 75 लाख रुपये हो सकती है? जी हाँ, 'स्टैग बीटल' (Stag Beetle) दुनिया के सबसे महंगे कीड़ों में से एक है। तो, क्या बात है जो इसे इतना ख़ास बनाती है? स्टैग बीटल महंगा है क्योंकि यह काफ़ी दुर्लभ है और इसे शुभ माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि स्टैग बीटल रखने से रातों-रात अमीर बना जा सकता है। यह कीड़े "जंगल पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण सैप्रोक्सिलिक सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने बड़े मैंडिबल्स और पुरुष बहुरूपदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। " वैज्ञानिक डेटा जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में लिखा गया है। लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अनुसार, ये कीड़े 2-6 ग्राम के बीच का वज़न होते हैं और उनका औसत जीवनकाल 3-7 साल होता है। जबकि नर 35-75 mm लंबे होते हैं, मादा 30-50mm लंबी होती हैं। इनका इस्तेमाल औषधीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है स्टैग बीटल नाम नर बीटल पर पाए जाने वाले विशिष्ट मैंडिबल्स से लिया गया है, जो हिरण के सींग से मिलते-जुलते हैं.। नर स्टैग बीटल अपने विशिष्ट, सींग जैसे जबड़ों का इस्तेमाल एक दूसरे से लड़ने के लिए करते हैं। ताकि प्रजनन के मौसम में मादा से मिलन का मौका मिल सके।
ये कहां पाए जाते हैं?स्टैग बीटल गर्म, उष्णकटिबंधीय वातावरण में पनपते हैं और ठंडे तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं.। वे स्वाभाविक रूप से वन में रहते हैं, लेकिन हेजरो, पारंपरिक बागों और शहरी क्षेत्रों जैसे पार्कों और बागानों में भी पाए जा सकते हैं, जहां मृत लकड़ी बहुत ज़्यादा होती है।वे क्या खाते हैं?वयस्क स्टैग बीटल मुख्य रूप से मीठे तरल पदार्थ जैसे पेड़ का रस और सड़ते फलों का रस खाते हैं।. वे मुख्य रूप से अपने लार्वा अवस्था के दौरान एकत्र की गई ऊर्जा भंडार पर निर्भर रहते हैं, जो उनके पूरे वयस्क जीवन में उनका पोषण करता है.। स्टैग बीटल के लार्वा मृत लकड़ी खाते हैं। अपने तेज़ जबड़ों का इस्तेमाल करके रेशेदार सतह से छीलन निकालते हैं.।चूंकि वे सिर्फ़ मृत लकड़ी खाते हैं, इसलिए स्टैग बीटल ज़िंदा पेड़ों या झाड़ियों के लिए कोई खतरा नहीं होते, जिससे वे स्वास्थ्य वनस्पतियों के लिए हानिकारक नहीं होते। - वैदिक धर्म पूर्णत: प्रतिमार्गी हैं वैदिक देवताओं में पुरुष भाव की प्रधानता है। अधिकांश देवताओं की आराधना मानव के रूप में की जाती थी किन्तु कुछ देवताओं की आराधना पशु के रुप में की जाती थी। ऋग्वैदिक आर्यो की देवमण्डली तीन भागों में विभाजित थी।आकाश के देवता - सूर्य, द्यौस, वरुण, मित्र, पूषन, विष्णु, उषा, अपांनपात, सविता, त्रिप, विंवस्वत, आदिंत्यगग, अश्विनद्वय आदि।अंतरिक्ष के देवता- इन्द्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातरिश्वन, त्रिप्रआप्त्य, अज एकपाद, आप, अहिर्बुघ्न्य।पृथ्वी के देवता- अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, तथा नदियां।ऋग्वेद में अन्तरिक्ष स्थानीय इन्द का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, ऋग्वेद के कऱीब 250 सूक्तों में इनका वर्णन है। इन्हें वर्षा का देवता माना जाता था। उन्होंने वृक्ष राक्षस को मारा था इसीलिए उन्हे वृत्रहन कहा जाता है। अनेक किलों को नष्ट कर दिया था, इस रूप में वे पुरन्दर कहे जाते हैं। इन्द्र ने वृत्र की हत्या करके जल का मुक्त करते हैं इसलिए उन्हे पुर्मिद कहा गया। इन्द्र के लिए एक विशेषण अन्सुजीत (पानी को जीतने वाला) भी आता है। इन्द्र के पिता द्योंस हैं अग्नि उसका यमज भाई है और मरुत उसका सहयोगी है। विष्णु के वृत्र के वध में इन्द्र की सहायता की थी। ऋग्वेद में इन्द्र को समस्त संसार का स्वामी बताया गया है। उसका प्रिय आयुद्ध बज्र है इसलिए उन्हे ब्रजबाहू भी कहा गया है। इन्द्र कुशल रथ-योद्धा (रथेष्ठ), महान विजेता (विजेन्द्र) और सोम का पालन करने वाला (सोमपा) है। इन्द्र तूफ़ान और मेध के भी देवता है । एक शक्तिशाली देवता होने के कारण इन्द्र का शतक्रतु (एक सौ शक्ति धारण करने वाला) कहा गया है वृत्र का वध करने का कारण वृत्रहन और मधवन (दानशील) के रूप में जाना जाता है। उनकी पत्नी इन्द्राणी अथवा शची (ऊर्जा) हैं।ऋग्वेद में दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनका काम था मनुष्य और देवता के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाना। अग्नि के द्वारा ही देवताओं आहुतियां दी जाती थीं। ऋग्वेद में कऱीब 200 सूक्तों में अग्नि का जि़क्र किया गया है। वे पुरोहितों के भी देवता थे। उनका मूल निवास स्वर्ग है। किन्तु मातरिश्वन (देवता) ने उसे पृथ्वी पर लाया। पृथ्वी पर यज्ञ वेदी में अग्नि की स्थापना भृगुओं एवं अंगीरसों ने की। इस कार्य के कारण उन्हें अथर्वन कहा गया है। वह प्रत्येक घर में प्रज्वलित होती थी इस कारण उसे प्रत्येक घर का अतिथि माना गया है। तीसरा स्थान वरुण का माना जाता है, जिसे समुद्र का देवता, विश्व के नियामक और शासक सत्य का प्रतीक, ऋतुु परिवर्तन एवं दिन-रात का कर्ता-धर्ता, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता के रूप में जाना जाता है। ईरान में इन्हें अहुरमज्द तथा यूनान में यूरेनस के नाम से जाना जाता है। ये ऋतु के संरक्षक थे इसलिए इन्हें ऋत्स्यगोप भी कहा जाता था। वरुण के साथ मित्र का भी उल्लेख है इन दोनों को मिलाकर मित्र वरूण कहते हैं। ऋग्वेद के मित्र और वरुण के साथ आप का भी उल्लेख किया गया है। आप का अर्थ जल होता है। ऋग्वेद के मित्र और वरुण का सहस्र स्तम्भों वाले भवन में निवास करने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वरुण को वायु का सांस कहा गया है। इनकी स्तुति लगभग 30 सूक्तियों में की गयी है। देवताओं के तीन वर्गों (पृथ्वी स्थान, वायु स्थान और आकाश स्थान) में वरुण का सर्वोच्च स्थान है। ऋग्वेद का 7 वां मण्डल वरुण देवता को समर्पित है।
- आल्हाखण्ड लोककवि जगनिक द्वारा लिखित एक वीर रस प्रधान काव्य हैं जो परमाल रासो का एक खण्ड माना जाता है। आल्हाखण्ड में आल्हा और ऊदल नामक दो प्रसिद्ध वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन हैं।आल्हाखण्ड में महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों- आल्हा और ऊदल (उदय सिंह) का विस्तृत वर्णन है। कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में चलते रहने के कारण उसके वर्तमान रूप में जगनिक की मूल रचना खो-सी गयी है, किन्तु अनुमानत: उसका मूल रूप तेरहवीं या चौदहवीं शताब्दी तक तैयार हो चुका था। आरम्भ में वह वीर रस-प्रधान एक लघु लोकगाथा (बैलेड) रही होगी, जिसमें और भी परिवद्र्धन होने पर उसका रूप गाथाचक्र (बैलेड साइकिल) के समान हो गया, जो कालान्तर में एक लोक महाकाव्य के रूप में विकसित हो गया।पृथ्वीराजरासो के सभी गुण-दोष आल्हाखण्ड में भी वर्तमान हैं, दोनों में अन्तर केवल इतना है कि एक का विकास दरबारी वातावरण में शिष्ट, शिक्षित-वर्ग के बीच हुआ और दूसरे का अशिक्षित ग्रामीण जनता के बीच। आल्हाखण्ड पर अलंकृत महाकाव्यों की शैली का कोई प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता। शब्द-चयन, अलंकार विधान, उक्ति-वैचित्र्य, कम शब्दों में अधिक भाव भरने की प्रवृत्ति प्रसंग-गर्भत्व तथा अन्य काव्य-रूढिय़ों और काव्य-कौशल का दर्शन उसमें बिलकुल नहीं होता। इसके विपरीत उसमें सरल स्वाभाविक ढंग से, सफ़ाई के साथ कथा कहने की प्रवृत्ति मिलती है, किन्तु साथ ही उसमें ओजस्विता और शक्तिमत्ता का इतना अदम्य वेग मिलता है, जो पाठक अथवा श्रोता को झकझोर देता है और उसकी सूखी नसों में भी उष्ण रक्त का संचार कर साहस, उमंग और उत्साह से भर देता है। उसमें वीर रस की इतनी गहरी और तीव्र व्यंजना हुई है और उसके चरित्रों को वीरता और आत्मोत्सर्ग की उस ऊँची भूमि पर उपस्थित किया गया है कि उसके कारण देश और काल की सीमा पार कर समाज की अजस्त्र जीवनधारा से आल्हखण्ड की रसधारा मिलकर एक हो गयी है।
-
नॉर्मन गार्डन्स (ऑस्ट्रेलिया). ‘बैलरैट क्लेरेंडन कॉलेज' ने पिछले महीने पांचवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षा में पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाकर एक परीक्षण किया। स्कूल के अनुसार, ‘‘प्रारंभिक प्रतिक्रिया'' से संकेत मिलता है कि ऐसा करने से कक्षा के दौरान शोर कम हुआ और शौचालय जाने के लिए छात्रों के ‘ब्रेक' लेने में कमी आई। पानी की बोतलें अब स्कूल के लिए जरूरी मानी जाती हैं लेकिन सवाल यह है कि बच्चों को एक दिन में कितना पानी पीने की जरूरत होती है? इसका उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? बच्चों और किशोरों को कितने तरल पदार्थ की जरूरत होती है? यह मौसम और शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है कि बच्चों को कितने तरल पदार्थ की जरूरत है लेकिन सामान्य तौर पर: चार से आठ साल के बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1.2 लीटर पानी पीना चाहिए।
नौ से 13 साल के लड़कों को 1.6 लीटर पानी पीना चाहिए।
नौ से 13 साल की लड़कियों को 1.4 लीटर पानी पीना चाहिए।
चौदह साल से अधिक उम्र के लड़कों को 1.9 लीटर पानी पीना चाहिए।
चौदह साल से अधिक उम्र की लड़कियों को 1.6 लीटर पानी पीना चाहिए।
आहार संबंधी ऑस्ट्रेलियाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, सादा पानी पीना बेहतर होता है लेकिन यदि आपका बच्चा पानी पीना पसंद नहीं करता है, तो आप जूस की कुछ बूंदें इसमें मिला सकते है। शोध से पता चलता है कि कई स्कूली बच्चे पर्याप्त पानी नहीं पीते। कुल 13 देशों (ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर) के 6,469 बच्चों (चार से 17 वर्ष की आयु वर्ग) को शामिल कर 2017 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 60 प्रतिशत बच्चे और 75 प्रतिशत किशोर पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन नहीं करते। हमें कितनी बार पानी पीना चाहिए?
इस बारे में कोई विशेष सलाह नहीं दी गई है कि बच्चों और किशोरों को कितनी बार पानी पीना चाहिए लेकिन शोध से मुख्य रूप से यह संदेश मिलता है कि छात्रों को सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। सुबह, सबसे पहले पानी पीने से शरीर और मस्तिष्क पानी का समुचित उपयोग करते हैं, जिससे पूरे दिन हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। हमारे मस्तिष्क के लिए पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
मस्तिष्क के कुल द्रव्यमान का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा पानी है और हमारे दिमाग को काम करते रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी हार्मोन के स्तर को संतुलित करने, उचित रक्त प्रवाह बनाए रखने और मस्तिष्क में विटामिन, खनिज एवं ऑक्सीजन पहुंचाने में मस्तिष्क की कोशिकाओं और ऊतकों की मदद करता है। इसलिए यदि छात्रों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाया जाए तो इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है।
पानी पढ़ाई में कैसे मददगार है?
जर्मनी के पांच और छह साल के बच्चों पर 2020 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जिन बच्चों ने सुबह चार घंटे की अवधि में पानी की अपनी दैनिक आवश्यकता का कम से कम 50 प्रतिशत (लगभग एक लीटर) पानी पिया, उनका दिमाग समग्र रूप से बेहतर कार्य करता है। बच्चों की दिनचर्या में पानी शामिल करें
नियमित समय पर पानी पीने से बच्चों और युवाओं के लिए नियमित दिनचर्या बनाने में भी मदद मिल सकती है। नियमित दिनचर्या ध्यान, भावनाओं और व्यवहार को प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी पीने के लिए ‘ब्रेक' कक्षा के दौरान ही दिया जाए (खासकर अगर स्कूल को लगता है कि इससे पढ़ाई में बाधा पैदा होती है)। बच्चों के जागने पर, भोजन के समय, बच्चों के स्कूल पहुंचने पर, कक्षाओं की शुरुआत या समाप्ति पर और घर पहुंचने पर पानी पीना मददगार होगा। -
नयी दिल्ली. व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली ‘ओजेम्पिक' और ‘वेगोवी' जैसी मधुमेह और वजन घटाने की दवाओं से पेट के पक्षाघात का खतरा बढ़ सकता है। नए अध्ययनों के निष्कर्ष से यह जानकारी मिली है। पेट का पक्षाघात यानी ‘गैस्ट्रोपैरेसिस' पेट की मांसपेशियों को कमजोर कर देता है, जिससे भोजन मुख्य पाचन अंग में लंबे समय तक पड़ा रहता है। ‘वेगोवी' वजन प्रबंधन के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित दवा है और ‘ओजेम्पिक' ‘टाइप 2' मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मधुमेह के मरीजों को दी जाने वाली दवाओं और वजन घटाने के लिए दी जाने वाली दवाओं से मतली, उल्टी और दस्त जैसे ‘गैस्ट्रोइन्टेस्टनल' (जठरांत्र) से जुड़े दुष्प्रभाव के खतरे के बारे में सभी को जानकारी है लेकिन नए अध्ययन में पता चला है कि इनसे पेट के पक्षाघात, ‘इलियस' (आंत का सिकुड़कर अपशिष्ट को शरीर के बाहर ना निकाल पाना) और ‘पैन्क्रियाटाइटिस' (अग्नाशय में सूजन) का खतरे बढ़ने का भी पता चला है। ये अध्ययन 18 से 21 मई तक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित सम्मेलन ‘पाचन रोग सप्ताह 2024' में पेश किए गए। ‘कन्सास' यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं सहित कई शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इन अध्ययनों में से एक अध्ययन ने मधुमेह या मोटापे से पीड़ित ऐसे 1.85 लाख रोगियों की पहचान की, जिन्हें एक दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2022 के बीच ये दवाएं दी गई थीं। शोधकर्ताओं ने पाया कि लगभग 0.53 प्रतिशत रोगियों में ‘गैस्ट्रोपैरेसिस' की समस्या पाई गई और उन्होंने अनुमान जताया है कि इस स्थिति का खतरा 66 प्रतिशत बढ़ गया है। एक अन्य अध्ययन में टाइप 2 मधुमेह की दवाएं लेने वाले रोगियों में ‘गैस्ट्रोपैरेसिस' के जोखिम का आकलन किया गया और उनमें इसका खतरा बढ़ने की पुष्टि हुई। ‘मायो क्लिनिक मिनेसोटा' के शोधकर्ताओं के एक अन्य अध्ययन में भी यही बात साबित हुई।
- हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर देखने में भले ही आम लगे, लेकिन वास्तव में यह एक गंभीर समस्या है, जिसे नजरअंदाज करना सेहत से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकती है। हाइपरटेंशन कई बार हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है। हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मकसद लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरुकता फैलाना होता है। इस दिवस पर जगह-जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरुक किया जाता है।विश्व हाइपरटेंशन दिवस का इतिहासहर साल 17 मई को विश्वभर में विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग (WHL) द्वारा 14 मई 2005 को की गई थी। आगे चलकर इस दिवस को 17 मई को मनाया जाने लगा। हर साल हाइपरटेंशन के बढ़ते मामलों को देखकर यह दिवस मनाया जाने लगा, जिससे लोगों में हाई बीपी की रोकथाम होने के साथ ही इसे बढ़ने से भी रोका जा सके। खराब लाइफस्टाइल और अनियंत्रित जीवनशैली के चलते यह समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की मानें तो हाई ब्लड प्रेशर के चलते हर साल दुनियाभर में 7.5 मिलियन लोगों की मौत होती है।विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाने का उद्देश्यविश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य या फिर मकसद लोगों को हाइपरटेंशन से मुक्त करना है। इस दिन दुनियाभर में अलग-अलग जगहों पर सेमिनार और इवेंट्स आयोजित करके लोगों को हाइपरटेंशन से जीतने का हौंसला दिया जाता है। इस दिवस को मनाकर लोगों का हौंसला उफजाई किया जाता है। इस दिन लोगों को हाइपरटेंशन के कारण, लक्षण और इससे बचने के तरीकों के बारे में बताया जाता है। जिससे लोग अपना लाइफस्टाइल ठीक करके इस बीमारी से बचे रहें।विश्व हाइपरटेंशन दिवस की थीमविश्व हाइपरटेंशन दिवस की इस साल की थीम Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, and Live Longer है। इस थीम से यह समझ आता है कि ब्लड प्रेशर को सटीकता के साथ कंट्रोल किया जाना चाहिए। इसे कंट्रोल करके आप लंबे समय तक सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हाई बीपी के लक्षण दिखने पर इसे नजरअंदाज नहीं करें।
- नयी दिल्ली. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने एक अनूठी पहल ‘‘रिंकल्स अच्छे हैं'' के तहत हर सोमवार को अपने कर्मचारियों को बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने के लिए कहा है जिससे कि करीब 1,25,000 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बंबई के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने यह जानकारी दी।हालांकि,सीएसआईआर ने स्पष्ट किया कि उसके मुख्यालय ने अपनी प्रयोगशालाओं को ऐसा कोई सुर्कलर या आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें कर्मचारियों को इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने से बचने को कहा गया हो। सीएसआईआर ने एक पोस्ट में कहा, ‘‘23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस समारोह के दौरान आईआईटी-बंबई के प्रोफेसर चेतन सोलंकी ने सीएसआईआर-मुख्यालय में जलवायु घड़ी स्थापित करने के बाद अपने भाषण में ऐसे विचार साझा किए थे।'' ‘रिंकल्स अच्छे है' पहल का उद्देश्य हर किसी को ऊर्जा बचाने, पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में याद दिलाना है। ‘एनर्जी स्वराज मूवमेंट' के संस्थापक चेतन सिंह सोलंकी ने कहा, ‘‘हम हर सोमवार को करीब 1,25,000 किग्रा. कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के सबसे आसान समाधानों में से एक ‘कुछ न करना' है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारा ‘रिंकल्स अच्छे हैं' (डब्ल्यूएएच/वाह) अभियान जोर पकड़ रह है। इसमें हम लोगों से सोमवार को बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि एक जोड़ी कपड़ा इस्त्री न करके हम 200 ग्राम तक कार्बन उत्सर्जन से बच सकते हैं।सोलंकी ने कहा, ‘‘हम लाखों लोग एक जैसा करते हैं तो बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन से बचते हैं और यह चलन बन जाता है। अभी हर सोमवार को 6,25,000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। हम हर सोमवार को करीब 1,25,000 किग्रा. कार्बन उत्सर्जन से बच रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष के अंत तक एक करोड़ से अधिक लोग इस ‘वाह' मंडे अभियान में शामिल होंगे।'' एक अधिकारी ने बताया कि सीएसआईआर अपनी सभी प्रयोगशालाओं में 10 फीसदी तक बिजली खपत को कम करने की भी योजना बना रहा है। प्रोफेसर सोलंकी ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सीएसआईआर इमारत के शीर्ष पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है।
















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)






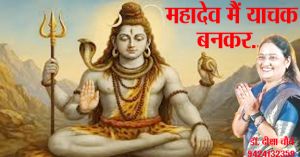


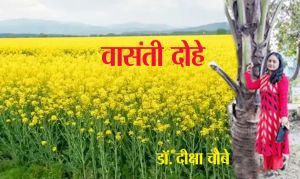








.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)



.jpg)



.jpg)

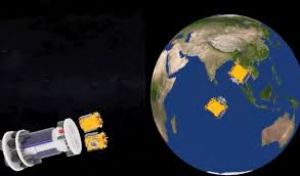





.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)





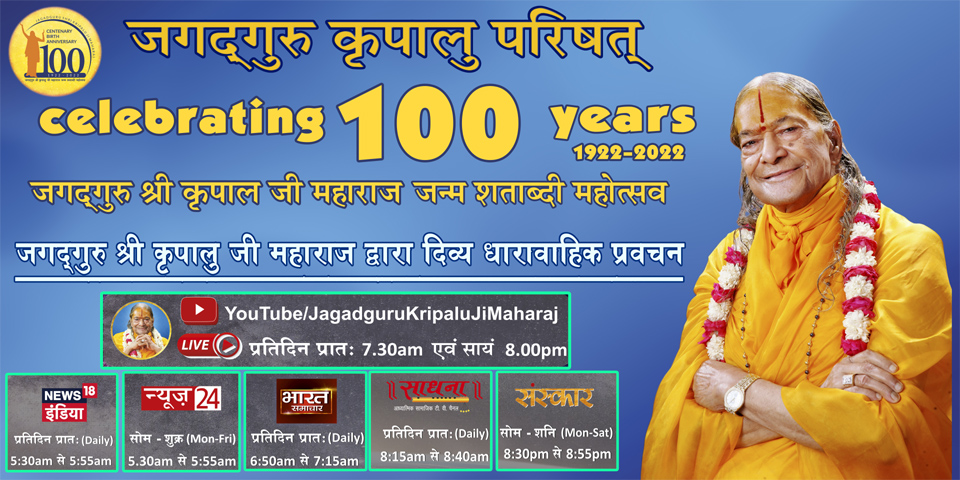



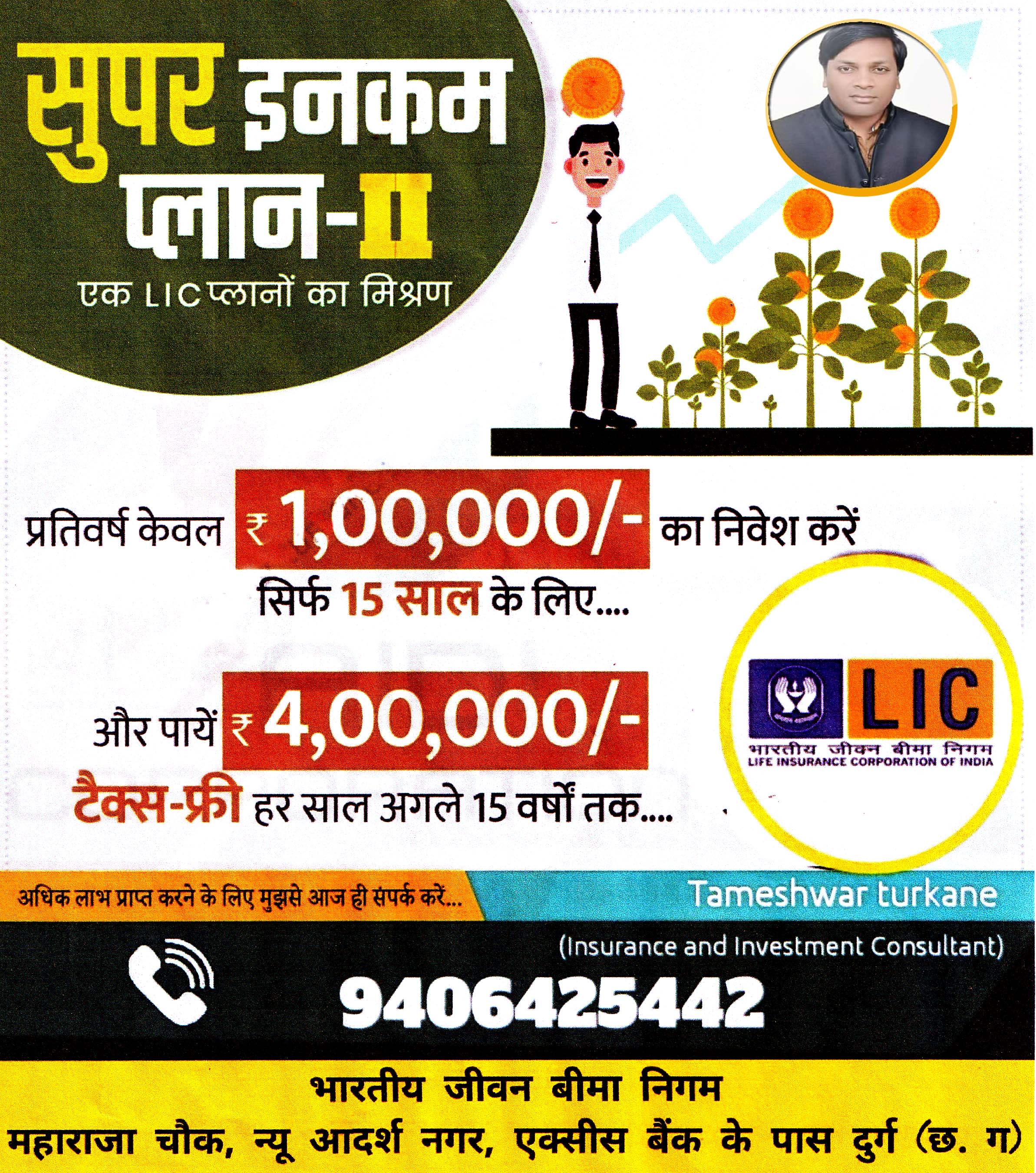
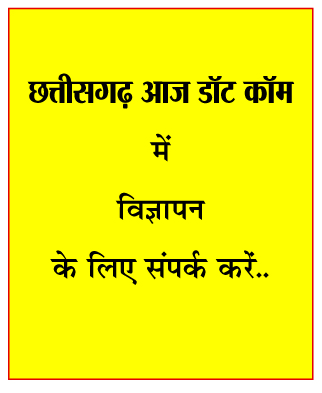

.jpg)
