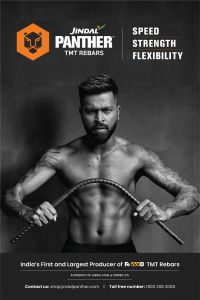- Home
- ज्ञान विज्ञान
-
नयी दिल्ली. वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने संभवत: इस बात का कारण ढूढ लिया है कि उम्र बढ़ने पर बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। उन्होंने इसके लिए रंजक (पिगमेंट) बनाने वाली स्टेम कोशिकाओं की परिपक्व होने की असमर्थता का हवाला दिया है। यह अध्ययन ‘नेचर' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है जिससे बाल सफेद होने की प्रक्रिया को पलटने का आधार मिल सकता है। इस अध्ययन में पाया गया कि स्टेम कोशिकाओं में बाल (रोओं) की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में बढ़ने की क्षमता है लेकिन जब जब लोग बुजुर्ग होते हैं तो उनके परिपक्व होने एवं बाल रंग को बनाये रखने की क्षमता खत्म हो जाती है। अमेरिका के एनवाईयू ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसीन के अनुसंधानकर्ताओं की अगुवाई में एक टीम ने चूहे की त्वचा की कोशिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें मनुष्य में भी ‘मेलानोसाइट' स्टेम कोशिकाएं मिलीं। बाल का रंग इस बात से नियंत्रित होता है कि मेलानोसाइट स्टेम कोशिकाओं की गैर क्रियाशीलता लेकिन निरंतर गुणकता को क्या परिपक्व कोशिकाओं में तब्दील होने का सिग्नल मिलता है या नहीं जो प्रोटीन पिगमेंट को रंग के लिए जिम्मेदार बनाता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि मेलानोसाइट स्टम कोशिकाएं काफी लचीली होती हैं जिसका तात्पर्य है कि बाल की सामान्य वृद्धि के दौरान ऐसी कोशिकाएं परिपक्वता अक्षरेखा पर कभी आगे तो कभी पीछे जाती जाती है, वह भी तब जब वे रोओं से विकास के विभिन्न चरणों से जब गुजरती हैं।
-- - आप यह जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहां एक, दो या तीन नहीं बल्कि पूरे 23 प्लेटफॉर्म हैं और 26 रेल लाइन बिछी हुई हैं। सबसे बड़ा स्टेशन होने के साथ ही इसे भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन का भी दर्जा प्राप्त है। यह स्टेशन हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहां से हर रोज करीब 600 ट्रेनें गुजरती हैं, जिसमें हर दिन लगभग 10 लाख लोगों की आवाजाही है। आप पहली बार इस रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, तो लगेगा जैसे पूरा शहर यहां समा गया है।बता दें कि हावड़ा जंक्शन भारत के सबसे बड़े और पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस जंक्शन का निर्माण 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के जमाने का यह रेलवे स्टेशन आज तके वैसे ही खड़ा है। इसका नाम हावड़ शहर के नाम पर रखा गया था। भारत का यह इकलौता रेलवे स्टेशन है, जिसका रेल संपर्क सीधे बांग्लादेश से है। मैत्री एक्सप्रेस जो सीधे कोलकाता से ढाका के बीच चलती है , दोनों शहरों को जोड़ती है। कभी यह जंक्शन क्रांतिकारियों का केंद्र हुआ करता था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी मीटिंग और सभी योजनाएं यहीं तैयार होती थीं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी योगेश चंद्र चटर्जी को काकोरी कांड से पहले हावड़ा स्टेशन पर ही गिरफ्तार किया गया था।हावड़ा जंक्शन को देश के सबसे खूबसूरत स्टेशन का भी दर्जा प्राप्त है। बाहर से ही नहीं भीतर से भी यह स्टेशन विदेश के स्टेशनों से कम नहीं लगता। कोलकाता का यह रेलवे स्टेशन टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इस जंक्शन पर एक साथ एक ही समय पर कई ट्रेनें खड़ी की जा सकती है। यह क्षमता शायद ही भारत के किसी अन्य रेलवे स्टेशन की हो।
-
पुणे (महाराष्ट्र) .स्कूलों, कॉलेजों और औपचारिक कार्यक्रमों में विज्ञान के विषयों पर चर्चा आम बात है लेकिन लोग अब मशीनों, ब्रह्मांड और जलवायु परिवर्तन जैसे विज्ञान के विभिन्न विषयों पर पब, लाउंज और कैफे में ही नहीं बल्कि शराब की चुस्की के साथ भी सामान्य बातचीत करने लगे हैं। उनका फार्मूला है : ‘‘विज्ञान ‘प्लस' शराब की चुस्की ‘माइनस' गपशप और गंभीरता यानी खूब सारा मजा''।
जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के जलवायु विज्ञानी अनूप महाजन की अगुवाई में पुणे के विज्ञानप्रेमियों का एक समूह अपनी अनूठी ‘साइंस ऑन टैप' पहल से विज्ञान और आम लोगों के बीच फासला कम करने के मिशन पर है। महाजन ने कहा कि विज्ञान और लोगों के बीच की खाई को कम करने के उद्देश्य से लोगों तक पहुंचने की यह पहल शुरू की गई है। ‘साइंस ऑन टैप' योजना के पीछे महाजन का ही दिमाग है। उन्होंने कहा, ‘‘बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं। लोग नहीं जानते कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत है। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी के संपर्क में हैं जो असत्यापित हैं और विज्ञान सहित सभी विषयों पर गलत सूचनाएं फैल रही हैं।'' महाजन ने कहा, ‘‘इस तरह के सभी विज्ञान संपर्क कार्यक्रम ऑडिटोरियम, स्कूल और कॉलेजों जैसी औपचारिक जगहों पर होते हैं जहां पहुंच सीमित है। यहां तक कि अगर हम ऑडिटोरियम में विशेषज्ञों को आमंत्रित करके वार्ता आयोजित करते हैं और उन्हें सभी के लिए खुला रखते हैं, तो भी संभावना है कि लोग नहीं आएंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए हमने आम जनता तक पहुंचने का फैसला किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि युवा लोग अच्छा समय बिताने के लिए कहां जाते हैं। जवाब था रेस्तरां, लाउंज, कैफे या उनका पसंदीदा बार या पब और फिर चर्चा को ऐसी जगहों पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।'' - ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया है कि पिंजरे में जन्मे पक्षियों का जीवन सामान्य नहीं होता। ईकोलॉजी लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है कि पिंजरे में जन्मे पक्षियों के पंखों का आकार भी बदल सकता है और उनकी मुश्किलें सहने की क्षमता भी प्रभावित होती है।शोधकर्ता डॉ. डिजान स्टोयानोविच कहते हैं कि प्रजातियों के संरक्षण के लिए पिंजरों में प्राणियों का प्रजनन एक अहम उपाय है, लेकिन इस तरीके का उनके शारीरिक आकार-प्रकार पर असर पड़ सकता है. शोधकर्ताओं ने जिन पक्षियों का अध्ययन किया, उनमें नारंगी पेट वाला तोता भी था। यह प्रजाति खतरे में है।ऑस्ट्रेलिया में जिन प्रजातियों को खतरे में होने के कारण सुरक्षित वातावरण में प्रजनन कराया जाता है, उनमें नारंगी पेट वाला तोता भी शामिल है और लंबे समय से इस प्रजाति को संरक्षण में रखा गया है। इस प्रजाति को बचाए रखने के लिए हर साल तय संख्या में पक्षियों को आजाद किया जाता है, जो मारे गए पक्षियों की जगह लेते हैं।डॉ. स्टोयानोविच कहते हैं, "पहले हम दिखा चुके हैं कि कैद में रहने से नारंगी पेट वाले तोते के परों का आकार बदल सकता है। हमें संदेह है कि इस कारण उनके लिए लंबी उड़ानें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन नए अध्ययन में हमें पहली बार ऐसे सीधे प्रमाण मिले हैं कि कैद में इनके परों का आकार बदल गया और जंगल में छोड़े जाने के बाद प्रवासन के लिए लंबी उड़ानों में उनकी सफलता की दर कम हो गई। "वैसे तो सभी नारंगी पेट वाले सभी युवा तोतों में प्रवासन के लिए उड़ान की सफलता दर कम पाई गई लेकिन पिंजरों में जन्मे छोटे परों वाले पक्षियों के इन उड़ानों के दौरान बचने की संभावना जंगल में पैदा हुए तोतों के मुकाबले 2.7 गुणा कम पाई गई। शोध में चार अन्य पक्षियों के परों में बदलाव देखा गया जिसके बाद शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि कैद का पक्षियों में पहले लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा असर होता है।डॉ. स्टोयानोविच बताते हैं, "कैद में रखे गए जानवरों में होने वाले शारीरिक बदलावों की यह झलक मात्र हो सकती है और इसे नजरअंदाज करना बहुत आसान है, लेकिन आजाद किए जाने के बाद उन पर इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। अगर हम प्रजातियों के संरक्षण को वन्य जीवन की मदद के लिए ज्यादा कारगर बनाना चाहते हैं तो हमें इस बारे में जागरूक होना चाहिए और ऐसे रास्ते खोजने चाहिए जिनसे पिंजरों में उन पर कम से कम असर हो। "हालांकि इस अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं होता कि पक्षियों में ये बदलाव क्यों आए। यानी, यह बंद वातावरण का असर था या आनुवांशिक वजहों से ये बदलाव हुए. डॉ. स्टोयानोविच के मुताबिक कई और सवाल भी अभी अनुत्तरित हैं, जैसे कि क्या एक बार आजाद किए जाने के बाद पक्षियों के परों का आकार वापस सामान्य हो सकता है या उडऩे के प्रशिक्षण से उन्हें मदद मिल सकती है। वह कहते हैं, "इन सवालों के जवाब खोजने जरूरी हैं ताकि हम यह जान सकें कि संरक्षित माहौल में प्राणी प्रजनन किस तरह से हो कि वे वन्य जीवन में जीने के लिए तैयार हो सकें। "
- राजस्थान अपनी रंग-बिरंगी संस्कृति और इतिहास के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यहां के कई किले और महल आकर्षण का केंद्र है। यहां पर घूमने आने वाले पर्यटक इन महलों की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल सबसे अलग और खास है। गुलाबी और बलुआ रंग के पत्थरों से बने इस महल की अलग ही शान है। इसी महल के कारण जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। हवा महल का निर्माण राजस्थानी और मुगल शैली में किया गया है। हालांकि हवा महल से जुड़ी सभी बातों को लोग जानते हैं। आइए जानते हैं हवा महल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें...जयपुर का हवा महल सिटी पैलेस का हिस्सा था। इसलिए इसका कोई बाहर से एंट्रेंस गेट नहीं बनाया गया था। सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाजा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। वहीं से आपको एंट्री लेनी होती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह महल बगैर नींव के बना है। जिसके कारण यह वजन से घुमावदार और 87 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है।पैलेस ऑफ विंड्सहवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में बनीं 953 खिड़कियां इसे दूसरे महलों से अलग बनाती हैं। इन खिड़कियों को इसलिए बनाया गया था। ताकि हवा महल के अंदर आ सके और यहां गर्मी का एहसास भी न हो।महिलाओं के लिए बनाया गयाहवा महल को खासतौर पर राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनवाया गया था। उस दौरान महिलाए खुले आम किसी भी आयोजन में नहीं शामिल होती थीं। इसलिए इस महल की खिड़कियों पर खड़े होकर वह नीचे आयोजित हो रहे कार्यक्रम को देखती थीं।महल में नहीं बनीं हैं सीढिय़ांभले ही यह महल पांच मंजिला बना है, लेकिन इस महल में आपको सीढिय़ां नहीं मिलेंगी। हर मंजिल पर आपको रैंप करके जाना होगा। बता दें कि हवा महल को रहने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। कुछ विशेष मौकों पर राजसी महिलाएं अपनी दासियों के साथ सिटी पैलेस से यहां आया करती थीं।महल में बने हैं 3 मंदिरइस भव्य महल के अंदर तीन मंदिर बने हुए हैं। जिन्हें गोवर्धन मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि पहले लोग गोवर्धन कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन करते थे। लेकिन उब उन्हें बंद कर दिया गया है।हवा मंदिर नाम के एक मंदिर के नाम पर इस महल का नाम रखा गया था। आज भी यह मंदिर हवा महल के अंदर है। इसलिए इस महल का नाम हवा महल रखा गया। हवा महल खूबसूरत वास्तुकला का नमूना है।
- तस्वीर में आपको जो गिटार दिख रहा है वो मामूली नहीं है। यह दुनिया का सबसे महंगा गिटार है। इसे 'एडन ऑफ कोरोनेट' (Eden of Coronet) कहा जाता है। इस गिटार में 11,441 हीरे जड़े हैं। 18 कैरेट वाइट गोल्ड से यह बना है। इसकी कीमत करीब 16 करोड़ 45 लाख रुपये है। इसे बनाने वाले हैं हांगकांग के आरोन शुम। यह 700 दिनों में बनकर तैयार हुआ था।इस गिटार को बनाने के लिए गिबसन ने ज्वैलरी डिजाइनर आरोन शुम और म्यूजिशियन मार्क लुई के साथ गठजोड़ किया था। यह कस्टमाइज्ड गिबसन एसजी गिटार है। गिबसन लेस पॉल एसजी ने 1961 में गिटार का इलेक्ट्रिक मॉडल पेश किया था। इसी को गिबसन एसजी कहते हैं। एडन ऑफ कोरोनेट को बनाने के लिए हीरे हांगकांग की फर्म चाव ताई फूक ने मुहैया कराए थे। इस गिटार की खास बात है कि यह सिर्फ शोपीस नहीं है। इसे बजाया जा सकता है। अपने ब्रांड कोरोनेट के लिए हांगकांग के आरोम शुम ज्वैलरी ने इसे बनाने का बीड़ा उठाया था।सबसे पहले अबूधाबी के मरीना मॉल में इस बेशकीमती गिटार को पेश किया गया था। वो साल 2015 था। तब बेसलवर्ल्ड वॉच एंड ज्वैलरी शो हुआ था। बाद में इसे चीन में डिस्प्ले किया गया था। अक्टूबर 2019 में यह वापस अबूधाबी आ गया। इसे बेसलवर्ल्ड में फिर से डिस्प्ले किया गया।गिटार की बॉडी वाइट गोल्ड से कवर है। इसमें फूल की आकृति में हीरे जड़े हैं। इन हीरों की संख्या 11,441 है। ये सभी 401.15 कैरेट के हैं। इसे बनाने में 1.6 किलो सोना लगा है। गिटार बनाने में 700 दिन का वक्त लगा था। इसमें 68 कारीगर लगे थे। गिटार के टोन कंट्रोल हीरों की परत के नीचे छुपे रहते हैं।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इस बात के बड़े सबूत मिले हैं कि कुकिंग गैस पर खाना बनाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इसका विकल्प खोजने पर जोर दिया जा रहा है।ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब कुकिंग गैस का विकल्प खोजने का वक्त आ गया है क्योंकि लगातार ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं कि खाना बनाने का यह तरीका सेहत के लिए ठीक नहीं है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है।वैसे तो कुकिंग गैस को लेकर चिंताएं काफी पहले से जताई जाती रही हैं लेकिन हाल ही में आए एक शोध के बाद इस बात पर बहस तेज हो गई है कि कुकिंग गैस कितनी खतरनाक हो सकती है। ताजा अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में बच्चों को दमे का रोग होने में कुकिंग गैस से होने वाले उत्सर्जन की बड़ी भूमिका है। इस अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में बच्चों में दमा होने के जितने मामले हैं उनमें से 12.7 फीसदी, यानी हर आठ में से एक मामले में वजह गैस स्टोव से हुआ उत्सर्जन है।इस साल की शुरुआत में ही अमेरिका के कंज्यूमर प्रॉडक्ट सेफ्टी कमीशन ने ऐलान किया था कि वह कुकिंग गैस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुकिंग गैस को लेकर चिंताएं बेवजह नहीं हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में एसोसिएट प्रोफेसर डोना ग्रीन कहती हैं कि कुकिंग गैस से होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंतित होना जायज है।उन्होंने कहा, "हम स्टोव पर आमतौर पर खाना बनाते हैं। इसका अर्थ है कि आपका प्रदूषकों से नियमित तौर पर वास्ता पड़ता है क्योंकि चेहरा गैस के करीब होता है और यह अच्छा नहीं है। अब हमारे पास विकल्प हैं जो ज्यादा सुरक्षित हैं और पर्यावरण के भी अनुकूल हैं।"प्रोफेसर ग्रीन की तरह ही पर्यावरण संबंधी रोगों के विशेषज्ञ डॉ. क्रिस्टीन कोवी भी इस चिंता से सहमत हैं और कहती हैं कि कुकिंग गैस से दूरी जरूरी है। उन्होंने कहा, "यह हमारे घरों और आसपास एक ऐसा प्रदूषक है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। विज्ञान दिखा रहा है कि हमें जीवाश्म ईंधनों को जलाने को रोकना चाहिए और गैस भी उनमें शामिल है। "कुकिंग गैस सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इससे कई तरह के प्रदूषक तत्वों का उत्सर्जन होता है। प्रोफेसर ग्रीन के मुताबिक जब आप गैस जलाते हैं तो असल में आप मीथेन गैस को जला रहे होते हैं जिससे जहरीले यौगिक बनते हैं। कुकिंग गैस में मीथेन मुख्य अवयव होता है, जो जलने पर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करता है। इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रो ऑक्साइड बनते हैं। प्रोफेसर ग्रीन कहती हैं कि इसके सेहत के लिए कई गंभीर परिणाम होते हैं जिनमें दमा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शामिल हैं। डॉ कोवी बताती हैं कि जब स्टोव जलता है तो असल में आप जीवाश्म ईंधन ही जला रहे हैं जिससे कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और फारमैल्डीहाइड भी बन सकते हैं। डॉ कोवी कहती हैं कि कार्बन मोनो ऑक्साइड के उत्सर्जन से हवा में ऑक्सजीन कम होती है और खून में भी ऑक्सीजन नष्ट होती है। इससे सिर दर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।कुकिंग गैस जलाना पर्यावरण के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। 2022 में एक अध्ययन में कहा गया था कि अमेरिका में गैस स्टोव से जितना कार्बन उत्सर्जन होता है वह पांच लाख कारों से होने वाले उत्सर्जन के बराबर है।इसीलिए अब वैज्ञानिक कुकिंग गैस का विकल्प खोजने पर जोर दे रहे हैं। इंडक्शन चूल्हे और बिजली के चूल्हों को इसके विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इंडक्शन चूल्हों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से गर्मी पैदा की जाती है और इसे कुकिंग गैस के सबसे सक्षम विकल्प के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह एक महंगा विकल्प है। वैज्ञानिक बिजली के चूल्हों को लेकर कुछ सशंकित हैं क्योंकि ज्यादातर बिजली उत्पादन कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाकर ही किया जाता है। इसलिए अक्षय ऊर्जा से पैदा की जा रही बिजली को ही एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है।
-
नयी दिल्ली। वैज्ञानिक वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग के विस्तार की दर को देखते हुए कानूनी रूप से बाध्य संधि की मांग कर रहे हैं ताकि पृथ्वी की कक्षा को अपूरणीय क्षति न पहुंचायी जाए। कई सामाजिक और पर्यावरणीय फायदे उपलब्ध कराने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसी आशंका है कि अंतरिक्ष उद्योग की अनुमानित वृद्धि पृथ्वी की कक्षा के बड़े हिस्सों को अनुपयोगी बना सकती है।
पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की संख्या आज के 9,000 से बढ़कर 2030 तक 60,000 तक पहुंच सकती है। ऐसा अनुमान है कि पुराने उपग्रहों के 100 लाख करोड़ से अधिक टुकड़े इस ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, जिनका अभी पता नहीं लगाया जा सका है। उपग्रह प्रौद्योगिकी और समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण समेत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय संघ ने कहा कि इस पर तत्काल वैश्विक सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता जान पड़ती है कि पृथ्वी की कक्षा को कैसे बेहतर तरीके नियंत्रित किया जाए। उन्होंने पत्रिका ‘साइंस' में अपनी चिंता व्यक्त की है।
विशेषज्ञों ने यह माना कि कई उद्योग और देश उपग्रह संवहनीयता पर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इसे हर देश को पृथ्वी की कक्षा का इस्तेमाल करने की योजनाओं में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में उपग्रहों और मलबे के लिए उत्पादक तथा ग्राहक की जिम्मेदारी को लागू करने के उपाय भी शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाबदेही को बढ़ावा देने के तरीकों पर गौर करते हुए वाणिज्यिक लागत पर भी विचार किया जाना चाहिए।
ऐसे विचार समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के प्रस्तावों के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि विभिन्न देशों ने वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ के अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता इमोजेन नैपर ने कहा, ‘‘प्लास्टिक प्रदूषण और हमारे समुद्र के सामने आ रही अन्य चुनौतियां अब दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।
हालांकि, इस पर सीमित कार्रवाई की गयी है और क्रियान्वयन धीमा रहा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘अब हम अंतरिक्ष में मलबा एकत्रित होने की ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। समुद्र में कचरा एकत्रित होने से हमने क्या सीखा, उस पर विचार करते हुए हम गलतियां दोहराने से बच सकते हैं और अंतरिक्ष में ऐसी ही त्रासदी को रोकने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक समझौते के बिना हम अपने आप को एक ही राह पर खड़े देख सकते हैं।फाइल फोटो
- राजस्थान का चित्तौडग़ढ़ किला जिसे 'भारत का सबसे विशाल किला' कहा जाता है। इसके निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह किला चित्तौडग़ढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले पर अलग-अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा है।आठवीं सदी में यहां गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्यवंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक भी शासन रहा। इसपर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनकी कहानियां इतिहास में अमर हैं।करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई एतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहां 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजूओं में बांधे रखते थे।इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल दरवाजे बने हुए हैं। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन सातों के नाम हैं- पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पाड़ा (भैंसा) बहता हुआ यहां तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पाडन पोल पड़ा। यहां मौजूद हर दरवाजे की एक अलग कहानी है।कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौडग़ढ़ किले में एक लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा-रानी से लेकर दास-दासियां और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहां पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतनसिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16 हजार दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा 16वीं सदी में यहां रानी कर्णावती ने 13 हजार दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों के बाद रानी फुलकंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था। ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक हैं।इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्यवंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने सातवीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। किवदंती के अनुसार, एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे, तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिसपर योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर दे तो देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों-रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाईयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था, सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होता देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकड़ेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिससे भीम समझें कि सुबह हो गई है। कुकड़ेश्वर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लत-लाताब के नाम से जानते हैं।
-
रोज 11 मिनट टहलने से जल्दी मृत्यु का खतरा कम होता है : कैंब्रिज विश्वविद्यालय का अध्ययन
लंदन. रोज केवल 11 मिनट या सप्ताह में 75 मिनट टहलने या मध्यम स्तर की शारीरिक गतिविधि से हृदय रोग और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। कैंब्रिज विश्वविद्यालय की अगुवाई में किए गए एक नए शोध में यह कहा गया है। ‘ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन' में मंगलवार को प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि जल्दी मृत्य के 10 मामलों में से एक को रोका जा सकता है यदि हर कोई ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) द्वारा अनुशंसित शारीरिक गतिविधि की आधी सलाह पर भी अमल करे। मध्यम स्तर की शारीरिक गतिविधि से हृदय संबंधी रोगों और कैंसर का खतरा घटता है और एनएचएस ने वयस्कों को एक सप्ताह में 75 मिनट मध्यम स्तर की शारीरिक गतिविधि करने की सलाह दी है। कैंब्रिज विश्वविद्यालय में मेडिकल रिसर्च काउंसिल (एमआरसी) एपिडेमिओलॉजी यूनिट से जुड़े डॉ. सोरेन ब्राज ने कहा, ‘‘कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ शारीरिक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक सप्ताह में 75 मिनट की शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं तो धीरे-धीरे आपको अनुशंसित स्तर तक गतिविधि को बढ़ानी चाहिए।'' दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें हृदय संबंधी रोगों के कारण होती है। वर्ष 2019 में 1.79 करोड़ लोगों की मौत हृदय रोगों से हुई वहीं 2017 में 96 लाख लोगों ने कैंसर से दम तोड़ दिया। अध्ययन के मुताबिक एक सप्ताह में 75 मिनट शारीरिक गतिविधि से हृदय संबंधी रोगों का खतरा 17 प्रतिशत और कैंसर का खतरा सात प्रतिशत तक कम हो जाता है। - आपने टिड्डों के सिर पर निकली लंबी सी डंडी देखी होगी, इन्हें एंटेना कहा जाता है। ये एंटेना अब बीमारियों का जल्द पता लगाने और सुरक्षा जांच को ज्यादा मुस्तैद बनाने में मददगार बनेंगे।इन एंटेनों का इस्तेमाल करके इजरायली शोधकर्ताओं ने सूंघने वाला एक खास रोबोट बनाया है। इस रोबोट में बायोलॉजिकल सेंसर लगे हैं। इन सेंसरों में टिड्डों का एंटेना इस्तेमाल किया गया है। टिड्डों में सूंघने की गजब क्षमता होती ह। वह एंटेना के सहारे सूंघते ह। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने टिड्डों की इसी क्षमता का इस्तेमाल बायो-हाइब्रिड रोबोट बनाने में किया है। उनका कहना है कि टिड्डों के एंटेना की मदद से ये रोबोट मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक स्निफर्स के मुकाबले ज्यादा कारगर हो सकते हैं।शोधकर्ताओं ने टिड्डों के एंटेना को रोबोट के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच लगाया, जो कि नजदीकी गंध सूंघकर इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। हर गंध का अपना एक खास सिग्नेचर होता है। मशीन लर्निंग की मदद से रोबोट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनकी पहचान कर सकता है। सागोल स्कूल ऑफ न्यूरोसाइंस की शोधकर्ता नेता श्विल ने रॉयटर्स को बताया, "हम ऐसा रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सूंघने की काबिलियत हो और जो अलग-अलग गंधों के बीच फर्क भी कर सकता हो। साथ ही, वो यह भी पता लगा सकता हो कि गंध कहां और किस चीज से आ रही है। "टिड्डे अपने संवेदनशील एंटेना का इस्तेमाल कर अपने आस-पास की हवा के रासायनिक बदलाव का पता लगाते हैं। इससे उन्हें करीबी आबोहवा की रासायनिक गंध के बारे में बहुत तेज और सटीक जानकारी मिलती है। सूंघने की ऐसी क्षमता कई और कीट-पतंगों में भी पाई जाती है। इनके मुकाबले इंसानों की सूंघने की क्षमता बहुत सीमित है। वैज्ञानिक लंबे समय से जानवरों के जैविक सूंघने वाले सेंसरों पर प्रयोग कर रहे हैं। इसकी मदद से एक बायो-हाइब्रिड सेंसर विकसित करने में कामयाबी मिली है, जो जीवों के जैविक सेंसरों और इलेक्ट्रॉनिक पुरजों का खास मिश्रण है।2022 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी टिड्डों के दिमाग और एंटेना की मदद से मुंह के कैंसर की पहचान की तकनीक विकसित की थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस तकनीक के लिए फिलहाल छह से 10 टिड्डों की जरूरत होती है। शोधकर्ता इस संख्या को घटाने की कोशिश पर काम कर रहे हैं। कीट-पतंगों के अलावा कुत्तों की सूंघने की शक्ति का भी दशकों से इस्तेमाल किया जाता रहा है।----
-
सिंगापुर. सूक्ष्म प्लास्टिक (माइक्रोप्लास्टिक) या पांच मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक कणों को लेकर वैज्ञानिकों की यह चिंता बढ़ती जा रही है कि क्या ये मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं? अध्ययन दर्शाते हैं कि ये कण हमारे पर्यावरण में, घरों तथा दफ्तरों में रोजमर्रा की चीजों में, समुद्र में, नदियों में, मिट्टी में और बारिश आदि सभी में व्यापक रूप से मौजूद हैं। लोग समय के साथ-साथ इस तरह के जितने रसायन शरीर से निकालते हैं, उससे ज्यादा कण उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। हाल में एक विश्लेषण में प्लास्टिक में इस्तेमाल ऐसे 10,000 से अधिक विशिष्ट रसायनों की पहचान की गयी जिनमें से अधिकतर वैश्विक रूप से सही से विनियमित नहीं हैं। अनुसंधान बताते हैं कि हम हर दिन कहीं भी एक लाख से अधिक तक सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को शरीर में सोख लेते हैं। अब मछलियों में, सर्जरी कराने वाले रोगियों के शरीर में, अज्ञात रक्तदाताओं के खून में और स्तनपान कराने वाली माताओं के दूध में भी सूक्ष्म प्लास्टिक पाया जा रहा है। सूक्ष्म प्लास्टिक और उससे सेहत पर असर के बीच तार जुड़े होने की पुष्टि करने वाला कोई अध्ययन अभी तक सामने नहीं आया है, हालांकि अनुसंधानकर्ताओं ने इशारा किया है कि प्लास्टिक में पाये जाने वाले रसायन कैंसर, हृदय रोगों, मोटापा और भ्रूण का सही विकास नहीं होने जैसी अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हमारे शरीर में अधिक मात्रा में सूक्ष्म प्लास्टिक होने से कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है। सभी हितधारक इस बात को मानते हैं कि सूक्ष्म प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। अनुसंधानकर्ताओं ने प्रदूषण के बारे में अपनी चेतावनी में कहा कि सूक्ष्म प्लास्टिक की खपत से ऐसे स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं जिन्हें कम नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि मनुष्य के शरीर में हर सप्ताह पांच ग्राम प्लास्टिक कण पहुंच जाते हैं। यह एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर है। मवेशियों के आहार में प्लास्टिक होने से उस मांस और दुग्ध उत्पाद में सूक्ष्म प्लास्टिक पहुंच सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में करते हैं।
-
बच्चे के घर में जन्म लेते ही माता-पिता ही नहीं बल्कि पूरा परिवार उसे पुकारने के लिए एक प्यारा सा नाम ढ़ूंढने लगता है। इस काम के लिए लोग अपने आस-पास के लोगों से ही नहीं बल्कि इंटरनेट की भी मदद लेने से पीछे नहीं हटते हैं। यूं तो भारत में कानूनी तौर पर आप अपने बच्चे के लिए कोई भी नाम पसंद कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कई ऐसे देश हैं जहां माता-पिता को ये आजादी नहीं होती है। जी हां, आपको बता दें, कई ऐसे देश हैं जहां बच्चों के लिए कुछ नाम बैन किए गए हैं। बच्चों के लिए ये नाम रखने पर उनके माता-पिता को जेल तक हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देशों और नामों के बारे में।
फ्रांस-
फ्रांस में कोर्ट ने बच्चों के उन नामों को बैन किया हुआ है, जिनकी वजह से बच्चों का मजाक उड़ाया जा सकता है। वहां बैन किए गए नामों में स्ट्रोबेरी, न्यूटिला, डेमोन, प्रिंस विल्यिम, मिनी कॉपर ये नाम शामिल हैं।
स्विट्ज़रलैंड-
स्विट्ज़रलैंड में बच्चों के नाम सिविल रजिस्ट्रार की तरफ से अप्रूव करवाने अनिवार्य होते हैं। कोर्ट के नियमों के अनुसार बच्चे का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके या फिर किसी की भावना को उस नाम से ठेस पहुंच सकें। खासकर बाइबिल में मौजूद किसी बुरे व्यक्ति के नाम पर, किसी ब्रांड, जगह या सरनेम के नाम पर बच्चे का नाम नहीं रखा जा सकता है। स्विट्जरलैंड में जुडस, चैनल, पेरिस, मर्सिडिज जैसे कुछ नामों पर बैन लगा हुआ है।
न्यूजीलैंड-
न्यूजीलैंड में भी नाम को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। यहां कोई अपने बच्चे का नाम प्रिंस, प्रिंसेस, किंग, मेजर, सार्जेंट और नाइट नहीं रख सकता है।
मेक्सिको-
मेक्सिको देश के सोनोरा में बच्चों के 61 नामों पर पाबंदी है। ये सभी वो नाम हैं जो बेहद अपमानजनक हैं, या फिर दूसरों को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन नामों में फेसबुक, रामबो, हेरमोनी, बेटमैन नाम शामिल हैं।
जर्मनी-
जर्मनी में बच्चों के नाम को रखने के लिए काफी सख्त नियम, कानून बनाए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक लड़के और लड़कियों के नाम एक जैसे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा किसी खाद्य पदार्थ के नाम पर भी बच्चों का नाम रखने पर पूरी तरह पाबंदी है। यहां जिन नामों पर बैन है उनमें माटी, ओसामा बिन लादेन, एडोल्फ हिटलर शामिल हैं। -
नयी दिल्ली. मध्य भारत की नर्मदा घाटी में अनुसंधानकर्ताओं ने सबसे बड़े डायनॉसौर में से एक टाइटानोसॉरस के कुल 256 जीवाश्म अंडों वाले 92 घोंसलों का पता लगाया है। इस खोज के बारे में जर्नल पीएलओएस वन में प्रकाशित लेख में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले टाइटनोसॉरस के जीवन के कुछ अनकहे विवरण का पता चलता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, मध्य भारत की नर्मदा घाटी में स्थित 'लेमेटा फॉर्मेशन' डायनॉसौर के कंकालों और अंडों के जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग 14.5 से 6.6 करोड़ साल पहले समाप्त हो गए थे। इन घोंसलों की विस्तृत जांच के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और उनके सहयोगियों ने डायनॉसौरों के बारे में कई तरह के अनुमान लगाए हैं। इसके लिए उन्होंने अंडे की ही छह अलग-अलग प्रजातियों की पहचान की जो इस क्षेत्र में टाइटनोसॉरस की उच्च विविधता को दर्शाते हैं। घोंसले के बाहरी आवरण के आधार पर, शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि इन डायनॉसौरों ने आधुनिक समय के मगरमच्छों की तरह अपने अंडों को उथले हुए गड्ढों में दबाया होगा। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि अंडों से संकेत मिलता है कि टाइटनोसॉरस सॉरोपोड्स में पक्षियों की तरह एक प्रजनन संरचना होती थी। वह संभवत आधुनिक पक्षियों में देखे जाने वाले क्रमिक तरीके से अपने अंडे देता था। वहीं, एक ही क्षेत्र में कई घोंसलों की मौजूदगी से पता चलता है कि ये डायनॉसौर कई आधुनिक पक्षियों की तरह ही सामूहिक रूप से अपने घोंसले का निर्माण करते थे। हालांकि, इन घोंसलों के बीच की कम दूरी ने व्यस्क डायनॉसौर के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है जिससे लगता है कि शायद वयस्कों ने नवजात बच्चों को अपना पेट भरने की जिम्मेदारी बहुत जल्द सौंप दी। शोधकर्ताओं ने बताया कि ये अंडे डायनॉसौर के इस धरती से समाप्त होने से कुछ पहले के हैं और उनके बारे में अहम जानकारियां दे सकते हैं।
-file photo
-
बेंगलुरु. कनाडा स्थित मैकगिल विश्वविद्यालय और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के खगोलविदों ने एक सुदूर आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन से निकलने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। इस रेडियो सिग्नल को पकड़ने के लिए उन्होंने पुणे स्थित ‘जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप' (जीएमआरटी) के डेटा का इस्तेमाल किया। आईआईएससी के एक बयान में कहा गया, "जिस खगोलीय दूरी पर यह सिग्नल पकड़ा गया है, वह अब तक अंतर के मामले में सबसे बड़ा है। यह किसी आकाशगंगा से 21 सेमी का उत्सर्जन दिखने की पहली पुष्टि भी है।" इस खोज से संबंधित निष्कर्ष 'मंथली नोटिसेज ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। परमाणु हाइड्रोजन किसी आकाशगंगा में तारे के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ईंधन है। जब आकाशगंगा के आसपास से गर्म आयनित गैस आकाशगंगा पर गिरती है, तो गैस ठंडी हो जाती है और परमाणु हाइड्रोजन बनाती है। इसके बाद यह आणविक हाइड्रोजन बन जाती है, और फिर तारों का निर्माण होता है। बयान में कहा गया, "इसलिए, ब्रह्मांडीय समय के अनुरूप आकाशगंगाओं के विकास को समझने के लिए विभिन्न ब्रह्मांडीय युगों में तटस्थ गैस के विकास का पता लगाने की आवश्यकता है।" परमाणु हाइड्रोजन 21 सेमी तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करती है, जिसका पता जीएमआरटी जैसी कम आवृत्ति वाले रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके लगाया जा सकता है। इस प्रकार, 21 सेमी उत्सर्जन निकट और सुदूर-दोनों तरह की आकाशगंगाओं में परमाणु गैस सामग्री का प्रत्यक्ष अनुरेखक है। हालांकि, यह रेडियो संकेत बेहद कमजोर है और इसकी सीमित संवेदनशीलता के कारण वर्तमान दूरबीनों का उपयोग कर सुदूर आकाशगंगा से उत्सर्जन का पता लगाना लगभग असंभव है। जीएमआरटी डेटा का उपयोग करते हुए मैकगिल विश्वविद्यालय के फिजिक्स एंड ट्रॉटियर स्पेस इंस्टिट्यूट के अनुसंधानकर्ता अर्नब चक्रवर्ती और आईआईएससी के भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर निरुपम रॉय ने सुदूर आकाशगंगा में ‘रेडशिफ्ट जेड=1.29' पर परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न रेडियो संकेत का पता लगाया। चक्रवर्ती ने कहा कि जब तक स्रोत से संकेत दूरबीन तक पहुंचा तब तक आकाशगंगा की अत्यधिक दूरी के कारण 21 सेमी उत्सर्जन रेखा 48 सेमी तक फैल गई। पकड़ा गया संकेत संबंधित आकाशगंगा से तब उत्सर्जित हुआ था जब ब्रह्मांड केवल 4.9 अरब वर्ष पुराना था। दूसरे शब्दों में कहें इस स्रोत के इतिहास को देखने का समय 8.8 अरब वर्ष है।
- जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। इसे पोंगल के अवसर पर खेला जाता है। इंसान और सांड के बीच होने वाली लड़ाई में काफी लोग घायल होते हैं , कई बार लोगों की जान तक चली जाती है।जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य का एक परंपरागत खेल है , जो वहां के गांवों में बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। इसे दक्षिण भारत के कृषि प्रधान विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दरअसल, वर्ष का दिसम्बर और जनवरी माह तमिलनाडु में फसल कटाई का मौसम होता है। फसल कटने के बाद वहां चार दिनों तक 'पोंगलÓ उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का तीसरा दिन पशु को समर्पित होता है और इसी दिन लोग जल्लीकट्टूू का खेल खेलते हैं। परंपरा के अनुसार खेल की शुरुआत में तीन बैलों (सांड) को खुला छोड़ दिया जाता है और इसे कोई नहीं पकड़ता है। ये तीनों बैल उस गांव के सबसे बूढ़े बैल होते हैं जिन्हें गांव की शान समझा जाता है.। इन तीनों बैलों के जाने के बाद जल्लीकट्टू खेल का आगाज होता है।इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों के सींग में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में कई लोग न सिर्फ घायल होते हैं बल्कि अनहोनी की स्थिति में जान जाने की आशंका भी बनी रहती है। हर साल अनहोनी की एक-दो घटनाएं होती भी हैं। अंतत: जो भी बैल को काबू में करने और उसके सींग पर बंधे सिक्कों के थैले को प्राप्त करने में सफल होता है उसे खेल का विजेता घोषित कर इनाम दिया जाता है।जल्लीकट्टू तमिल शब्द जल्ली और कट्टू से मिलकर बना है। जल्लीकट्टूू पौराणिक शब्द सल्लिकासु का अपभ्रंश है जहां सल्ली का अर्थ है सिक्के की थैली और कासु का तात्पर्य बैल के सींग से हैै। कहा जाता है कि जल्लीकट्टूू तमिलनाडु की लगभग 2500 वर्ष पुरानी परंपरा हैै। पौराणिक काल में योद्धा लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस खेल का सहारा लेते थे। इस खेल के माध्यम से कुंवारी कन्याएं अपने वर का चुनाव करती थीं। यह सब उस स्वयंवर की तरह ही होता था, जिसमें किसी खास लड़की से शादी करने के लिए इच्छुक युवकों को ताकतवर बैल को काबू में करने की चुनौती मिलती थी और जो उसे काबू में कर लेता था उसे ही उस लड़की को अपना वर चुनना होता था।
- कार के आकार का कछुआ. इतना बड़ा कछुआ इंसान ने तो नहीं देखा है लेकिन 8.3 करोड़ साल पहले यानी जब धरती पर डायनासोर हुआ करते थे तब इतने बड़े आकार के कछुए भी थे। इसका पता वैज्ञानिकों को अभी चला है जब स्पेन में उसके अवशेष मिले ।स्पेन में शोधकर्ताओं को एक कछुए के अवशेष मिले हैं। अवशेष दिखाते हैं कि यह कछुआ एक छोटी कार के आकार का रहा होगा। शोधकर्ताओं ने बताया है कि उत्तरी स्पेन में मिला यह कछुआ 12 फुट लंबा होगा। उसका वजन दो टन से कुछ कम रहा होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कछुआ क्रेटेसियस युग में जीवित था। यह वो युग था जबकि डायनासोर युग का अंतिम चरण चल रहा था। यूरोप में अब तक का यह सबसे बड़ा कछुआ है।इस वक्त पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा कछुआ जीवित है, उसे लेदरबैक कछुआ कहते हैं। उसकी लंबाई सात फुट तक हो सकती है। उत्तरी स्पेन में जो अवशेष मिले हैं, उस कछुए को वैज्ञानिकों ने लेवियाथानोचेलिस नाम दिया है। लेवियाथानोचेलिस विशालतम ज्ञात कछुए से कुछ ही छोटा है।दूसरा सबसे बड़ा कछुआविश्व इतिहास का सबसे बड़ा कछुआ आर्चेलोन था, जो सात करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहता था। यह कछुआ 15 फुट लंबा था। इस शोध में शामिल रहे जीवविज्ञानी एल्बर्ट सेलेस कहते हैं कि लेवियाथानोचेलिस मिनी कूपर जितना लंबा था जबकि आर्चेलोन टोयोटा कोरोला जितना। सेलेस बार्सिलोना विश्वविद्यालय के पेलियंथोलॉजी इंस्टिट्यूट में पढ़ाते हैं। वह बताते हैं कि जिस युग में लेवियाथानोचेलिस जीवित था, उस दौर में इतना विशाल होना काफी सहूलियत भरा रहा होगा, क्योंकि जिस प्राचीन टेथीस सागर में वह तैरता था, वहां जानवरों की भारी भीड़ रहती थी।टेथीस सागर में मोजासॉरस नामक विशालकाय जीव होते थे जिनकी लंबाई 50 फुट तक हो सकती थी। वे सबसे बड़े शिकारी जीव थे और बेहद खतरनाक होते थे। इसके अलावा कई तरह की शार्क मछलियां और लंबी गर्दन वाले मत्स्याहारी (मछली खाने वाले मांसाहारी) जीव भी लेवियाथानोचेलिस के लिए बड़ा खतरा होते थे।इस रिसर्च रिपोर्ट के मुख्य लेखक पोस्ट ग्रैजुशन के छात्र ऑस्कर कास्टिलो हैं जो बार्सिलोना विश्वविद्यालय में पेलियंथोलॉजी पढ़ रहे हैं। वह कहते हैं, ''महासागरीय जीवन के संदर्भ में लेवियाथानोचेलिस के आकार के किसी प्राणी पर हमला करना विशालतम शिकारियों द्वारा ही संभव हो पाता होगा। उस वक्त यूरोपीय इलाके में ऐसे विशाल शिकारी मोजारस और शार्क ही थे। '' कास्टिलो की यह खोज साइंटिफिक रिपोट्र्स नाम की विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुई है। वह बताते हैं, ''क्रेटासियस युग में महासागरीय कछुओं में अपने शरीर का आकार बढ़ाने की प्रवृत्ति थी। लेवियाथानोचेलिस और आर्चेलोन इस प्रक्रिया के सबसे सटीक उदाहरण कहे जा सकते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि अपने आसपास के विशालकाय शिकारी जीवों से बचने के लिए ऐसा होता होगा। ''
-
नयी दिल्ली. दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुके स्मार्टफोन अब लोगों के रिश्तों में खटास बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट उपकरण विनिर्माता वीवो के एक अध्ययन में सोमवार को बताया गया कि स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से भारत में विवाहित जोड़ों के संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। साइबर मीडिया के अध्ययन ‘‘स्मार्टफोन और मानवीय संबंधों पर उनका असर 2022' में 67 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने के दौरान भी वे अपना फोन देखने में व्यस्त रहते हैं। वहीं 89 प्रतिशत ने कहा कि अपने जीवनसाथी के साथ हल्की-फुल्की बातचीत में उन्होंने कम वक्त दिया जबकि वे चाहते तो अधिक समय दे सकते थे। इसमें स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं ने यह माना कि आमने-सामने की बातचीत ज्यादा राहत देनी वाली होती है लेकिन इसके लिए वे कम वक्त देते हैं। इसमें कहा गया, ‘‘अध्ययन में शामिल लोगों में से 84 प्रतिशत ने कहा कि वे अपने जीवनसाथी के साथ और वक्त गुजारना चाहते हैं। लोग समस्या को स्वीकार कर रहे हैं और इसे बदलने के लिए भी तैयार हैं। 88 प्रतिशत लोगों ने यह माना कि स्मार्टफोन के अधिक इस्तेमाल का असर जीवनसाथी के साथ उनके रिश्ते पर पड़ रहा है।'' इसमें 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अपने जीवनसाथी के साथ अर्थपूर्ण बातचीत करके ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। अध्ययन के मुताबिक, स्मार्टफोन उपयोगकर्ता प्रतिदिन औसतन 4.7 घंटे इस उपकरण को देखते हुए बिताते हैं और यह अवधि पति और पत्नी दोनों के लिए एक समान है। 73 प्रतिशत ने कहा कि उनके जीवनसाथी की यह शिकायत रहती है कि वे उनके साथ अधिक समय बिताने के बजाय फोन में ज्यादा उलझे रहते हैं। इसमें कहा गया, ‘‘अध्ययन में पता चला कि 70 प्रतिशत लोग जब स्मार्टफोन देख रहे होते हैं और ऐसे में उनका जीवसाथी उनसे कुछ कहता है तो वे झल्ला जाते हैं। 66 प्रतिशत ने यह महसूस किया कि स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से जीवनसाथी के साथ उनका संबंध कमजोर हुआ है।'' यह अध्ययन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद तथा पुणे में 1,000 लोगों पर किया गया। वीवो इंडिया के प्रमुख (ब्रांड रणनीति) योगेंद्र श्रीरामुला ने कहा, ‘‘आज के जीवन में स्मार्टफोन का महत्व निस्संदेह है लेकिन इसके अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर उपयोगकर्ताओं को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। -
नयी दिल्ली. दिल का दौरा पड़ने के मामले आमतौर पर 'मोटापे' और 'उच्च कोलेस्ट्रॉल' के शिकार लोगों के बीच देखने को मिलते हैं, लेकिन हाल ही में युवाओं में सामने आईं ऐसी घटनाएं एक अलग और चिंताजनक तस्वीर पेश करती हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें सैर, जिम में कसरत जैसी रोजमर्रा की गतिविधियां करते और शादी में नाचते समय लोग हृदयाघात के शिकार हो गए। ऐसे में प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञों का मानना है कि 'असामान्य व्यायाम' या 'अति व्यायाम' युवाओं में दिल के दौरे का कारण बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों में, हृदयाघात के मामलों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से 25 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के बीच। हाल ही में कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, गायक केके और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जैसी कई हस्तियों का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसके बाद हृदयाघात के बारे में कुछ व्यापक रूप से गलत धारणाएं सामने आई हैं और उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. नीतीश नाइक कहते हैं, “हृदय को रक्त और पोषण की आपूर्ति करने वाली धमनियों में अचानक रुकावट के कारण दिल का दौरा पड़ता है।” फोर्टिस अस्पताल, नोएडा के ‘कार्डियक साइंसेज' के अध्यक्ष और ‘कार्डियक सर्जरी' के प्रभारी डॉ. अजय कौल बताते हैं, "धमनी में वसा की परत का निर्माण होता है। यह परत टूटकर रक्त वाहिका में प्रवेश कर जाती है, जिससे वाहिका में रक्त का थक्का बन जाता है, और वह बंद हो जाती है।" नाइक कहते हैं, "धूम्रपान के आदी, सुस्त जीवन शैली वाले, मोटापे, खराब रक्तचाप से ग्रस्त, मधुमेह से पीड़ित या उच्च कोलेस्ट्रॉल के शिकार लोगों के साथ इस तरह की दिक्कत हो सकती हैं।" उन्होंने कहा कि इसके केवल यही कारण नहीं हैं। जिम में अत्यधिक कसरत करने से भी ऐसा हो सकता है।
पैन मैक्स- कार्डिएक साइंसेज में कैथ लैब के प्रमुख निदेशक और प्रमुख डॉ. विवेक कुमार कहते हैं, "अनियमित व्यायाम से दिल का दौरा पड़ सकता है, इसलिए बिना प्रशिक्षण के व्यायाम नहीं करना चाहिए।" उजाला सिग्नस ब्राइटस्टार हॉस्पिटल, मुरादाबाद के सीनियर कंसल्टेंट और ‘इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट' डॉ. विजया कुमार कहते हैं, "हां, ज्यादा व्यायाम करने से कोरोनरी वाहिकाओं में जमी परत फट सकती है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है।" नयी दिल्ली के पटपड़गंज में स्थित मैक्स अस्पताल में हृदय रोग विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर विनीत भाटिया ने कहा, "आंकड़ों की बात की जाए तो युवाओं में इसके 15-18 प्रतिशत मामले होते हैं।" लेकिन युवाओं में हृदयाघात के मामले केवल अत्यधिक व्यायाम के कारण नहीं देखे गए हैं। कोविड से भी दिल का दौरा पड़ने के मामले बढ़े हैं। कौल कहते हैं, "यह सच है कि कोविड ने बहुत दिक्कतें पैदा की हैं। कोविड से रक्त के थक्के जम सकते हैं। कोविड से हृदय और फेफड़ों की समस्याएं पैदा होती हैं।" ऐसे में सवाल उठता है कि कोई कैसे जान सकता है कि कोविड या अधिक व्यायाम हृदय की समस्याओं का कारण है? कौल कहते हैं, "मूल्यांकन। किसी डॉक्टर के पास जाएं, और वह आपको बताएगा कि क्या कोविड केवल आपके फेफड़ों तक ही सीमित था या नहीं।" कोविड के खिलाफ लड़ाई में टीकों का अहम योगदान रहा है। हालांकि, कोविड रोधी टीके कुछ मामलों में हृदयाघात का कारण भी बने हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों से कितना चिंतित होने की जरूरत है? इस बारे में कौल कहते हैं, "लाभ, जोखिमों से कहीं अधिक हैं। टीकाकरण में कई अन्य समस्याएं हैं। हां, ऐसा है। लेकिन संख्या इतनी कम है कि उन्हें अनदेखा किया जा सकता है। दूसरा, यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोविड हृदय की समस्याओं को और अधिक बढ़ा सकता है -
आमतौर पर रोमांस या स्नेह से जोड़े जाते चुंबन की शुरुआत बेहद दिलचस्प है. वहीं बीच में ऐसा भी दौर आया, जब कई सरकारों ने इसपर बैन लगा दिया. मसला जितना दिलचस्प हो, उसपर बातें भी उतने ही तरह की होंगी, किस के साथ भी कुछ ऐसा ही है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग-अलग थ्योरी देते हैं कि चुंबन की शुरुआत कैसे और कहां से हुई होगी.
हां, एक बात लगभग सभी कहते हैं कि पहला किस एक हादसा रहा होगा. हादसा, जो पसंद आ गया.
शुरुआत मां के बच्चों को खाना खिलाने से हुई होगी. पहले पशु भी खाने का निवाला या अनाज-फल सीधे बच्चों के मुंह में नहीं डालते थे, बल्कि चबाया हुआ कौर मुंह से मुंह में दिया जाता. इसे प्रीमेस्टिकेशन फूड ट्रांसफर कहते हैं. ह्यूमन इवॉल्यूशन इसी तरह से हुआ होगा. चिंपाजियों में अब भी ऐसा होता है. और चिंपाजी मांएं अपने बच्चों को दुलारते हुए किस भी करती हैं. तो ये भी हो सकता है कि हमने अपने पूर्वजों की देखादेखी चुंबन का लेनदेन सीख लिया हो.
दूसरी थ्योरी भी है, जिसके मुताबिक चुंबन एक एक्सिडेंट की देन है. टेक्सास ए एंड एम यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने इसपर भारी स्टडी की और क्लेम किया कि सूंघते हुए हमने एकाएक एक-दूसरे को चूम लिया होगा. यहीं से हुई शुरुआत. बात में थोड़ा दम इसलिए भी है कि पुराने समय में एक-दूसरे को मिलते हुए सूंघने का चलन था. बहुत सी सोसायटी में सूंघना ही एक तरह का अभिवादन था. सूंघते हुए ही एकाएक किसी जोड़े ने चुंबन ले लिया होगा. ये नई चीज है. शायद ज्यादा लुभावनी और ज्यादा करीबी लगने वाली.
माना जाता है कि चुंबन की शुरुआत इसी तरह से और वो भी हमारे ही देश से हुई. बाद में प्राचीन ग्रीक भारत आए और लौटते हुए चुंबन का कंसेप्ट भी साथ ले गए. इसी तरह से ये पूरी दुनिया में फैला.
भले ही चुंबन को अक्सर प्यार जताने की भंगिमा की तरह देखा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं. कम से कम पुराने समय में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. मध्यकालीन यूरोप में इसे ग्रीटिंग की तरह देखा जाता, जो हल्के ओहदे वाले लोग ऊंचे ओहदेदारों के साथ करते. दो बराबरी के लोग आपस में मिलते हुए माथे या होठों पर किस करते, जबकि गैर-बराबरी की मुलाकात में केवल नीचे के ओहदे वाला ही ऊपर वाले को चूमता, वो भी हाथ या पैर या फिर कपड़े के किनारे को.
इसके बाद चुंबन का रूप और गहराता गया. ये ज्यादा इंटेन्स हो गया. खासकर होठों पर चुंबन प्यार का प्रतीक बनने लगा. हालांकि फिलहाल किस के जिस स्वरूप पर फ्रांस अपना ठप्पा लगाता है, उसकी शुरुआत किसी फ्रांसीसी जोड़े से हुए होगी, इसपर काफी लट्ठम-लट्ठ हो चुकी. ये बात अलग है कि तगड़ी दावेदारी फ्रांस की ही है.
लगभग एक दशक पहले ही इस देश ने देर तक चुंबन को अपनी डिक्शनरी में शामिल करते हुए उसे एक नाम दिया- गलॉश. साथ में ये दावा भी ठोक दिया कि पहले वर्ल्ड वॉर के समय फ्रांस में समय बिता चुके अमेरिकी सैनिकों ने उनका ये भेद जान लिया और यहां-वहां फैला दिया. बता दें कि पश्चिम के कई मुल्क फ्रेंच किस पर अपनी मुहर लगाना चाहते हैं. कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसके लिए अलग-अलग तरह के हवाले देते हैं.
मिसाल के तौर पर रोमन शासक टाइबेरिअस ने होठों पर चुंबन पर बैन लगा दिया क्योंकि इससे यौन रोग फैलने का डर रहता था. शासक का राज काफी दूर-दराज तक फैला हुआ था. इजीप्ट से लेकर इटली-जर्मनी और बेल्जियम-स्विटजरलैंड का बड़ा हिस्सा उसके कब्जे में था, यानी इन सारे इलाकों में चूमना प्रतिबंधित हो गया. यहीं से गाल चूमने का चलन आया होगा, जो कि अब पश्चिम समेत हमारे यहां भी खूब जोरों पर है. वैसे बैन की बात चल ही निकली है तो बता दें कि 17वीं सदी में जब दुनिया का बड़ा हिस्सा प्लेग से दम तोड़ रहा था, तब भी ब्रिटेन समेत कई देशों ने चूमने पर रोक लगा दी. न मानने वाले को सजा के तौर पर भारी जुर्माना देना होता.
अमेरिका, जो अब अपने खुलेपन और लोकतांत्रिक तौर-तरीकों के लिए जाना जाता है, वहां एक समय ऐसा भी था, जब सार्वजनिक तौर पर किसिंग को शिष्टाचार से बाहर माना गया. ये बात पहले विश्व युद्ध के बाद की है. तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति केल्विन कूलिज ने इसे बैड मैनर्स की लिस्ट में रखा. इसके बाद शिष्टाचार सिखाने वाली एक लेखिका एमिली पोस्ट ने अपनी मैगजीन में इसे जगह दी.
चुंबन सुनते ही सबके जेहन में कोई न कोई रोमांटिक तस्वीर बनती है, लेकिन ये उतना रोमांटिक है नहीं, जितना हमने मान रखा है. कम से कम दुनिया की 54 प्रतिशत आबादी तो यही सोचती है. अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने कुछ साल पहले एक रिसर्च की, जिसमें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के 168 कल्चर्स को शामिल किया गया. इसमें पता लगा कि सिर्फ 46 प्रतिशत लोग ही हैं जो चुंबन को रोमांस से जोड़ते हैं, खासकर होठों पर चुंबन. बाकियों ने चुंबन के इस रूप को रोमांस से जोड़ने से साफ इनकार कर दिया.
दुनिया के कई हिस्से हैं, जहां चुंबन को अब भी खराब माना जाता है, जैसे सोमालिया में इसे बीमारी फैलाने की साजिश की तरह देखते हैं. इसी तरह से बोलिविया का सिरिओनो ट्राइब किसिंग से एकदम अछूता है. हो ये भी सकता है कि शायद एक-दूसरे को पहचानने, या प्रेम जताने के लिए वे आज भी सूंघने जैसी प्राचीन भंगिमा अपनाते हों.-sabhar
- डेमोडेक्स आठ-पैर वाले घुन परिवार का एक सदस्य है जो हमारे बालों के रोम में रहते हैं और कई स्तनधारियों की तेल ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। मनुष्यों में इस घुन की दो प्रजातियाँ ज्ञात हैं - डेमोडेक्स फॉलिकुलोरम, जो मुख्य रूप से हमारे चेहरे (विशेष रूप से पलकों और भौहों) पर बालों के रोम में रहते हैं, और डेमोडेक्स ब्रेविस, जो चेहरे और अन्य जगहों पर तेल ग्रंथियों में घर बनाते हैं। नवजात शिशुओं में डेमोडेक्स माइट्स नहीं होते हैं। वयस्क मनुष्यों पर उनकी तलाश करने वाले एक अध्ययन में, शोधकर्ता उन्हें केवल 14 प्रतिशत लोगों में देखकर पहचान सके। हालांकि, एक बार जब उन्होंने डीएनए विश्लेषण का उपयोग किया, तो उन्होंने जितने लोगों पर परीक्षण किया उन सभी पर यानी 100 प्रतिशत वयस्क मनुष्यों पर डेमोडेक्स के संकेत पाए। यह एक ऐसी खोज थी जो इस संबंध में पहले हो चुके परीक्षणों का समर्थन कर रही थी। यदि वह पूरी मानवता में रहते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये घुन परजीवी हैं या हानिरहित जीव हैं और अपने अनजाने यजमानों के साथ सद्भाव से रहते हैं? और हमारी कौन सी दैनिक आदतें, जैसे चेहरा धोना और मेकअप लगाना, घुन के जीवित रहने में सहायता या बाधा डाल सकती हैं? यही सवाल मुश्किल हैं।डेमोडेक्स घुन बहुत छोटे होते हैं। दो मानव प्रजातियों में से बड़ी, डी. फोलिक्युलोरम, लगभग एक तिहाई मिलीमीटर लंबी होती है, जबकि डी. ब्रेविस एक चौथाई मिलीमीटर से भी कम होती है। वे अपने शरीर पर बैक्टीरिया की कई प्रजातियों को भी साथ रखते हैं। घुनों का सीधे पता लगाने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छा तरीका एक त्वचा बायोप्सी है जिसमें माइक्रोस्कोप स्लाइड पर साइनोएक्रिलेट ग्लू (सुपरग्लू) की थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। घुन की रहने की आदतें ऐसी होती हैं कि वह बालों में अकसर लगने वाली बेलनाकार रूसी में आराम से रह जाते हैं। ज़िट एक्सट्रैक्टर के साथ माइट्स को फॉलिकल्स से भी निकाला जा सकता है। घुन त्वचा की कोशिकाओं और वसामय तेलों को अपने भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें वे एंजाइमों की एक श्रृंखला को स्रावित करके पहले से पचा लेते हैं। चूंकि उनके शरीर में मलद्वार नहीं होते, वे अपने अपशिष्ट उत्पादों को मुंह से निकालते हैं। फॉलिकल में अपने आरामदायक घरों में रहते हुए ये नन्हे जीव साथी बनाते हैं और अंडे देते हैं; लगभग 15 दिनों के जीवनकाल के बाद, वे मर जाते हैं और कूप में वहीं सड़ जाते हैं। इनके इन्हीं खराब जीवनचक्र के कारण डेमोडेक्स कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है, और कई संबद्ध नैदानिक प्रभावों का कारण भी हो सकता है। फेस माइट्स कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं और हाल के अध्ययन डेमोडेक्स माइट्स से जुड़ी कई स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं: जैसे चकत्ते, त्वचा पर मुंहासे और फुंसियां , पलकों में सूजन, पलकों की तेल ग्रंथियों में रुकावट जिससे सिस्ट की समस्या हो सकती है, कॉर्निया में सूजन, शुष्क आंखें और आंख पर मांस बढ़ जाना। हालांकि इन स्थितियों के अन्य कारण भी हैं, लेकिन इनमें घुन की भूमिका को लेकर अधिक संदेह है।हालांकि, हम सभी की इन प्राणियों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब हम इनसे संक्रमित होते हैं, तो हमारे जीन हमारी प्रतिरक्षा और अन्य प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करते हैं घुन अपने परपोषी से अधिक समय तक जीवित नहीं रहते हैं। सीधे संपर्क के अलावा, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद संभवतः संक्रमण का रास्ता बनाते हैं। मेकअप ब्रश, चिमटी, आईलाइनर और काजल साझा करना शायद एक अच्छा विचार नहीं है, हालांकि साझा बाथरूम में संक्रमण से बचना मुश्किल हो सकता है। एक अध्ययन में, काजल में डेमोडेक्स के जीवित रहने का औसत समय 21 घंटे था। मेकअप के उपयोग के अन्य पहलू, जैसे नियमित सफाई और चेहरे की धुलाई, घुन की संख्या को कम कर सकते हैं, हालांकि अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि घुन अच्छी तरह से धोने से भी बच जाते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं है कि आप अपने घुन की आबादी को कितना प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको पलकों और आस-पास के क्षेत्रों में कोई सूजन है, तो मेकअप से परहेज करना और चिकित्सकीय सलाह लेना सबसे अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर, भले ही वे अप्रिय लगें, डेमोडेक्स हमारी त्वचा वनस्पतियों का एक सामान्य हिस्सा प्रतीत होता है। हालांकि, हममें से कुछ लोग उनकी उपस्थिति पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं और चकत्ते और सूजन से पीड़ित होते हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना उतना ही आसान हो सकता है जितना कि एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा निर्धारित धोने या उपचार के साथ घुन की संख्या को सीमित करना - बस यह जान लें कि हमारे घुन मित्रों से पूरी तरह से छुटकारा पाना शायद असंभव है।
- चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक किसी भी शाखा से खरीद सकती है. ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं. ये बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं, जो मांग पर वाहक को देने होते हैं.कब हुई थी शुरुआतचुनावी बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी. 29 जनवरी, 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA गवर्नमेंट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया था.कैसे काम करते हैं चुनावी बॉन्ड (Electoral bond)इलेक्टोरल बॉन्ड यूज करना काफी आसान है. ये बॉन्ड 1,000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं जैसे कि 1,000, ₹10,000, ₹100,000 और ₹1 करोड़ की रेंज में हो सकते हैं. ये आपको SBI की कुछ शाखाओं पर आपको मिल जाते हैं. कोई भी डोनर जिनका KYC- COMPLIANT अकाउंट हो इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकते हैं. और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट किया जा सकता है. इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है. इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वैरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता है. इलेक्टोरल बॉन्ड भी सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड रहते हैं.कब खरीदे जाते हैं ये बॉन्डचुनावी बॉन्ड हर तिमाही के पहले 10 दिन खरीदे जा सकते हैं. अप्रैल, जनवरी, जुलाई और अक्टूबर के शुरुआती 10 दिन सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के समय तय किए गए हैं. लोक सभा चुनाव के समय अलग से 30 दिन का समय भी सरकार तय कर सकती है.नियम और शर्तेंकोई भी पार्टी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29A के तहत पंजीकृत है और हाल के आम चुनावों या विधानसभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया है, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है. पार्टी को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा एक सत्यापित खाता आवंटित किया जाएगा और चुनावी बांड लेनदेन केवल इस खाते के माध्यम से किया जा सकता है.
-
चीन में मिलने वाली डा-हॉन्ग-पाओ-टी की. इस चाय पत्ती का नाम दुनिया में मिलने वाली सबसे महंगी चाय की पत्तियों में शुमार है। इसकी देखभाल में काफी मेहनत लगती है।
दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग चाय के शौकीन हैं। भारतीय लोगों के लिए तो चाय एक इमोशन है। आमतौर पर भारतीय दुकानों में 10 से 20 गिलास या कप चाय मिलती है, वहीं अगर कोई बड़े होटल- रेस्टोरेंट में चले जाएं तो 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की चाय मिलेगी।
लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के एक कोने में ऐसी चाय मिलती है, जो सबसे महंगी है. हम बात कर रहे हैं चीन में मिलने वाली डा-हॉन्ग-पाओ-टी की। यदि 1 किलो चाय खरीदना हो तो आपको लगभग 10 करोड़ रुपए कीमत अदा करनी होगी। जानकारी के मुताबिक डा हॉन्ग पाओ टी की खेती चीन के फोजियान के वूईसन इलाके में की जाती है, जिन पेड़ों में यह चाय लगती है वह रेयर पेड़ होते हैं और उन्हें मदर्स ट्री भी कहते हैं।
चीनी लोगों के मुताबिक इस चाय का इतिहास से बहुत ही पुराना है मिंग शासन के दौरान एक बार महारानी की तबीयत खराब हुई थी जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें यह चाय पिलाई। चाय ने कमाल दिखाते हुए महारानी को ठीक कर दिया था। यह पौधा बहुत ही दुर्लभ होता है। इसकी देखभाल में काफी मेहनत लगती है दवा तो यह भी किया जाता है कि इसे पीने से शरीर की कई गंभीर बीमारियों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। दुनियाभर में इसके सिर्फ 6 पेड़ मौजूद हैं।
--- -
सर्दी के मौसम की शुरूआत हो रही है. लेकिन इस सीजन की शुरूआत के साथ ही राजधानी दिल्ली की आबो-हवा भी खराब हो गई है. दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे सांस संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि जिन लोगों को पहले से ही फेफड़ों संबंधी कोई परेशानी है, उन्हें प्रदूषण के चलते और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसी लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस समय घरों के अंदर ही व्यायाम करने की सलाह दे रहे हैं. बाहर के अलावा आपके घर के अंदर की हवा भी साफ होनी चाहिए. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे घर की हवा को साफ रख सकते हैं.
Air Purifier है जरूरी
आपको बता दें कि घरों में लगे Air Purifier हमें प्रदूषण से होने वाली एलर्जी के तो बचाते ही हैं, साथ ही हमारे घर की हवा भी साफ करते हैं. बता दें कि Air Purifier में मौजूद HEPA फिल्टर्स 99.9 फीसदी तक हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं. हालांकि, प्रदूषक तत्वों को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता. लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है.
लगाएं Indoor Plants
घर के अंदर की हवा को साफ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप Indoor Plants लगाएं. आप ऐसे पौधें लगाएं, जो हवा को साफ कर सकते हों. आप चाहें तो एलोवेरा के पौधे को भी घर के अंदर रख सकते हैं. बता दें कि एलोवेरा कार्बनडाईऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखता है.
एसी के फिल्टर को करें चेक
सबसे जरूरी बात की आप अपने घर में लगे एसी के फिल्टर को चेक करते रहें. इसमें कई तरह के प्रदूषक तत्व रहने का अंदेशा रहता है. अगर आपको प्रोन एलर्जी की शिकायत है, तो आप अपने घर के एसी के फिल्टर को जरूर साफ करें. इसके अलावा, आप अपने घर में साफ-सफाई का भी ख्याल रखें. घर में गंदगी रहने से भी हवा में जहरीले तत्व शामिल हो जाते हैं. - पृथ्वी पर अधिकांश जानवर अकशेरुकी (रीढ़ की हड्डी के बिना) होते हैं - जैसे कि कीड़े, मकड़ी परिवार और कड़े खोल वाले जलजीव। ये अद्भुत जानवर हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं: वे परागणक, कीट नियंत्रक, मिट्टी निर्माता और अपशिष्ट प्रबंधक हैं। अकशेरूकीय अनगिनत अन्य जानवरों के भोजन के रूप में भी काम करते हैं। अपनी सारी मेहनत के बावजूद, इनमें से कई जीवों को अक्सर डरावने रेंगने वाले जीवों के रूप में वर्णित किया जाता है। उनके अजीब से दिखने वाले शरीर बुरे सपने की तरह लग सकते हैं, लेकिन अधिकांश अकशेरुकी प्रजातियां मनुष्यों के लिए हानिरहित हैं। वास्तव में, अकशेरुकी जीवों के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि वे हमारे ग्रह से चुपचाप गायब हो रहे हैं। यहां सात आकर्षक लेकिन डरावने रेंगने वाले जीवों के बारे में बात करते हैं, जिनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है।मकड़ियों (डेलेना कैंसराइड्स)ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, सामाजिक शिकारी मकड़ियों सूख चुके या सूख रहे पेड़ों की ढीली छाल के नीचे बड़े परिवार समूहों में रहती हैं। चिंता न करें, सोशल हंट्समैन मकड़ियां बेहद सौम्य होती हैं जो शायद ही कभी इंसानों को काटती हैं (और जब वे ऐसा करती हैं तो कम से कम नुकसान पहुंचाती हैं)। अधिकांश मकड़ी प्रजातियों के विपरीत, सामाजिक शिकारी एक बड़े वयस्क मादा वाले समूहों में एक साथ रहते हैं और उनकी 300 संतानें होती हैं। मकड़ियों बाहरी लोगों के खिलाफ आक्रामक रूप से अपने घर की रक्षा करती हैं, जिससे लगता है कि उनके पास अपने कबीले से बाहर वालों को पहचानने की क्षमता होती है। रात में, ये शिकारी कीड़ों का शिकार करने के लिए अपने सामुदायिक घर से बाहर निकलते हैं। शिकार मिलने पर यदि एक ही कीट के सामने कई सारी मकड़ियाँ होती हैं तो वह एक दूसरे से लड़ने के बजाय भोजन आपस में बांट लेती हैं। दरअसल, मकड़ी प्रजातियों एक साथी मकड़ी को खाने की बजाय भूख से मरना पसंद करेंगी। बड़ी संख्या में कीड़े खाकर, सामाजिक शिकारी या सोशल हाउंट्समन कीटों की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं।विशालकाय कॉकरोच (मैक्रोपेनेस्थिया रायनोसर्स)तिलचट्टे दुनिया के सबसे अधिक डरावने और निंदनीय कीड़े में से एक माने जाते हैं - जो उनके प्रति सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश तिलचट्टे हानिरहित जानवर हैं जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाले विशालकाय तिलचट्टे को लें। यह कोमल विशालकाय तिलचट्टे की दुनिया की सबसे भारी प्रजाति है, जिसका वजन तकरीबन 30-35 ग्राम होता है। अपने कुख्यात रिश्तेदारों के विपरीत, विशालकाय तिलचट्टा एक कीट नहीं है और अपना अधिकांश समय भूमिगत बिलों में बिताना पसंद करता है। विशालकाय तिलचट्टे यूकेलिप्टस के सूखे पत्तों का भोजन करते हैं, जिसे वे इकट्ठा करते हैं और अपनी बिल में खींच लेते हैं। इस दौरान मिट्टी को हिलाने और मिलाने से, विशालकाय तिलचट्टे मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। वे उत्कृष्ट माताएँ हैं जो जन्म के बाद नौ महीने तक अपने बच्चों को खिलाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। विशालकाय तिलचट्टा भी आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक जीवित रहता है, जिसकी उम्र 10 साल तक होती है।बैफोमेट कीट (क्रिएटोनोटोस गैंगिस)अजीब तरह से अपने अंगों को फुलाने वाले बैफोमेट कीट देखने में डरावने हो सकते हैं - लेकिन दरअसल ये पतंगे बस प्यार की तलाश में रहते हैं। जब नर बाफोमेट पतंगे मादा की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो वे "कोरमाटा" नामक विशाल, अंगों को तंबु की तरह फुलाते हैं, जो मादा को रिझाने के लिए एक अनूठा रासायनिक गुलदस्ता बनाते हैं। कैटरपिलर के रूप में, नर बैफोमेट पतंगे अपनी मादा-आकर्षित करने वाली सुगंध बनाने के लिए पौधों की पत्तियों को खाते हैं जिनमें पाइरोलिज़िडिन एल्कलॉइड नामक रसायन होते हैं। पौधे इन अल्कलॉइड का उत्पादन पौधों को कुतरने वाले जानवरों को रोकने के लिए करते हैं, लेकिन बैफोमेट पतंगों ने इन रसायनों को अपनी आकर्षक सुगंध में बदलने का एक तरीका विकसित किया है।ब्लैक सोल्जर फ्लाई मैगॉट्स (हर्मेटिया इल्यूसेंस)कीड़ों का यह विशाल समुदाय भले ही प्रकृति के चमत्कारों में से एक न लगता हो, लेकिन ब्लैक सोल्डर फ्लाई के लार्वा ऐसे सुपरहीरो को पुनर्चक्रित कर रहे हैं जो एक दिन मानवता को भोजन की बर्बादी में कटौती करने में मदद कर सकते हैं। सोल्जर फ्लाई कीड़े एक अनोखी प्रक्रिया के माध्यम से भोजन को तेजी से खाते हैं जिसे भौतिकविदों ने "मैगॉट फाउंटेन" का नाम दिया है। जिस अविश्वसनीय गति से मैगॉट्स भोजन की बर्बादी को रोकते हैं, उसने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है, जो जानवरों के मल और खाद्य अपशिष्ट जैसे अपशिष्ट उत्पादों को मैगॉट-आधारित प्रोटीन में परिवर्तित करने के लिए सोल्जर फ्लाई मैगॉट्स का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं, जिन्हें पशुओं या मनुष्यों को खिलाया जा सकता है।यम! टेललेस व्हिप बिच्छू (एंबलीपिगी)इनके नाम पर मत जाइए, टेललेस व्हिप बिच्छू दरअसल बिच्छू नहीं हैं, बल्कि एंब्लीपिगी नामक कीड़े के एक असामान्य समूह से संबंधित हैं। उनकी डरावनी उपस्थिति के बावजूद, एंब्लीपीगिड में जहर की कमी होती है और ये डरपोक जानवर होते हैं जो शायद ही कभी काटते हैं जब तक कि उन्हें खतरा न हो। ये शर्मीले जानवर नम आवासों जैसे पत्तियों के कूड़े में, गुफाओं के अंदर या छाल के नीचे छिपे रहना पसंद करते हैं। एंब्लीपिगी के सामने के पैर लंबे होते हैं जो फीलर्स के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें अपने शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं। एक बार शिकार का पता लगने के बाद, एंब्लीपीगिड अपने शिकार को कुचलने के लिए अपने तेज पेडिपल का उपयोग करते हैं। इनमें कुछ प्रजातियां जटिल सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, जिसमें माताएँ एक वर्ष तक अपने बच्चों के पास रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। विशालकाय हाथी मच्छर (टोक्सोरहिन्चाइट्स स्पेशियोसस)जीवन में कुछ चीजें उतनी ही भयावह होती हैं जितनी कि अंधेरे में मच्छर की तेज आवाज। अब कल्पना कीजिए कि एक विशाल मच्छर आपके औसत मच्छर की सोच से पांच गुना बड़ा है। आश्चर्यजनक रूप से 8 मिमी लंबाई वाला, ऑस्ट्रेलियाई हाथी मच्छर दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर प्रजाति है। लेकिन डरिए मत, यह विशाल मच्छर शाकाहारी होते हैं। हां अधिकांश मादा मच्छरों को अपने बढ़ते अंडों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए रक्त के भोजन की आवश्यकता होती है। मादा हाथी मच्छर अन्य जलीय कीड़ों को खाकर आवश्यक पोषक तत्व एकत्र करती हैं। और यह इसलिए बेहतर है, क्योंकि हाथी मच्छरों का पसंदीदा भोजन है ... अन्य मच्छरों के लार्वा!सामान्य बिच्छू मक्खी (पैनोरपा)बिच्छू मक्खी और बिच्छू के बीच एक अजीबोगरीब समानता है। ताजा मानव लाशों को खाने की एक भयानक आदत के साथ उनकी शक्लो सूरत इतनी डरावनी होती है कि आपको किसी डरावनी फिल्म की याद दिला सकती है। सौभाग्य से, बिच्छू, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, उड़ने वाले बिच्छू नहीं हैं, न ही वे किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। वास्तव में, बिच्छू के "डंक" बढ़े हुए पर जननांग होते हैं! प्रेमालाप के दौरान, नर बिच्छू मादाओं को या तो एक मृत कीट या लार की एक बूँद भेंट करके उन्हें लुभाने का प्रयास करते हैं। बिच्छू मक्खियाँ ज्यादातर मैला ढोने वाली होती हैं और अक्सर मकड़ी के जाले से शिकार चुराते हुए देखी जाती हैं।








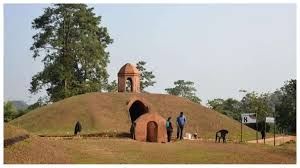
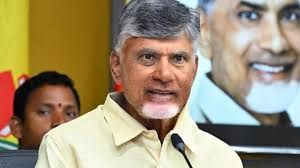
.jpeg)



.jpg)



.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)



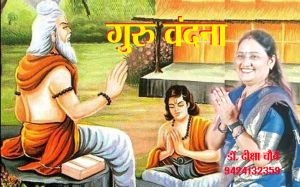
.jpg)

.jpeg)


.jpg)
.jpg)



.jpg)


.jpg)


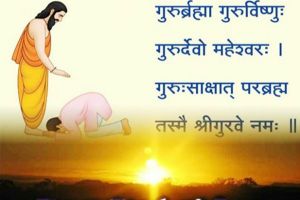










.jpg)


.jpeg)











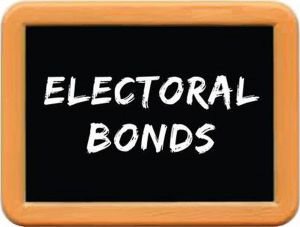


.jpg)

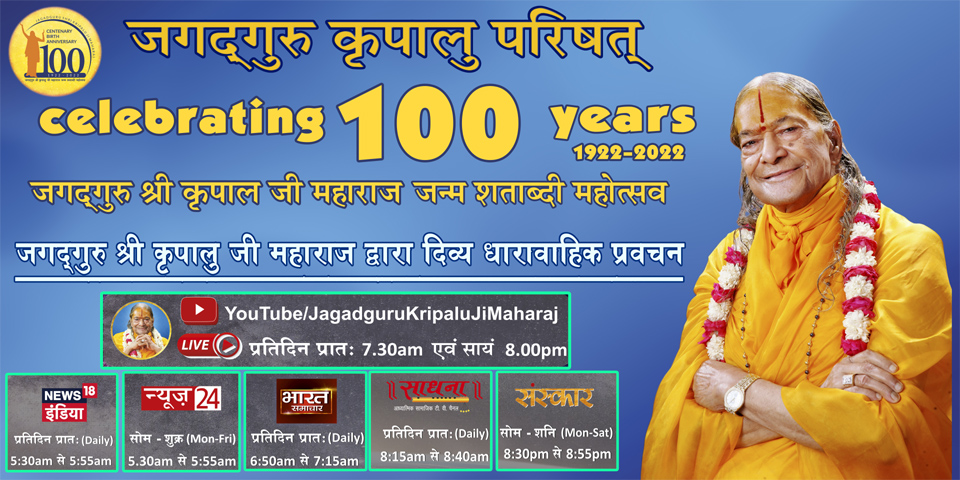

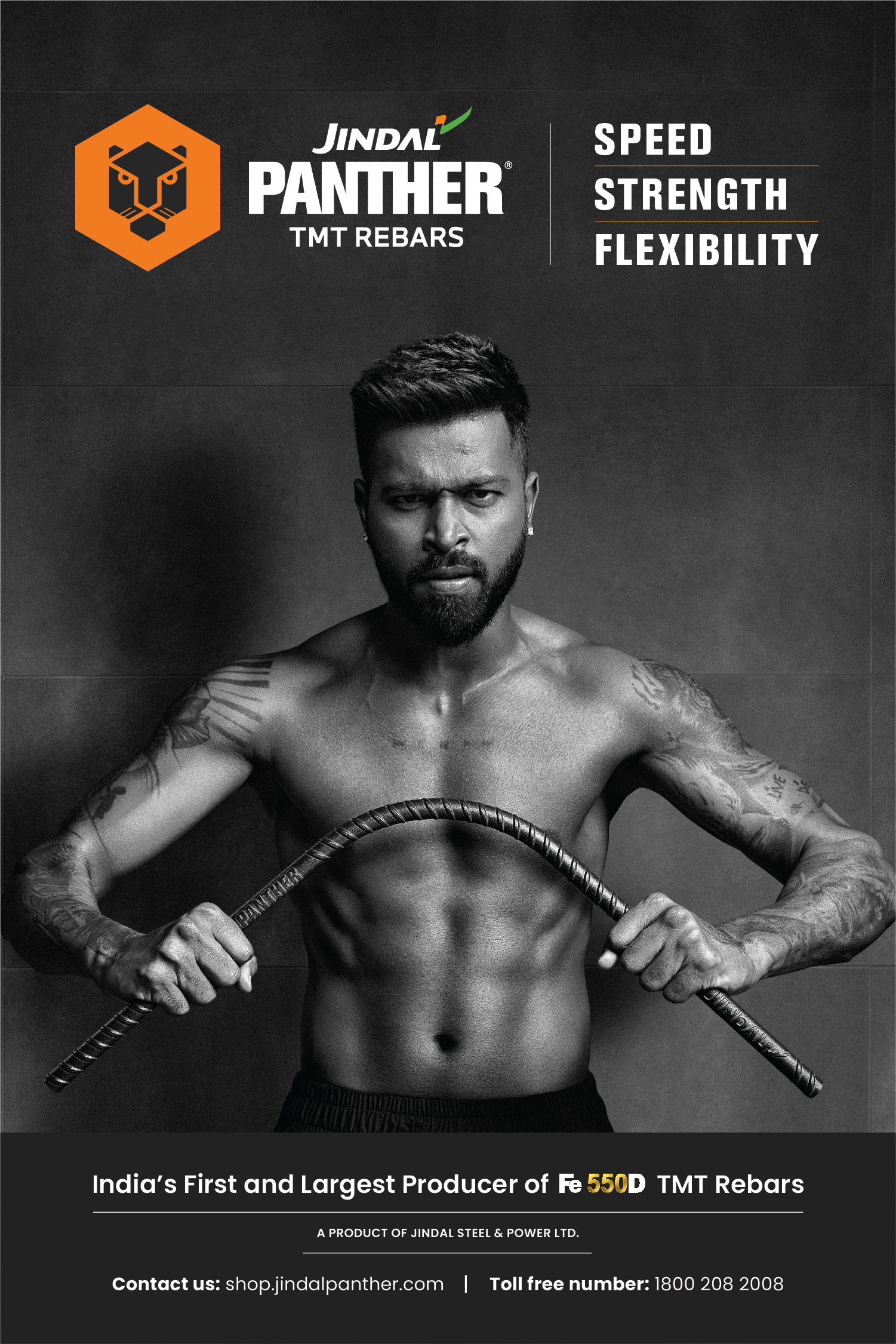
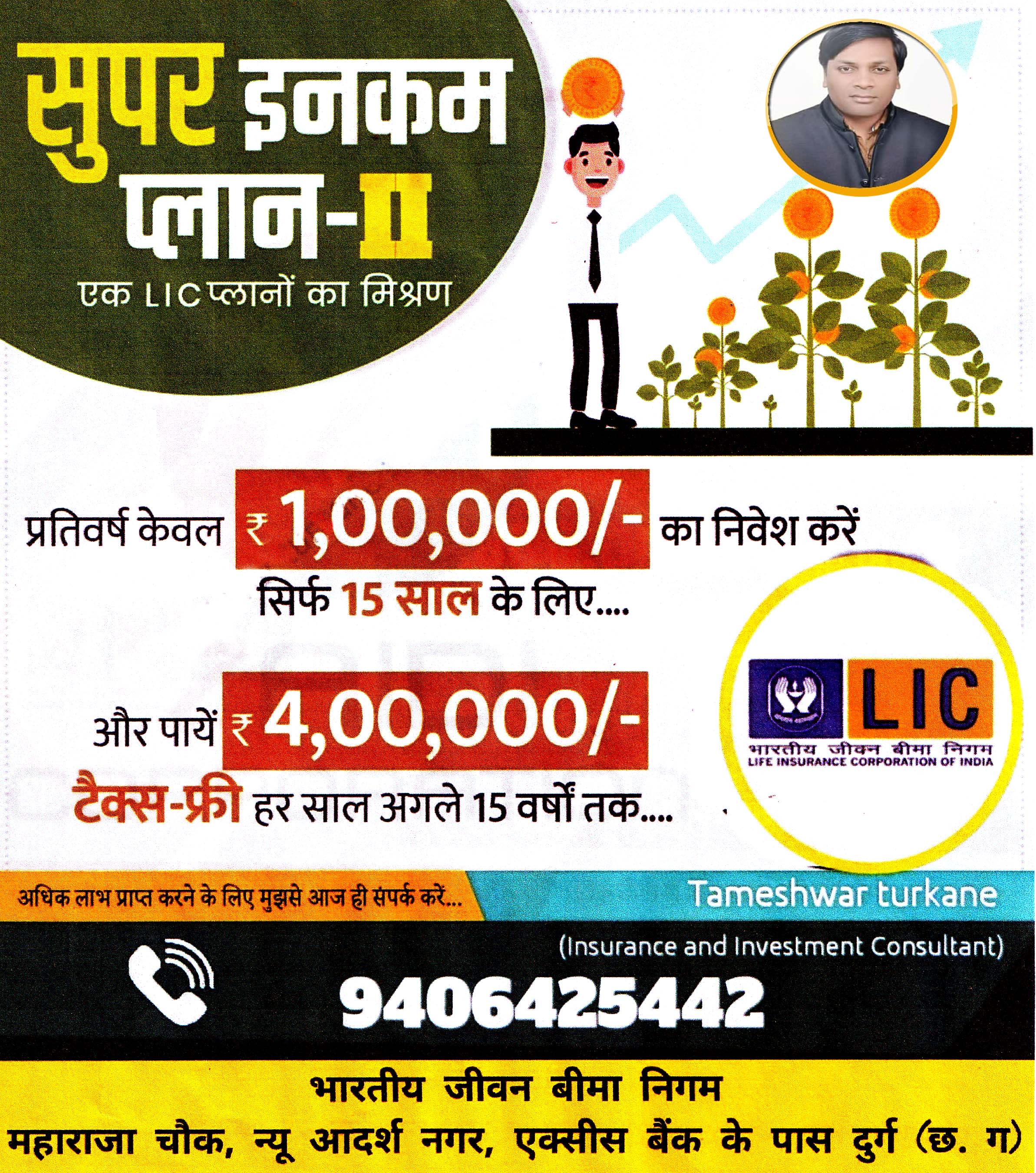
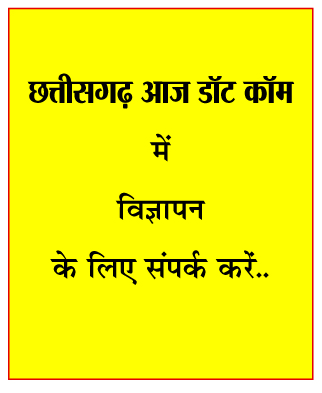
.jpg)