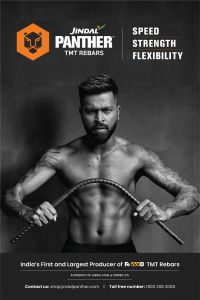- Home
- ज्ञान विज्ञान
- भारत कई रहस्यमयी मंदिरों का घर है। रहस्य भी ऐसे जो सदियों से अनसुलझे हैं। इसके अलावा कई मंदिर अपने साथ जुड़ी अजीब मान्यताओं, भौगोलिक स्थितियों आदि के कारण भी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक है बिहार के दरभंगा में चिता पर बना मां काली का मंदिर। श्यामा माई के नाम से मशहूर यह काली मंदिर श्मशान घाट में है। इतना ही नहीं यह मंदिर चिता के ऊपर बना है। मान्यता है कि इस मंदिर में मां श्यामा काली के दर्शन मात्र से सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं।किसकी है चिता?श्यामा माई का यह मंदिर महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता पर बनाया गया है। यह बेहद ही अजीब बात है कि किसी मंदिर का निर्माण किसी व्यक्ति की चिता पर किया गया हो। हालांकि इसके पीछे की एक खास वजह है। महाराजा रामेश्वर सिंह दरभंगा राज परिवार के साधक राजाओं में से एक थे। देवी के प्रति उनकी साधना मशहूर है। यहां तक कि अब इस मंदिर को रामेश्वरी श्यामा माई के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1933 में महाराजा रामेश्वर सिंह के वंशज दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने की थी।आरती में शामिल होने भक्त करते हैं घंटों इंतजारइस मंदिर में मां काली के गले में मुंडों की माला है और इसमें मुंड की संख्या हिंदी के वर्णमाला के अक्षरों जितनी यानी कि 52 है। मान्यता है कि हिंदी वर्णमाला सृष्टि की प्रतीक है। इस मंदिर की एक और खास बात यहां कि आरती है। इस मंदिर की आरती इतनी मशहूर है कि इसमें शामिल होने के लिए भक्त घंटों तक इंतजार करते हैं। खासतौर पर नवरात्रि में तो यहां भारी भीड़ होती है।तंत्र-मंत्र दोनों से होती है पूजाइस मंदिर में मां काली की पूजा वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से की जाती है। वैसे हिंदू धर्म में शादी के एक साल बाद तक दूल्हा-दुल्हन को श्मशान घाट में नहीं जाने के लिए कहा गया है, लेकिन इस मंदिर में दर्शन करने के लिए नवविवाहित दूर-दूर से आते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनका दांपत्य जीवन सुखी रहता है।
- भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। इस साल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 24 जनवरी के बजाए 23 जनवरी से मनाने का फैसला लिया है। अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व का आगाज होगा। भारत सरकार का यह निर्णय नेताजी के सम्मान और देश की स्वतंत्रता में उनके संघर्षों को याद रखने के लिए लिया गया है। इस साल भारत सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती मना रहा है।सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज के गठन से लेकर हर भारतीय को आजादी का महत्व समझाने तक हर काम को किया। वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर के लिए प्रेरणा हैं। 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' ये वह नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गरम कर दिया। अंग्रेजों से लडऩे के लिए एक ऐसी ताकत दी, जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। लेकिन भारत के इस महान नेता के बारे में आप कितना जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई ऐसी बातें हैं, जिसे जानकर आप हर भारतीय गर्व करेगा। चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनसे जुड़ी रोचक बातें।सुभाष चंद्र बोस का बचपन और शिक्षासुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा राज्य के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपने माता-पिता के 14 बच्चों में वह 9 वीं संतान थे। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेंशॉव कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए 1913 में कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से साल 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उनके माता-पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैंब्रिज विश्वविद्यालय भेजा गया था।प्रशासनिक सेवा में नेताजी का चौथा स्थानये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था कि अंग्रेजों के शासन में जब भारतीयों के लिए किसी परीक्षा में पास होना तक मुश्किल होता था, तब नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने पद संभाला, लेकिन भारत की स्थिति और आजादी के लिए सब छोड़कर स्वदेश वापसी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे।सुभाष चंद्र बोस का परिवार और बच्चेनेताजी ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से शादी की थी जो कि ऑस्ट्रियन मूल की थीं। उनकी अनीता नाम की एक बेटी भी हैं, जो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती हैं।नेताजी और द्वितीय विश्व युद्धसाल 1938 में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। एक साल बाद 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में पट्टाभि सीतारमैया को नेताजी ने हरा दिया। इसके बाद नेताजी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी। जिसके कारण उन्हे घर पर ही नजरबंद कर दिया गया, लेकिन नेताजी किसी तरह जर्मनी चले गए। यहां से उन्होंने विश्व युद्ध को काफी करीब से देखा।आजाद हिंद फौज का गठनदेश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। साथ ही उन्होंने आजाद हिंद बैंक की भी स्थापना की। दुनिया के दस देशों ने उनकी सरकार, फौज और बैंक को अपना समर्थन दिया था। इन दस देशों में बर्मा, क्रोसिया, जर्मनी, नानकिंग (वर्तमान चीन), इटली, थाईलैंड, मंचूको, फिलीपींस और आयरलैंड का नाम शामिल हैं। इन देशों ने आजाद हिंद बैंक की करेंसी को भी मान्यता दी थी। फौज के गठन के बाद नेताजी सबसे पहले बर्मा पहुंचे, जो अब म्यांमार हो चुका है। यहां पर उन्होंने नारा दिया था, 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'। यह वह दौर था जब भारत देश आजादी की ओर अग्रसर था।सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्यनेताजी की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन अचानक 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज मंचुरिया जा रहा था, जो रास्ते में लापता हो गया। आज तक ये नहीं पता चल सका कि सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज का क्या हुआ, वह कहां गया?
- वैज्ञानिकों को अमेरिका के ऊटा में तंबाकू के इस्तेमाल के 12 हजार 300 साल पुराने सबूत मिले हैं। इससे पहले मिले तंबाकू के सबसे पुराने अवशेष बस 3 हजार 300 साल पुराने थे।इस खोज को मानव संस्कृति के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। तंबाकू के ये पुराने अवशेष ऊटा के ग्रेट सॉल्ट लेक रेगिस्तान में एक सिगड़ी के अवशेषों में मिले हैं। शोधकर्ताओं को सिगड़ी के अंदर मौजूद चीजों में तंबाकू के एक जंगली पौधे के चार जले हुए बीज मिले। इनके साथ साथ पत्थर के कुछ औजार और खाने में से बची हुई बत्तख की हड्डियां मिलीं। अभी तक तंबाकू के इस्तेमाल के जो सबसे पुराने सबूत मिले थे वो अल्बामा में मिले 3 हजार 300 साल पुराने धूम्रपान के एक पाइप के अंदर निकोटीन के अवशेष थे।शोधकर्ताओं का मानना है कि ऊटा वाली जगह पर खानाबदोश लोगों ने इस तंबाकू से धूम्रपान किया होगा या तंबाकू के पौधे के रेशों के गुच्छों को चूसा होगा। संभव है उन्होंने उसका सेवन उसमें मौजूद उत्तेजित करने वाले गुणों के लिए किया हो। तंबाकू के इस्तेमाल की शुरुआत "नई दुनिया" के नाम से जाने जाने वाले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के इलाकों में ही हुई। सबसे पहले वहां के मूल निवासियों ने इसका सेवन किया और फिर करीब 500 साल पहले यूरोपीय लोगों के वहां पहुंचने के बाद तंबाकू दुनिया भर में फैल गई। आज इसे एक वैश्विक संकट के रूप में देखा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आज पूरी दुनिया में 1.3 अरब लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और हर साल इसकी वजह से 80 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है।इस नई खोज के बारे में 'नेचर ह्यूमन बिहेवियर' पत्रिका में छपे लेख के मुख्य लेखक पुरातत्वविद डैरन ड्यूक कहते हैं, "वैश्विक स्तर पर तंबाकू मादक पौधों का राजा है और अब हम इसकी सांस्कृतिक जड़ों की पहुंच सीधे शीत युग तक पा सकते हैं।"ड्यूक नेवाडा के फार वेस्टर्न ऐंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च ग्रुप के सदस्य हैं. उन्होंने इन बीजों के बारे में बताया, "इस नस्ल के पौधे हमेशा से जंगली रहे लेकिन इस प्रांत के मूल निवासी आज भी इसका सेवन करते हैं।" यह बीज निकोटियाना आतेनुआता नाम के रेगिस्तानी तंबाकू की एक जंगली किस्म के पौधे के हैं। यह पौधा यहां आज भी पाया जाता है। ग्रेट सॉल्ट लेक रेगिस्तान उत्तरी ऊटा में स्थित एक विशाल सूखी हुई झील का इलाका है.। सिगड़ी के ये अवशेष जिस समय के हैं उस समय यह इलाका एक विशाल दलदली भूमि का हिस्सा था। शीत युग का अंत नजदीक था लेकिन तब भी यहां का मौसम ठंडा था। सिगड़ी में मिली हड्डियों के नाम पर इस जगह को विशबोन स्थल कहा जाता है। सिगड़ी के अवशेष वहां मौजूद मिट्टी के घरों से उड़ती धूल के नीचे मिले थे। यहां मौजूद दलदली भूमि करीब 9 हजार 500 साल पहले सूख गई थी और तब से हवा वहां की तलछट को परत दर परत हटा रही है।उन खानाबदोशों के बारे में बताते हुए ड्यूक कहते हैं, "हम उनकी संस्कृति के बारे में बहुत कम जानते हैं। मुझे इस खोज के बारे में सबसे दिलचस्प बात यही लगती है कि इसने इस सरल सी गतिविधि की सामाजिक अवधि को बढ़ा दिया है। मेरी कल्पना के घोड़ों ने दौडऩा शुरू कर दिया है। " ड्यूक आगे बताते हैं कि इस खोज के हजारों साल बाद इसी महाद्वीप पर दक्षिणपश्चिमी और दक्षिणपूर्वी अमेरिका और मेक्सिको में तंबाकू को उगाना शुरू किया गया। उन्होंने कहा, "हमें यह नहीं मालूम कि तंबाकू को उगाना ठीक ठीक कब शुरू किया गया, लेकिन पिछले 5 हजार सालों में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में कृषि काफी फला-फूला था। तंबाकू के इस्तेमाल के सबूत इस समय में खाद्य फसलों की खेती के साथ बढ़ते जाते हैं।" कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहां तक दावा किया है कि तंबाकू उत्तरी अमेरिका में उगाया जाने वाला पहला पौधा भी हो सकता है और ऐसा खाने की जगह सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों की वजह से किया गया होगा।
- लंबे समय से एस्टेरॉयड को धरती के लिए खतरा बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर एस्टेरॉयड धरती से टकराता है, तो बड़ी तबाही मच सकती है। आज यानी 18 जनवरी को विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। बताया जा रहा है यह अभी तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है जिसका नाम 7482 है। इस एस्टेरॉयड की लंबाई करीब 1 किलोमीटर यानी 3280 फीट है। यह धरती से 19.3 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। इसलिए इससे धरती को कम खतरा है। अगर इसके रास्ते में थोड़ा भी बदलाव होता है, तो धरती के लिए खतरनाक हो सकता है और तबाही मच सकती है।अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इसको खतरनाक घोषित किया हुआ है।नासा का कहना है कि अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता, तो है बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। इसलिए ऐसे एस्टेरॉयड को नासा ने संभावित खतरों की सूची में रखा हुआ है। हालांकि नासा ने बताया है कि यह सुरक्षित तरीके से धरती से 19.3 लाख किमी की दूरी से गुजरेगा। पहली बार साल 1994 में इसकी खोज की गई थी।89 साल पहले 17 जनवरी 1933 को एस्टेरॉयड 7482 धरती के सबसे पास से गुजरा था। उस समय यह 11 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। अब यह 18 जनवरी 2105 को इतने ही करीब से धरती के पास से गुजरेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी धरती से एस्टेरॉयड को टकराने से रोकने के लिए तकनीक खोजने में लगी हुई है। इसके लिए अमेरिकी अतंरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन को लांच किया है।
- दही जमाने के लिए जामन यानी दही की कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। क्या कभी आपने कल्पना की है कि किसी पत्थर के संपर्क में आते ही दूध दही में बदल सकता है? ऐसा सच में है। ये पत्थर मिलती है राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक गांव में। आइए जानते हैं उस गांव के पास विशेष पत्थर के साथ दही बनाने की अनूठी विधि कौन सी है ? और उस पत्थर का रहस्य क्या है? ॉये है हाबूर गांव , जो जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। हाबूर गांव का वर्तमान नाम पूनमनगर है। हाबूर पत्थर को लोकल भाषा में हाबूरिया भाटा कहा जाता है। ये गांव देश-विदेश में अनोखे पत्थर की वजह से प्रसिद्ध है। यहां के पीले पत्थर दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन हाबूर गांव का जादुई पत्थर अपने आप में विशिष्ट खूबियां समेटे हुए हंै। हाबूर पत्थर दिखने में बहुत सुन्दर होता है। ये हल्का सुनहरा और चमकीला होता है। हाबूर पत्थर का चमत्कार ऐसा है कि इस पत्थर में दूध को दही बनाने की कला है। हाबूर पत्थर के संपर्क में आते ही दूध एक रात में दही बन जाता है। जो स्वाद में मीठा और सौंधी खुशबू वाला होता है। इस पत्थर का उपयोग आज भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दूध को जमाने के लिए किया जाता है। इस गांव में मिलने वाले स्टोन से यहां के लोग बर्तन, मूर्ति और खिलौने बनाते हैं जो अपनी विशेष खूबी के चलते देश-विदेश में काफी लोकप्रिय है। इस पत्थर से गिलास, प्लेट, कटोरी, प्याले, ट्रे, मालाएं,फूलदान, कप, थाली और मूर्तियां निर्मित किये जाते हैं।अब सवाल उठता है कि एक पत्थर से कैसे दही जमाया जा सकता है। वो भी रात को दूध उस पत्थर से बने बर्तन में डाला और सुबह उठकर दही खा लो। जब ऐसा होने लगा तो रिसर्च भी होने लगी, जिसमें ये सामने आया है कि हाबूर पत्थर में दही जमाने वाले सारे केमिकल्स मौजूद है। इस पत्थर में एमिनो एसिड, फिनायल एलिनिया, रिफ्टाफेन टायरोसिन हैं। ये केमिकल दूध से दही जमाने में सहायक होते हैं। हाबूर गांव के भूगर्भ से निकलने वाले इस पत्थर में कई खनिज और अन्य जीवाश्मों की भरमार है जो इसे चमत्कारी बनाते हैं।कहा जाता है कि जैसलमेर में पहले समुद्र हुआ करता था। जिसका का नाम तेती सागर था। कई समुद्री जीव समुद्र सूखने के बाद यहां जीवाश्म बन गए और पहाड़ों का निर्माण हुआ। हाबूर गांव में इन पहाड़ों से निकलने वाले पत्थर में कई खनिज और अन्य जीवाश्मों की भरमार है। जिसकी वजह से इस पत्थर से बनने वाले बर्तनों की भारी मांग है। अगर आपको हाबूर पत्थर से बनी एक प्याली खरीदनी है तो आपको 1500 से 2000 रुपये चुकाने होंगे। वहीं कटोरी की कीमत 2500 के आसपास हो सकती है। वहीं एक गिलास की कीमत 650 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होती है।ऐसा कहा जाता है कि इस पत्थर से बने गिलास में रात को सोते समय पानी भरकर रख दो और सुबह खाली पेट पी लो। अगर आप एक से डेढ़ महीने तक लगातार इसका पानी पीते है, तो आपके शरीर में एक परिवर्तन नजर आएगा। आपके शरीर में होने वाला जोड़ों का दर्द कम होगा साथ ही पाइल्स की बीमारी कंट्रोल होगी।
- एक शौकिया वैज्ञानिक ने बृहस्पति जैसे ग्रह की खोज की। इस एक्सोप्लैनेट का वजन यानी द्रव्यमान सूर्य के बराबर है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि इसका नाम TOI-2180 b है जो धरती से करीब 379 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह का तापमान करीब 170 डिग्री फ़ारेनहाइट (76 डिग्री सेल्सियस) है। इसका तापमान धरती और सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तुलना में ज्यादा है।जानिए कौन है ग्रह खोजने वालानासा का कहना है कि टॉम जैकब्स नाम के वैज्ञानिक ने इस ग्रह की खोज की है और ये अमेरिकी नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। नासा की सिटिजन साइंटिस्ट प्रॉजेक्ट से टॉम जैकब्स से जुड़े हुए हैं। एस्ट्रॉनमी और फिजिक्स में जिन लोगों की रुचि होती है उनको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नासा शोधकर्ताओं की मदद के लिए लगाता है। आइए जानते हैं इस एक्सोप्लैनेट के बारे में नासा ने और क्या-क्या जानकारी दी है।नासा की तरफ से बताया गया है कि वैज्ञानिक टॉम जैकब्स ने नई खोज के लिए अलग-अलग दूरबीनों से प्राप्त डेटा को स्कैन किया है। उन्होंने इन डेटा का परीक्षण कंप्यूटर एल्गोरिदम के माध्यम से किया। वैज्ञानिक किसी एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए सितारों की चमक में होने वाले बदलाव के बारे में पता लगाते हैं। इससे यह जानकारी मिलती है कि कोई ग्रह एक निश्चित तारे की परिक्रमा कर रहा है या नहीं। अगर जिस तारे की परिक्रमा कर रहा होता है उसकी चमक कुछ समय के लिए बाधित होती है।जानिए कैसे खोजा गया ग्रहकंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए से इस ग्रह की खोज की गई है, क्योंकि इसका निर्माण अलग-अलग ग्रहों की खोज करने के लिए किया गया है। इस शौकिया वैज्ञानिक ने नए एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। टॉम जैकब्स विजुअल सर्वे समूह नाम की एक टीम में काम करते हैं। यह समूह आंखों से टेलीस्कोप डेटा का निरीक्षण करता है।
- नयी दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी) के अनुसंधानकर्ताओं ने हिमालयी पौधे बुरांश की पत्तियों में 'फाइटोकेमिकल' होने का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए हो सकता है।'फाइटोकेमिकल' या पादप रसायन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद हो सकते हैं। अनुसंधान में पता चला कि हिमालयी क्षेत्र में पाये जाने वाले पौधे बुरांश या 'रोडोडेंड्रॉन अरबोरियम' की पादप रसायन युक्त पत्तियों में विषाणु रोधी या वायरस से लडऩे की क्षमता होती है। अध्ययन के निष्कर्षों को हाल में जर्नल 'बायोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डाइनामिक्स' में प्रकाशित किया गया। अनुसंधान दल के अनुसार कोविड-19 महामारी को शुरू हुए लगभग दो वर्ष हो चुके हैं और अनुसंधानकर्ता इस वायरस की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं तथा संक्रमण की रोकथाम के नये तरीके खोज रहे हैं।आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम कुमार मसकपल्ली ने कहा, ''वायरस के खिलाफ शरीर को लडऩे की क्षमता देने का एक तरीका तो टीकाकरण है, वहीं दुनियाभर में ऐसी गैर-टीका वाली दवाओं की खोज हो रही है जिनसे मानव शरीर पर विषाणुओं के हमले को रोका जा सकता है। इन दवाओं में वो रसायन होते हैं जो या तो हमारी शरीर की कोशिकाओं में रिसेप्टर अथवा ग्राही प्रोटीन को मजबूती प्रदान करते हैं और वायरस को उनमें प्रवेश करने से रोकते हैं या स्वयं वायरस पर हमला कर हमारे शरीर में इसके प्रभाव होने से रोकथाम करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''उपचार के विभिन्न तरीकों का अध्ययन किया जा रहा है, जिनमें पौधों से निकलने वाले रसायन फाइटोकेमिकल को उसकी सहक्रियाशील गतिविधियों के कारण और कम विषैले तत्वों के साथ प्राकृतिक स्रोत के नाते विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।'' हिमालयी पादप बुरांश की पत्तियों का स्थानीय लोग स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए सेवन करते हैं। मसकपल्ली ने कहा, ''टीम ने वैज्ञानिक तरीके से फाइटोकेमिकल वाले अर्क की जांच की और विशेष रूप से उनकी विषाणु रोधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। अनुसंधानकर्ताओं ने बुरांश की पत्तियों से पादप रसायन निकाले और उसकी वायरस रोधी विशेषताओं को समझने के लिए अध्ययन किया।'' आईसीजीईबी से जुड़े रंजन नंदा ने कहा, ''हमने हिमालय से प्राप्त रोडोडेंड्रॉन अरबोरियम की पत्तियों के पादप रसायनों का विश्लेषण किया और उन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर पाया।''
- मिल्टन केनेस (ब्रिटेन)। हम सौर मंडल के बाहर लगभग 5,000 ग्रहों के बारे में जानते हैं। अगर आप कल्पना करते हैं कि दूर की इस दुनिया या एक्सोप्लैनेट (सौर मंडल के बाहर के ग्रह) का वजूद कैसा होगा तो आपके दिमाग में किसी मूल तारे या एक से अधिक तारों की छवि उभरेगी, विशेष रूप से यदि आप 'स्टार वार्स' फिल्मों के प्रशंसक हैं। वैज्ञानिकों ने हाल में पता लगाया है कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक ग्रह अपने आप अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। ये बर्फीले ''फ्री-फ्लोटिंग प्लैनेट'' अथवा एफएफपी हैं। लेकिन वे अपने आप कैसे समाप्त हो जाते हैं और ऐसे ग्रह कैसे बनते हैं? इसके बारे में हमें वे बता सकते हैं। अध्ययन करने के लिए अधिक से अधिक एक्सोप्लैनेट खोजने से जैसा कि हमने उम्मीद की होगी, हमारी समझ को व्यापक किया है कि ग्रह क्या है। विशेष रूप से ग्रहों और ''ब्राउन ड्वाफ्र्स'' के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती गई है।''ब्राउन ड्वाफ्र्स'' ऐसे ठंडे तारे होते हैं जो अन्य तारों की तरह हाइड्रोजन को 'फ्यूज' नहीं कर सकते। क्या तय करता है कि कोई वस्तु एक ग्रह है या ''ब्राउन ड्वाफ्र्स'', यह लंबे समय से बहस का विषय रहा है। क्या यह द्रव्यमान का सवाल है? यदि वे परमाणु संलयन से गुजर रहे हैं तो क्या वस्तुएं ग्रह नहीं रह जाती हैं? अथवा, जिस तरह से वस्तु का गठन हुआ वह सबसे महत्वपूर्ण है? लगभग आधे तारे और ''ब्राउन ड्वाफ्र्स'' अलग-थलग रहते हैं, बाकी कई तारा सौर मंडल में मौजूद हैं। हम आमतौर पर ग्रहों को एक तारे के चारों ओर कक्षा में अधीनस्थ वस्तुओं के रूप में सोचते हैं। दूरबीन तकनीक में सुधार ने हमें अंतरिक्ष में छोटी और अलगाव में रह रही वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाया है, जिसमें एफएफपी भी शामिल है। ये एफएफपी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान या तापमान बहुत कम होता है जिन्हें ''ब्राउन ड्वार्फ'' माना जाता है। हम अभी भी यह नहीं जानते हैं कि वास्तव में ये वस्तुएं कैसे बनीं। तारे और ''ब्राउन ड्वार्फ'' तब बनते हैं जब अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक क्षेत्र अपने आप गिरने लगता है। यह क्षेत्र सघन हो जाता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण की एक प्रक्रिया में अधिक से अधिक सामग्री उस पर गिरती रहती है। आखिर गैस का यह गोला परमाणु संलयन शुरू करने के लिए गर्म होता जाता है। एफएफपी एक ही तरह से बन सकते हैं, लेकिन फ्यूजन शुरू करने जितना आकार बड़ा नहीं होता है। यह भी संभव है कि ऐसा ग्रह किसी तारे के चारों ओर कक्षा में जीवन शुरू कर सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर अंतरताराकीय स्थान से बाहर हो जाता है। तारों के बीच भटकते ग्रह को कैसे पहचानें?इस तरह के ग्रहों का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि वे अपेक्षाकृत छोटे और ठंडे होते हैं। आंतरिक ऊष्मा का उनका एकमात्र स्रोत नष्ट होने की प्रक्रिया से बची शेष ऊर्जा है जिसके परिणामस्वरूप उनका निर्माण हुआ। ग्रह जितना छोटा होगा, उतनी ही तेजी से ऊष्मा विकिरित होगी। अंतरिक्ष में ठंडी वस्तुएं कम प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और वे जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वह लाल रंग का होता है। एफएफपी को सीधे देखने के लिए सबसे अच्छी रणनीति शुरुआती अवस्था में उनका पता लगाना है क्योंकि इस दौरान सबसे ज्यादा चमक रहती है। हाल के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इसी तरीके से भटकने वाले ग्रहों का पता लगाया है। इन भटकते ग्रहों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। दूरबीन की नयी तकनीक उपलब्ध होने के साथ ही ग्रहों को और अधिक विस्तृत जांच के लिए फिर से देखा जा सकता है। इससे ऐसे ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है।-
- स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के क्षेत्र में बड़ी छलांग सामने आई जब एक आर्टिफिशियल किडनी का टेस्ट सफल हुआ। अब किडनी रोगियों को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट लिस्ट से फ्री होने का समय आ गया है। इस मामले में इसे बनाने वाली टीम को 6 लाख 50 हजार डॉलर का प्राइज भी मिला है।'स्कूल ऑफ फॉर्मेसी' की एक स्टडी के अनुसार, इस प्राइज को देने वाली किडनीएक्स की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेस और अमेरिकन सोसायटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के बीच एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये संस्थान किडनी की बीमारियों की रोकथाम, निदान और ट्रीटमेंट में नए एक्सपेरिमेंट में तेजी लाने का काम करता है।आर्टिफिसियल किडनी में दो जरूरी पार्ट होते हैं हीमोफिल्टर और बायोरेक्टर, इन दोनों स्मार्टफोन साइज के डिवाइस को सफलतापूर्वक मरीज में प्रत्यारोपण कर देखा गया। इस काम के लिए टीम को किडनीएक्स के फेज 1 आर्टिफिसियल किडनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।पिछले कुछ वर्षों में इस किडनी प्रोजेक्ट ने हेमोफिल्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और विषाक्त पदार्थों को निकालता है और बायोरिएक्टर जो अन्य गुर्दा कार्य जैसे रक्त में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन करता है।किडनी के सबसे ज्यादा मरीजों को खून लेने के लिए हर हफ्ते कई बार डायलिसिस के क्लीनिक जाना होता है। इसमें उन्हें फि़ल्टर किया गया खून चढाऩा होता है जो एक असुविधाजनक और जोखिम भरा होता है। इसके अलावा इसके स्थाई इलाज के लिए किडनी दान में लेनी होती है जिसकी बहुत ज्यादा मांग होती है। इस वजह से आर्टिफिशियल किडनी की टेस्टिंग बहुत बड़ी खोज है।
- 2021 में इंटरनेट पर हर एक मिनट में क्या क्या हुआ इस पर एक नए शोध के नतीजे आए हैं। आइए देखते हैं इतनी छोटी से अवधि में किस कदर बदल जाती है इंटरनेट की दुनिया।सोशल मीडियावल्र्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2021 में हर एक मिनट में यूट्यूब पर 500 घंटों की सामग्री अपलोड की गई और इंस्टाग्राम पर 6 लाख 95 हजार स्टोरी साझा की गईं।नेटफ्लिक्सक्या आपने 2021 में नेटफ्लिक्स पर खूब वीडियो देखे? इस शोध के मुताबिक तो हर मिनट नेटफ्लिक्स के 28 हजार ग्राहक उसके ऐप पर कुछ न कुछ देख ही रहे थे। फोरम ने यह जानकारी स्टैटिस्टा के साथ मिल कर दी है।टिकटॉकमनोरंजन की दुनिया में टिकटॉक पर भी खूब सामग्री देखी गई। हर मिनट में टिकटॉक पर 5 हजार वीडियो डाउनलोड किए गए।बातचीतइतने ही समय में व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए करीब सात करोड़ मैसेज भेजे गए। इसके अलावा अलग ईमेल सेवाओं के जरिए सिर्फ एक मिनट में 19 करोड़ से भी ज्यादा ईमेल भेजे गए।लिंक्डइनलोगों ने सिर्फ मनोरंजन और सोशल नेटवर्किंग पर ही समय नहीं बिताया बल्कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी की। लिंक्डइन पर हर एक मिनट में 9,132 कनेक्शन बने।खर्चाइंटरनेट पर कितनी शॉपिंग होती है और कितनी चीजों का भुगतान होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 में हर एक मिनट में इंटरनेट पर 16 लाख डॉलर खर्च किए गए।----
- -स्टुअर्ट मार्शल और डेविड ए.स्टोरी, मेलबर्न विश्वविद्यालयमेलबन। रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर होना कोविड के बिगडऩे का एक प्रारंभिक संकेत है। लेकिन सभी में बीमारी के स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ या अन्यथा अस्वस्थ महसूस किए बिना भी ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। इसलिए कुछ लोग घर पर अपने ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं। अन्य लोगों को उनके कोविड होम-केयर पैकेज के हिस्से के रूप में नियमित रूप से पल्स ऑक्सीमीटर की आपूर्ति की जाती है। विचार यह है कि घर पर आप स्वयं अपने ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करके, आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके फेफड़े आपके रक्त को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन दे रहे हैं। वैकल्पिक रूप से, ऑक्सीजन के निम्न स्तर का पता लगाना यह संकेत दे सकता है कि आपको तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? और यदि यह आपके पास है तो आप वास्तव में घर पर कोविड की निगरानी के लिए इसका उपयोग कैसे करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? यह कैसे काम करता है?एक पल्स ऑक्सीमीटर एक नियमित नैदानिक मॉनिटर है जो वर्षों से अस्पताल में और बाहर उपयोग में है। अधिकांश प्रकार जिन्हें आप घर पर उपयोग के लिए खरीद सकते हैं, उन्हें एक चिमटी की तरह डिज़ाइन किया गया है जिसे आप अपनी उंगलियों पर क्लिप करते हैं। क्लिप का एक पक्ष आपकी अंगुली से क्लिप के दूसरी ओर सेंसर तक प्रकाश डालता है। यह आपके खून के रंग का माप देता है। अधिक ऑक्सीजन ले जाने वाला रक्त (ऑक्सीजन युक्त रक्त) नीले रंग के डी-ऑक्सीजनेटेड रक्त की तुलना में अधिक चमकदार लाल होता है। ऑक्सीमीटर रक्त के रंग की व्याख्या करता है (अवशोषित प्रकाश की मात्रा के माध्यम से) एक संख्या प्रदान करने के लिए - रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो अधिकतम मात्रा में ले जाया जा सकता है। यह प्रतिशत ''ऑक्सीजन संतृप्ति'' स्तर है। स्वस्थ लोगों के लिए यह 95 प्रतिशत से 100 प्रतिशत होता है। चूंकि ऑक्सीमीटर आपकी उंगली में नाड़ी से रक्त को मापता है, यह आपकी हृदय गति (दिल की धड़कन प्रति मिनट) को भी प्रदर्शित करेगा। लोग अब उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं?कोविड वाले अधिकांश लोगों को अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कुछ के लिए घर पर स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा निगरानी रखने के लिए सेवाओं की स्थापना की गई है और केवल तभी अस्पताल आते हैं जब वे बहुत अस्वस्थ होने लगते हैं। जिन लोगों को इस प्रकार के घर-में-अस्पताल जैसी निगरानी की जरूरत नहीं हैं, उन्हें घर में रहते अपने लक्षणों की निगरानी करने और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा देखभाल लेने की आवश्यकता होगी। कोविड के बिगडऩे के सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती लक्षणों में से एक रक्त में ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट है। ऐसा तब होता है जब फेफड़े फूल जाते हैं और ऑक्सीजन को अवशोषित करने में कम सक्षम होते हैं। यह व्यक्ति के बीमार महसूस करने से पहले भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई दिशानिर्देश बताते हैं कि जब आराम की अवस्था में ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर 92 प्रतिशत -94प्रतिशत तक गिर जाता है, तो अस्पताल में भर्ती होने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। किसी को अस्पताल जाने की कब आवश्यकता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या अन्य चेतावनी संकेत हैं जैसे कि तेजी से सांस लेना, वृद्धावस्था, पूरी तरह से टीकाकरण नहीं होना, यदि अन्य चिकित्सा समस्याएं हैं, और यदि किसी के पास सीमित सामाजिक सहयोग है। बच्चों के लिए, यह संख्या 95 प्रतिशत या उससे कम है।यदि संभव हो तो आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए जो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर सलाह देगा। क्या रीडिंग सटीक हैं?ऑक्सीजन संतृप्ति रीडिंग आमतौर पर बहुत सटीक होती है। हालांकि, खराब परिसंचरण, या ठंडी या हिलती उंगलियां डिवाइस के लिए नाड़ी को ढूंढना मुश्किल बना सकती हैं या नाड़ी की जगह डिवाइस गति नापने लगता है। यदि आपकी उंगलियां ठंडी हैं या खराब परिसंचरण है, तो आपको दूसरी उंगली से कोशिश करनी पड़ सकती है, या रीडिंग लेने से पहले अपने हाथों को एक साथ रगड़ कर गर्म कर सकते हैं। माप लेते समय आपको स्थिर रहने और अपने हाथ को स्थिर रखने की भी आवश्यकता होगी। छोटे बच्चों पर रीडिंग लेने के लिए यह एक चुनौती हो सकती है! नेल पॉलिश, विशेष रूप से गहरे रंग, भ्रामक ऑक्सीमीटर रीडिंग का कारण बन सकते हैं और इसलिए हम लोगों से अस्पताल में रीडिंग लेने से पहले इसे हटाने के लिए कहते हैं। हालांकि, ऐक्रेलिक नाखूनों की तुलना में नेल पॉलिश का प्रभाव कम होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप परीक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उंगलियों पर लगे नेल पॉलिश या एक्रेलिक नाखून को हटा दें। अगर मेरी त्वचा का रंग गहरा है तो क्या होगा?जिस तरह अधिकांश घरों में थर्मामीटर होता है, उसी तरह एक साधारण कम लागत वाला ऑक्सीमीटर हम सभी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति पर निगरानी रखने और यदि हालात बिगड़ते हैं तो तत्काल जरूरी कदम उठाने में मदद कर सकता है।-
- दुनिया के बड़े-बड़े देशों ने चंद्रमा पर अपने सैटेलाइट भेज रखे हैं जो समय-समय पर चंद्रमा पर हो रही छोटी बड़ी घटना के बारे में सूचना देते हैं। इसी कड़ी में चीन ने भी चंद्रमा पर यूतु-2 रोवर को भेजा हुआ है। अब इस रोवर ने चंद्रमा पर एक 'रहस्यमयी झोपड़ी' को खोज लिया है। जैसे ही वैज्ञानिकों को इस खोज के बारे में पता चला उन्होंने इसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, रोवर ने जो जानकारी भेजी थी, जब इसकी करीब से जांच की गई तो पता चला कि वो वास्तव में एक प्रकार की चट्टान है जो खरगोश के आकार की दिखाई देती है। यूतु-2 की टीम ने इस चट्टान को 'जेड रैबिट' नाम दिया है। इस चट्टान को दिसंबर में रोवर ने देखा था। जब चंद्रमा के क्षितिज पर एक चौकोर आकृति नजर आई थी।आइए जानते हैं कि इस 'रहस्यमयी झोपड़ी' का क्या है राज-जानकारों ने ये दावा किया है कि ये किसी बड़े पत्थर का टुकड़ा हो सकता है। यूतु चंद्रमा पर 186 किलोमीटर में फैले वॉन कार्मन क्रेटर में खोज कर रहा है। इस रोवर ने 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। ये रोवर सौर ऊर्जा से चलता है। रोवर ने एक महीने की लंबी यात्रा करने के बाद 'मून हट' की ये तस्वीर इतने करीब से खींच कर पृथ्वी पर भेजी है।खरगोश की तरह दिखा ये चट्टानजब इस चट्टान को पास से देखा गया तो आकार में छोटा और गोल दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई खरगोश है इसीलिए इस चट्टान को 'जेड रैबिट' नाम दिया गया। अंतरिक्ष पत्रकार एंड्रयू जोंस ने अपने ट्विटर पर लिखा ,' चंद्रमा की सतह पर 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक चट्टानों का विस्तार है। ऐसे में ये संभव है कि ये एक बड़े चट्टान का टुकड़ा हो।चंद्रमा की सतह पर चीनी मिशनजोंस ने बताया कि कई लोगों को ये उम्मीद थी कि ये कोई बड़ा सा ढांचा होगा, जिससे काफी कुछ रहस्यमयी चीजें निकल कर सामने आएंगी। चांद की सतह पर चीन के दो यान पहले से ही मौजूद हैं। साल 2013 में चांद की सतह पर पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था जिसका नाम चेंग-ई-3 था। दूसरा जनवरी 2019 में भेजा गया था जिसका नाम चेंग-ई-4 है जिसने यूतु-2 के साथ लैंड किया था। जानकार बताते हैं कि अभी ये दोनों एक्टिव मोड में हैं।
- हम सभी ने कभी ना कभी ट्रेन में सफर तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाली लोहे की पटरियों पर कभी जंग क्यों नहीं लगती और इसके पीछे वजह क्या है? वैसे तो हमारे घर में भी कई चीजें लोहे की होती हैं और रेल की पटरी भी लोहे की होती है, लेकिन इन दोनों में ऐसा क्या फर्क है कि घर के लोहे में जंग लग जाती है और रेल की पटरी पर कभी जंग नहीं लगती। आइए जानते हैं इसका कारण....लोहे पर जंग लगती ही क्यों है?रेल की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगती, ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोहे पर जंग क्यों और कैसे लगती है। लोहा एक मजबूत धातु होता है, लेकिन जब उस पर जंग लगती है तो वह किसी काम का नहीं होता। लोहा या लोहे से बना सामान ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड जम जाती है और फिर धीरे-धीरे लोहा खराब होने लगता है। साथ ही इसका रंग भी बदल जाता है। इसी को लोहे पर जंग लगना कहते हैं।रेल की पटरी में जंग इसलिए नहीं लगती क्योंकि रेल की पटरी बनाने के लिए एक खास किस्म की स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टील और मेंगलॉय को मिला कर ट्रेन की पटरियों को तैयार किया जाता है। स्टील और मेंगलॉय के इस मिश्रण को मैंगनीज स्टील कहा जाता है। इस वजह से ऑक्सीकरण नहीं होता है और कई सालों तक इसमें जंग नहीं लगती है।रेल की पटरियों को अगर आम लोहे से बनाया जाएगा तो हवा की नमी के कारण उसमें जंग लग सकती है और ट्रैक कमजोर हो सकता है। इसकी वजह से पटरियों को जल्दी-जल्दी बदलना पड़ेगा और साथ ही इससे रेल दुर्घटनाएं होने का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए रेलवे इन पटरियों के निर्माण में खास तरह के मैटेरियल का इस्तेमाल करता है।
-
दुनिया के इतिहास में कई युद्ध और लड़ाईयों के बारे आपने पढ़ा और सुना होगा। भारतीय इतिहास में भी कई युद्ध लड़े गए हैं जिनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें अधिकतर जंग दूसरे राज्यों पर कब्जे को लेकर हुई हैं। लेकिन 1644 ईस्वी में एक युद्ध सिर्फ एक तरबूज के लिए लड़ा गया था। आज से करीब 376 साल पहले हुई इस जंग में हजारों सैनिकों की मौत हुई थी। आईए जानते हैं इस युद्ध के बारे में...
दुनिया की यह पहली जंग हैं जो सिर्फ एक फल के लिए लड़ी गई थी। इतिहास में यह युद्ध 'मतीरे की राड़' के नाम से दर्ज है। राजस्थान के कई इलाकों में तरबूज को मतीरा के नाम से जाना जाता है और राड़ का मतलब लड़ाई होती है। आज से 376 साल पहले 1644 ईस्वी में यह अनोखा युद्ध हुआ था। तरबूजे के लिए लड़ी गई यह लड़ाई दो रियासतों के लोगों के बीच हुई थी।
दरअसल उस दौरान बीकानेर रियासत के सीलवा गांव और नागौर रियासत के जाखणियां गांव की सीमा एक दूसरे सटी हुई थी। ये दोनों गांवइन रियासतों की आखिरी सीमा थे । बीकानेर रियासत की सीमा में एक तरबूज का पेड़ लगा था और नागौर रियासत की सीमा में उसका एक फल लगा था। यही फल युद्ध की वजह बना।
सीलवा गांव के निवासियों का कहना था कि पेड़ उनके यहां लगा है, तो फल पर उनका अधिकार है, तो वहीं नागौर रियासत में लोगों का कहना था कि फल उनकी सीमा में लगा है, तो यह उनका है। इस फल पर अधिकार को लेकर दोनों रियासतों में शुरू हुई और लड़ाई ने एक खूनी जंग का रूप ले लिया।
राजाओं की नहीं थी युद्ध की जानकारी
बताया जाता है कि सिंघवी सुखमल ने नागौर की सेना का नेतृत्व किया, जबकि रामचंद्र मुखिया बीकानेर की सेना का नेतृत्व। सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध के बारे में दोनों रियासतों के राजाओं को जानकारी नहीं थी। जब यह लड़ाई हो रही थी, तो बीकानेर के शासक राजा करणसिंह एक अभियान पर थे, तो वहीं नागौर के शासक राव अमरसिंह मुगल साम्राज्य की सेवा में तैनात थे। मुगल साम्राज्य की अधीनता को इन दोनों राजाओं ने स्वीकार कर लिया था। जब इस लड़ाई के बारे में दोनों राजाओं को जानकारी मिली, तो उन्होंने मुगल राजा से इसमें हस्तक्षेप करने की अपील की। लेकिन जब यह बात मुगल शासकों तक पहुंची तब तक युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में बीकानेर रियासत की जीत हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि दोनों तरफ से हजारों सैनिकों की मौत हुई थी। -
बारिश के दौरान आसमान से बूंदों के साथ कभी-कभी ओले गिरना आम बात है। सिर्फ यही नहीं, बारिश के साथ आसमान से ओले गिरते हुए भी सभी ने देखे होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि आसमान से बारिश के साथ मछलियां भी गिरती हैं, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। हाल ही में अमेरिका के टेक्सास में स्थित एक कस्बे में कुछ ऐसा ही हुआ है। इस कस्बे में हुई बारिश के साथ आसमान से मछलियां भी गिर रही थीं। वहीं आसमान से अचानक मछलियों की बारिश होते देख लोग भी काफी हैरान रह गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी तस्वीरें भी शेयर की हैं। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो मौके का फायदा भी उठाया और मछलियों को इकठ्ठा करके घर भी ले गए।
बारिश के दौरान आसमान से जब मछलियां गिरना शुरु हुई तो लोगों को यही लगा कि ओले गिर रहे हैं। इसलिए लोग घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन जब बारिश थमी, तब लोगों ने देखा कि ये कोई सामान्य बारिश नहीं थी। बल्कि पूरे कस्बे में चारों तरफ मछलियां पड़ी थीं।
इस घटना के बारे में हर कोई अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। लोगों का कहना है कि मछली की बारिश कोई मजाक नहीं है। आम लोग इस घटना को देखकर आश्चर्य में पड़ रहे हैं।
हालांकि विज्ञान के नजरिए से इस तरह की भौगोलिक घटना संभव है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और इसे विज्ञान की भाषा में एनिमल रेन या वॉटर स्प्राउट्स भी कहा जाता है।
जानकारों के मुताबिक ये एक तरह का बवंडर होता है, जो तालाब और झील जैसे पानी के कुछ हिस्से में बनता है। इस बवंडर के दौरान किसी वॉटर सोर्स पर ऐसा चक्रवात बनता है, जो हवा-पानी और पानी के अंदर मौजूद चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। सिर्फ यही नहीं छोटे जीव-जंतुओं को अपनी ओर समेटते हुए ये जमीन की तरफ बढ़ता है। इस दौरान तूफान की रफ्तार जैसे-जैसे कम होती है, इसमें मौजूद जीव-जंतु जमीन पर गिरने लगते हैं। - -टीवी को लिकेबल टीवी कहा जा रहा है, 'टेस्ट-द-टीवी' नाम दिया गया-टीवी के साथ 10 कैनिस्टर फिट किए जिसमें अलग-अलग स्वाद के केमिकल स्टोर किए-इस लिक्विड को चखने पर दर्शक को उसी स्वाद का अनुभव होगा जिसे वह देख रहे हैंटोक्यो। वर्तमान में हम स्मार्ट टेलीविजन का दौर देख रहे हैं लेकिन, कुछ साल पीछे जाएं तो टीवी के हमें कई रूप देखने को मिलेंगे। पहले दुनिया ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का स्वागत किया, उसके बाद कलर, टीएफटी, एलसीडी, एचडी, 4के और अब स्मार्ट टीवी। समय के साथ टीवी में कई बदलाव हुए और आने वाले समय में कई और चेंज देखने को मिलेंगे। अब जल्द ही मार्केट में चाटने या स्वाद चखने वाली टीवी दिखाई दे सकती है। जी हां, एक ऐसी टीवी जिसे आप चाटकर उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्यंजन का स्वाद चख सकते है।दुनिया की पहली लिकेबल टीवीदरअसल जापान के एक प्रोफेसर होमेइ मियाशिता ने एक ऐसा टीवी बनाया है जिसे लिक यानी चाटा जा सकता है। इस टीवी को लिकेबल टीवी कहा जा रहा है, जिसे 'टेस्ट-द-टीवी' नाम दिया गया है। यह दुनिया का पहला ऐसा टीवी है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे व्यंजन का स्वाद अपने दर्शकों को चखा सकता है। लेकिन, टीवी ऐसा कैसे करता है? होमेइ मियाशिता टीवी के साथ 10 कैनिस्टर फिट किए हैं जिसमें अलग-अलग स्वाद के केमिकल स्टोर किए गए हैं।इस तरह काम करती है टीवीजब टीवी पर कोई भोजन या व्यंजन आता है तो कैनिस्टर में लगे स्प्रे से इजेनिक फिल्म पर फ्लेवर यानी स्वाद को मिलाकर छिड़क दिया जाता। इस लिक्विड को चखने पर दर्शक को उसी स्वाद का अनुभव होगा जिसे वह देख रहे हैं। हालांकि इसमें काफी बदलाव होना बाकी है लेकिन, टीवी को लेकर दुनियाभर में चर्चा शुरू हो गई है। प्रोफेसर होमेइ मियाशिता ने बताया कि ऐसी टीवी बनाने का मकसद यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में घर बैठे आप व्यंजन का स्वाद चख सकें।घर बैठे ले सकेंगे स्वादप्रोफेसर मियाशिता ने कहा कि इस टीवी की मदद से दूर बैठे दर्शक किसी भी रेस्तरां में परोसे जाने वाले खाने का लुफ्त उठा सकते हैं। इतना ही नहीं टीवी की मदद से शेफ बनने के शौकीन लोगों को भी कहीं से भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह अभी दूसरे मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, जिसमें वो इस तकनीक के और भी इस्तेमालों पर विचार कर रहे हैं। जैसे कि टोस्ट में कैसे और फ्लेवर डाला जा सकता है।टीवी के अलावा बनाई ये चीजमीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर होमेइ मियाशिता ने अपनी 30 छात्रों की एक टीम के साथ टीवी के अलावा कई स्वाद से संबंधित प्रोडक्ट तैयार किए हैं। उन्होंने एक ऐसा चम्मच तैयार किया था जिससे खाने पर भोजन का स्वाद और बढ़ जाता है। इसके अलावा वह अब ऐसी स्पे तकनीक पर काम कर रहे हैं जो टोस्टेड ब्रेड का स्वाद पिज्जा या चॉकलेट के स्लाइस की तरह बना सके।यह टीवी किसी अन्य स्मार्ट टीवी की कीमत में ही मिल सकता है। इसकी कीमत लगभग 875 डॉलर यानी 65 हजार रुपए के आस-पास हो सकती है।
- लोबॉरो (ब्रिटेन) ।जब हम पुराने जमाने के खाने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम की तस्वीर सामने आती है जिनके सामने टेबल पर मांस से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन दिखते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि हमारे पूर्वज सलाद खाने के अधिक स्वास्थ्य फायदों को जानते थे और संभवत: हमारी सोच से कहीं ज्यादा जड़ी-बूटियों यां सब्जियों के बारे में सोचते थे। अतीत की सतत आत्मनिर्भरता को देखते हुए हम पाते हैं कि हम कई प्रकार के ऐतिहासिक सलाद व्यंजनों के बारे में जान सकते हैं जिन पर लगभग कोई खर्च नहीं आता है और कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है और संभवत: हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं। डायरी लेखक और उद्यान में रुचि रखने वाले जॉन इवेलिन (1620-1706) ने 17वीं सदी के मध्य में सलाद को लेकर अपनी रुचि दिखाई थी। इसमें उन्होंने प्रत्येक व्यंजन की विस्तार से जानकारी देने के साथ यह भी बताया है कि कैसे घर में ही सालभर सलाद के लिए सामग्री पैदा कर सकते हैं। इवेलिन के लिए आदर्श किचन गार्डन का अभिप्राय था कि वह ऐसी सब्जियों और फलों से भरा हो जिन्हें आसानी से उगाया जा सके, साथ ही उनमें विविधता भी हो। इवेलिन ने यहां तक सलाद बनाने की और उसके लिए सामग्री उगाने की पूरी निर्देशिका ‘एसिटेरिया- ए डिस्कोर्स ऑन सैलेट्स' के नाम से सन 1699 में प्रकाशित की थी। ‘‘सैलेट'' शब्द अंग्रेजी भाषा में फ्रांसीसी शब्द ‘सलाद' से 13वीं सदी में आया और 16वीं सदी में इस शब्द का आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता था। ‘एसिटेरिया' में इवेलिन ने कम मांस वाले भोजन को प्रोत्साहित किया और जोर दिया कि जो लोग जड़ी-बूटी और जड़ों पर जिंदा रहते हैं, वे लंबे समय तक जीते हैं। अपनी बात को पुख्ता रूप से रखने के लिए वह पंरपरागत दर्शन का हवाला देते थे और महान विचारक प्लेटो एवं पाइथागोरस का उदाहरण देते थे जिन्होंने अपनी खाने की मेज पर से ‘मांस' को बिल्कुल हटा दिया था। पिछले साल बागवानी और सब्जियों को उगाने का चलन बढ़ा है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना शायद संभव नहीं हो लेकिन इवेलिन की ‘एसिटेरिया' कुछ नुस्खे देती है जिससे घर में उगाए खाद्य सामग्री का इस्तेमाल परिवार को खिलाने में किया जा सकता है और कुछ सुझाव भी देती है जिससे असामान्य तरीके से उत्पादन का विस्तार किया जा सकता है। माली का वर्ष इवेलिन के घोषणापत्र के केंद्र में सलाद है जो उन्होंने ‘एसिटेरिया' में लिखी कविता में रेखांकित किया, ‘‘ रोटी, शराब और कुछ सलाद जो आप खरीद सकते हो लेकिन प्रकृति से क्या जोड़ता है? वह है विलासिता।'' इस कविता में सलाद खरीदने का संदर्भ दिया गया है। इवेलिन रेखांकित करते हैं कि ऐसे पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं और इनके व्यंजन बनाने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और पचाने में भी आसान हैं। यह किताब खाना बनाने के लिए सामग्री का उत्पादन करने के संकेत और नुस्खा बताती है।वह गुलबहार, दलदली गेंदा आदि के सलाद की भी बात करते हैं। ये और कई तरह के पौधे बेकार जमीन पर भी उगाए जा सकते हैं और माली को बिना कीमत आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं। कई तरह के ‘‘खरपतवारों' को सही समय पर लिया जा सकता है और कई बार कड़वापन खत्म करने के लिए उनकी जड़ों को उबालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, आधुनिक काल के शुरुआती दिनों में कच्ची सब्जियों को खाने को लेकर चिंता जताई जाती थी कि अगर अधिक खाया जाए तो पाचन तंत्र खराब हो सकता है। हालांकि, मुख्य बिंदु यह है कि उन्होंने विस्तृत परिभाषा दी है कि सलाद में किन-किन चीजों को शामिल किया जा सकता है जैसे उच्च श्रेणी के रेस्तरां में जगली पौधों की वापसी। सलाद, ‘‘शहर के दावत के लिए उपयुक्त''एक व्यंजन बनाने की विधि जो इवेलिन ने दी है और उसकी समीक्षा करने के बाद सलाद ऐसी हो सकती है-सलाद में पड़ने वाली सामग्री : छिलके वाले बादाम कटे हुए, ठंडे पानी में भिगोए हुए मसालेदार खीरे, कॉनिलियन्स (एक प्रकार की चेरी), जामुन, चुकुंदर, जलकुंभी के डंठल, अखरोट, मसालेदार मशरुम, संतरे के छिलके आदि। बनाने की विधि : उपरोक्त सामग्री को काट लें और उनमें भुना हुआ अखरोट, पिस्ता, बादाम आदि डाले और फूलों से सजाएं और उस पर गुलाबजल का छिड़काव करें। साथ में सिरका में भिगोए फूल भी रख सकते हैं। इवेलिन की किताब का संदेश है कि प्रकृति ने जो दिया है, उसका इस्तेमाल करें।
- 68 इंच है घोड़े की लंबाईमुंबई। महाराष्ट्र के देशभर में प्रसिद्ध सारंगखेड़ यात्रा में राज्य भर से घोड़े बिक्री के लिए आते हैं। यहां बिकने आने वाले कई घोड़ों की कीमत करोड़ों में होती है। हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक का एक घोड़ा जिसका नाम 'रावण' है, चर्चाओं में हैं। इस राकाले घोड़े की कीमत मेले में 5 करोड़ लगाई जा रही है। 5 करोड़ में इस घोड़े को खरीदने के लिए कई लोग तैयार हैं। इस घोड़े की लंबाई 68 इंच है। इसे चमकदार बनाने के लिए दूध, घी, अंडा, और सूखे मेवे खिलाए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हर दिन 1 किलो घी और 10 लीटर दूध पीता है। घोड़े के मालिक मुंबई निवासी असद सैयद ने इसे बेचने से इनकार कर दिया है।
- 50 फीट है मछली की लंबाईहैदराबाद। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में तांताडी समुद्र तट पर मछली पकड़ने के जाल में दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क फंस गई। इसके बाद कुछ स्थानीय मछुआरों ने जाल में फंसी 50 फीट लंबी मछली को फिर से समुद्र में छोड़ दिया। जिला वन अधिकारी अनंत शंकर ने बताया कि वन विभाग, मछुआरों और वन्यजीव संरक्षणवादियों के जबरदस्त कॉर्डिनेशन और सहयोग से 2 टन की व्हेल शार्क को समुद्र में वापस भेजा गया। यह एक व्हेल शार्क है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। जिला वन अधिकारी ने कहा पहचान के लिए व्हेल शार्क की तस्वीरें अब मालदीव में शार्क अनुसंधान दल के साथ शेयर की गई हैं।
- हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है स्कूल लाइफ. जहां हम अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करते हैं और अपने सुनहरे भविष्य की नींव रखते हैं. कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती करने के अलावा एक और चीज है जो हमें सबसे ज्यादा याद रहती है और वो है स्कूल की पनिशमेंट.उठक-बैठक लगाने के पीछे छिपा एक वैज्ञानिक कारणआपको भी कभी न कभी अपने स्कूल में इस तरह की पनिशमेंट मिली ही होगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में कान पकड़ कर उठक-बैठक लगाने की ही सजा क्यों मिलती है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? जी हां, कोई भी चीज बेवजह नहीं होती और कान पकड़ कर उठक-बैठक लगाने के पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है.क्या है वजहमाना जाता है कि उठक-बैठक करने से बच्चों की याद्दाश्त तेज होती है और मस्तिष्क के कई हिस्से सक्रिय हो जाते हैं. इससे एलर्ट रहने, याद्दाश्त और बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार आता है. यही वजह है कि बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट के तौर पर कान-पकड़ कर उठक-बैठक लगाने के लिए कहा जाता है. इससे बच्चों की याद्दाश्त तेज होती है जो उन्हें सीधे तौर पर पढ़ाई में फायदा पहुंचाती है.कैसे पहुंचता है फायदाइस संदर्भ में पिछले कुछ दशकों में कई रिसर्च की गई हैं. रिसर्च के दौरान पता चला है कि एक मिनट तक कान पकड़ कर उठक-बैठक लगाने से ही दिमाग के अंदर अल्फा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में कानों के लोब पर दबाव पड़ता है, जो एक्यूप्रेशर के अनुसार मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से को सक्रिय करता है और संबंधित पिट्यूटरी ग्रंथि को एक्टिवेट करता है. इस तरह दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है.कब तक रहते हैं फायदेइसे आप एक्सरसाइज भी मान सकते हैं लेकिन यह जरूर जान लें कि अगर इसे रोज न किया जाए तो इससे मिलने वाले फायदे अस्थायी होते हैं. बच्चों के दिमाग को तेज करने और मस्तिष्क की कोशिकाओं को ताकत देने के लिए आप उन्हें सुपर ब्रेन योगा भी करवा सकते हैं.
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा स्पेस के रहस्यों को जानने की कोशिश रहा है। अब इस बीच नासा ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बारे में जानकर दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैरान हैं। नासा ने अपना जूनो मिशन साल 2016 में शुरू किया था जिसने हाल ही में बृहस्पति के पास 38वीं उड़ान भरी है। नासा ने इस मिशन को इस साल की शुरुआत में बढ़ा दिया था। इसमें जून में बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड की करीब से उड़ान भरना था। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति ग्रह और गैनीमेड के पास से उड़ान भरी और इस दौरान रहस्यमयी आवाज को रिकॉर्ड किया था और कुछ हैरान करने वाली तस्वीरों को भी खींचा था।नासा ने खुलासा करते हुए बताया है कि जूनो स्पेसक्राफ्ट ने एक रहस्यमयी आवाज को रिकॉर्ड किया है जो 50 सेंकेड का है। चंद्रमा के ऑडियो की क्लिप को विद्युत और चुंबकीय रेडियो तरंगों ने बनाया था। इन तंरगों के बारे में जानने के लिए स्पेसक्राफ्ट के वेव्स इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया जिससे यह डिटेक्ट हो पाया। रिकॉर्ड की गई आवाजें एक ट्रिपी स्पेस एज साउंडट्रैक जैसी हैं।जूनो मिशन की टीम उड़ान के दौरान स्पेसक्राफ्ट द्वारा बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड से मिले डाटा के बारे में जाच कर रही है। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने गैनीमेड चंद्रमा सतह से 1,038 किलोमीटर दूरी से उड़ान भरा था। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट 67,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा है।जूनो मिशन की टीम ने जूनो मिशन के स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई तस्वीरों को शेयर किया है। इन तस्वीरों में ग्रह के घूमने वाले वातावरण की खूबसूरती को देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह पर आए तूफान की तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। बृहस्पति के वायुमंडलीय डायनेमिक्स और पृथ्वी के महासागरों के भंवरों में समानताएं नजर आ रही हैं।जूनो स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा की मदद से वैज्ञानिक ग्रेट ब्लू स्पॉट और बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र का नक्शा बनाने का काम कर रहे हैं। ग्रेट रेड स्पॉट एक ग्रह के भूमध्य रेखा पर सालों से आया तूफान है। जूनो मिशन की टीम ने ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव को देखा है।-
- केप केनवेरल (अमेरिका) ।अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि वह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अगले शुक्रवार को प्रक्षेपित कराएगा। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने शुक्रवार को बताया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 24 दिसंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। यूरोपीय एरियन रॉकेट दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुएना से इसे लेकर रवाना होगा। वेब को हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और इसे शनिवार को प्रक्षेपित कराया जाना था लेकिन तकनीकी खामियों के चलते प्रक्षेपण के काम में पहले चार दिन और फिर दो और दिन की देरी हुई। अब इसे प्रक्षेपित कराने के लिए अगले शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है। नेल्सन ने छुट्टी का दिन होने के कारण प्रक्षेपण स्थल पर कम लोगों के मौजूद होने की संभावना है। यह प्रक्षेपण ईस्टर्न टाइम जोन (ईएसटी) सुबह सात बजकर 20 मिनट पर होगा। उन्होंने ‘एसोसिएटेड प्रेस' से कहा, ‘‘चूंकि क्रिसमस की पूर्व संध्या है इसलिए अमेरिकी कांग्रेस से जुड़े अधिकारी भी नहीं रहेंगे।'' यहां तक कि नासा और कॉन्ट्रैक्टर टीम के लोग भी कम ही होंगे, लेकिन वह खुद वहां मौजूद रहेंगे। इस परियोजना में नासा यूरोपीय और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिल कर काम कर रहा है। उन्होंने कहा,‘‘ इससे बहुत कुछ हासिल होगा। ब्रह्मांड के बारे में नयी बातें जानने और नयी समझ पैदा करने में मदद मिलेगी।'-
-
दुनियाभर में कई तरह के मसाले पाए जाते हैं जिनका खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सभी मसालों की कीमत अलग-अलग होती है। ये मसाले अपने बेहतरीन स्वाद और अलग-अलग वजहों से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आपको एक ऐसे ही मसाले के बारे में बताते हैं जो दुनिया में मिलने वाले मसालों में सबसे महंगा है। इस मसाले की कीमत बाजार में इतनी है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।
दुनिया में सबसे महंगा बिकने वाले इस मसाले को लोग रेड गोल्ड भी कहते हैं। इस मसाले के बारे में हस सभी जानते हैं। इस मसाले का नाम कुछ और नहीं बल्कि केसर है। वर्तमान समय में बाजार में केसर सबसे महंगा मसाला है। एक किलोग्राम केसर की कीमत ढाई लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक होती है। आईए जानते हैं आखिर इस मसाले में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह दुनिया का सबसे महंगा मसाला है।
केसर की कीमत हीरे की तरह होने की कई वजहे हैं। बताया जाता है कि इसके पौधों के डेढ़ लाख फूलों से सिर्फ एक किलो केसर निकलता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके एक फूल से सिर्फ तीन केसर ही मिलते हैं। यह भी जानकर आपको हैरानी होगी कि केसर का पौधा भी काफी मंहगा बिकता है। केसर के पौधे को दुनिया में सबसे महंगा पौधा कहा जाता है। जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में केसर की खेती की जाती है।
इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि सबसे पहले केसर की खेती कहां हुई थी। बताया जाता है कि लगभग 2300 साल पहले ग्रीस (यूनान) में सिकंदर महान की सेना ने सबसे पहले इसकी खेती की थी। केसर का मसालों के अलावा कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। सेहत के लिए केसर को अच्छा माना जाता है। इसका इस्तेमाल चेहरे पर लगाने वाली क्रीम में भी किया जाता है। केसर का अलग-अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। - रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप की नजर पटरियों पर पड़ी होगी। पटरी के इर्द-गिर्द भले ही जंग लगा हो ,लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा हमेशा चमचमाता नजर आता है। पटरी के इस हिस्से पर कभी जंग नहीं लगती। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह इसके बनावट का तरीका। जानिए पटरी के ऊपरी हिस्से पर जंग क्यों नहीं लगता-आमतौर पर लोहे की चीजों में जंग तब लगती है जब इससे तैयार कोई भी सामान हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन के बाद उस चीज पर एक भूरे रंग की पर्त जम जाती है। यह आयरन ऑक्साइड होता है। यह पर्तों के रूप में जमता है। जैसे-जैसे पर्त बढ़ती है, जंग का दायरा बढ़ता जाता है।अब जानिए, पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती। रेलवे की पटरियों को खास तरह के स्टील से तैयार किया जाता है। इसे मैंग्नीज स्टील कहते हैं। इस खास तरह के स्टील में 12 फीसदी मैंग्नीज और 0.8 फीसदी कार्बन होता है। पटरी में ये मैटल्स के होने के कारण आयरन ऑक्साइड नहीं बनता और इस तरह पटरियों पर जंग नहीं लगती।अगर रेलवे की पटरियों को लोहे से तैयार किया जाता तो बारिश के कारण इनमें नमीं बनी रहती। इनमें जंग लग जाती। ऐसा होने के बाद पटरियां कमजोर लेने लगती और इन्हें जल्दी-जल्दी बदलने की नौबत आ जाती। पटरी कमजोर होने के कारण दुर्घटनाओं का भी रिस्क बढ़ता। इसलिए पटरियों को ऐसे मेटल से तैयार किया गया है, जिससे इसमें जंग नहीं लगती।
- सालों से दुनियाभर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर नजर जमाए हुए हैं। इस दौरान वैज्ञानिकों को नए-नए ग्रह भी मिलते रहते हैं। वहीं कभी-कभी अंतरिक्ष में ऐसे नजारे भी दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक विशालकाय ग्रह का पता लगाया है जो आकार में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह यानी बृहस्पति से भी 11 गुना बड़ा है। इस विशालकाय ग्रह के बारे में चिली के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है।इस विशालकाय ग्रह की तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिक भी हैरत में हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये ग्रह दक्षिणी आकाश में दो चमकदार सितारों का चक्कर लगा रहा है। इस ग्रह को बी-सेंचुरी नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 325 प्रकाश वर्ष दूर है। आईये इस रिपोर्ट में जानते हैं इस विशालकाय ग्रह के बारे में और भी हैरान कर देने वाली बातें...चिली के यूरोपीयन टेलिस्कोप के जरिए मार्कस जॉनसन और उनकी टीम ने इस ग्रह की खोज की है। धरती से करीब 325 प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में घूम रहा ये ग्रह गैस से भरा हुआ है। वहीं इस ग्रह का परिक्रमा पथ बृहस्पति ग्रह से 100 गुना चौड़ा है। एक अध्ययन के जरिए वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के बारे में पूरा विवरण दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब एक गैस से भरे ग्रह को एक सितारे के आसपास खोजा गया है जो सूर्य से आकार में तीन गुना बड़ा है।इस नए ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिक मार्कस जॉनसन ने कहा 'मैंने सोचा था कि सितारों के आसपास ऐसा कोई ग्रह नहीं होगा जो रोचक होगा, लेकिन इसके आसपास कई ग्रह मौजूद हैं जो और ज्यादा रोचक हो सकते हैं।' वैज्ञानिकों ने बताया कि बी सेंचुरी सिस्टम में दो सितारे हैं- बी सेंचुरी A और बी सेंचुरी B।वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इन दोनों को मिला दिया जाय तो ये सूरज से 6 से 10 गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों ही बहुत गरम हैं। वहीं मार्कस जॉनसन ने कहा कि इस ग्रह के बारे में अब तक मिली जानकारी बहुत ही अजीब है।







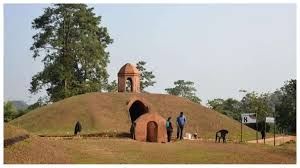
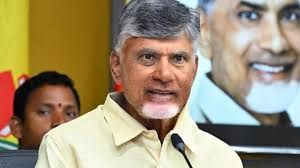
.jpeg)
.jpeg)



.jpg)



.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)



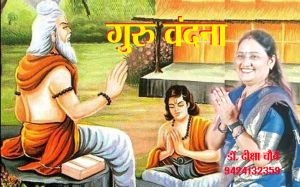
.jpg)

.jpeg)


.jpg)
.jpg)





.jpg)



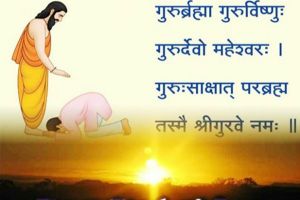

























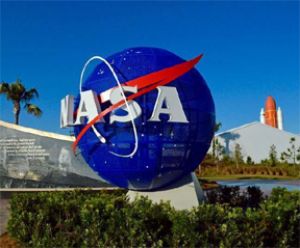

.jpg)


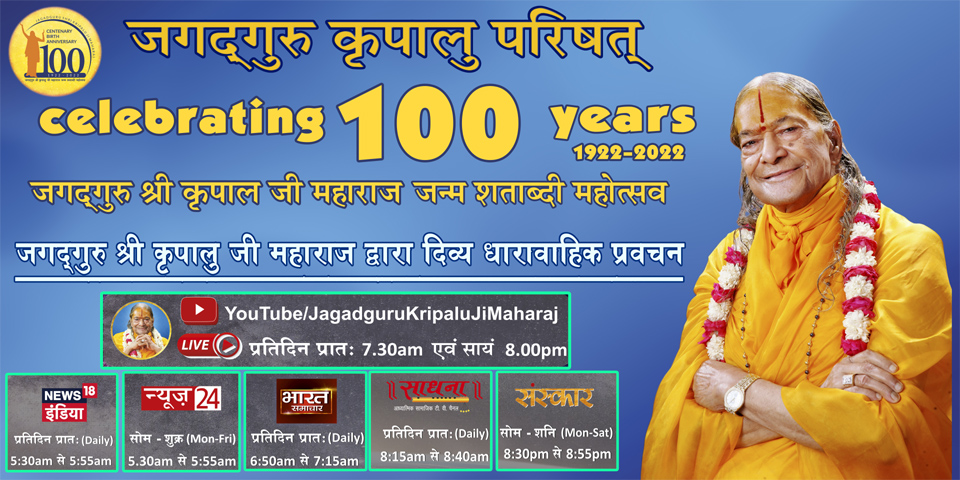

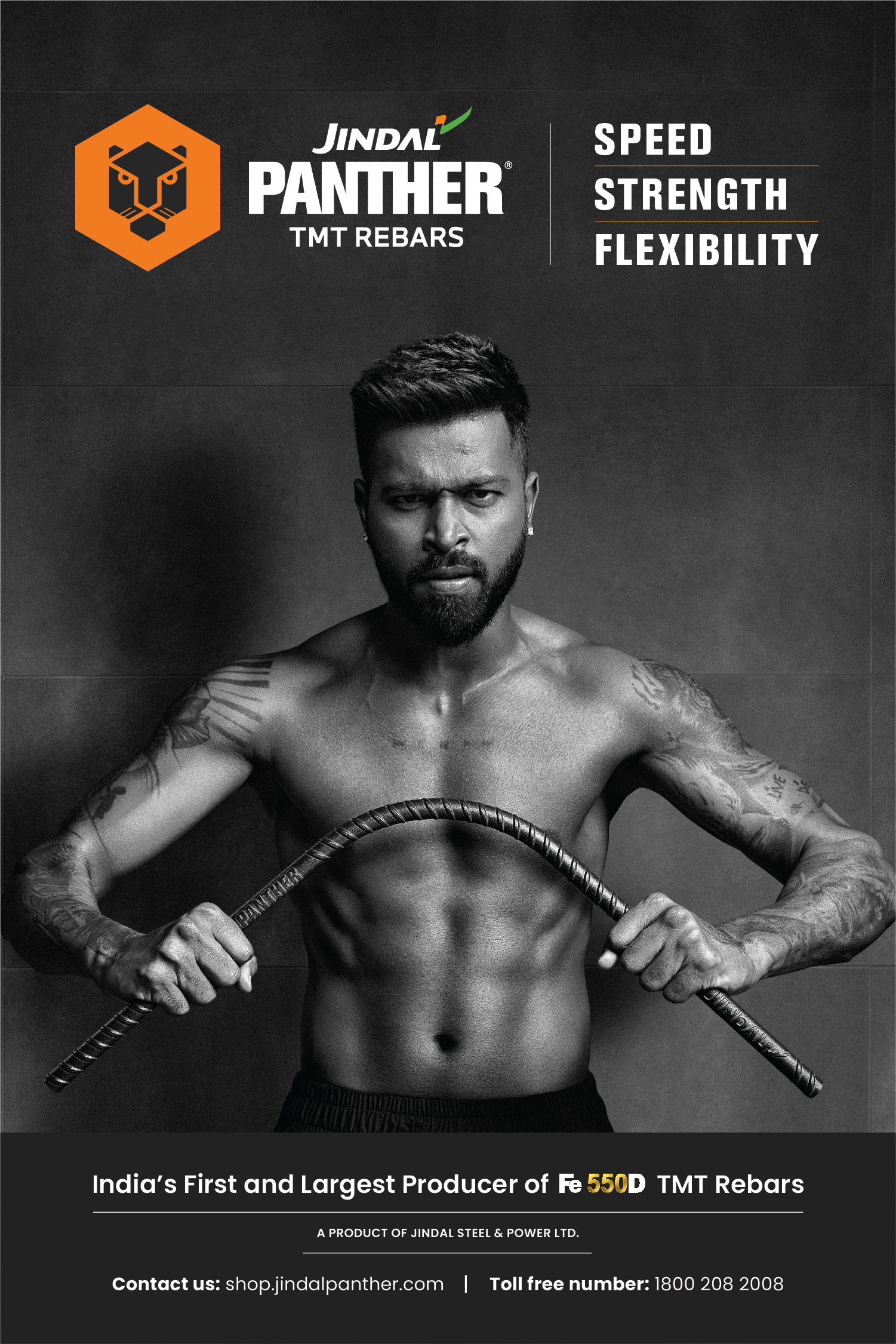
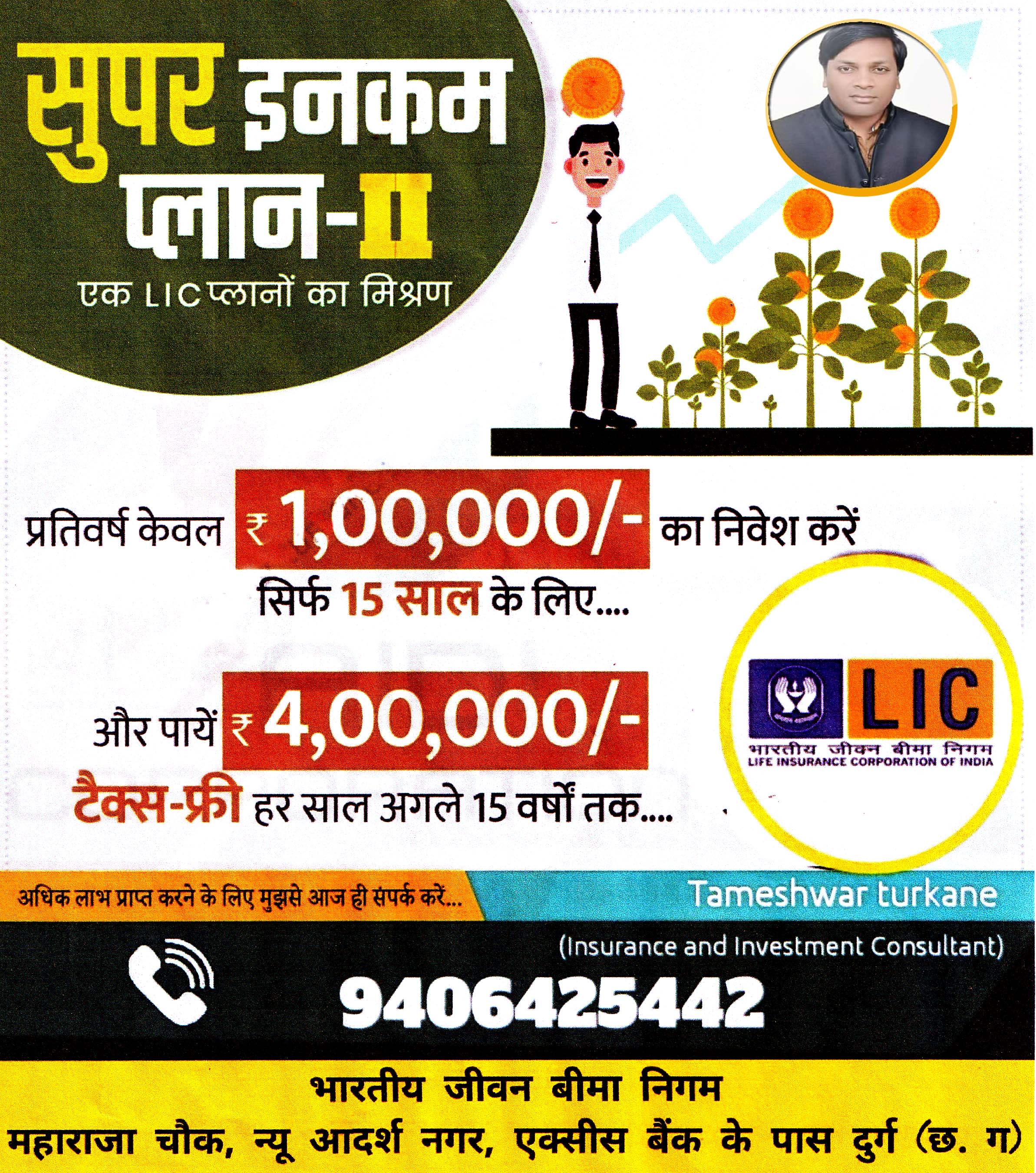
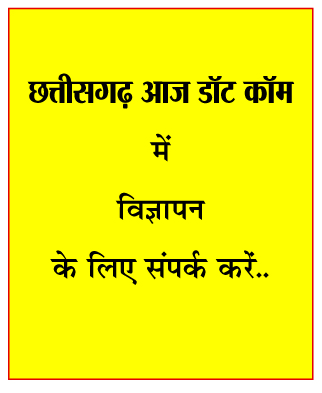
.jpg)
.jpg)