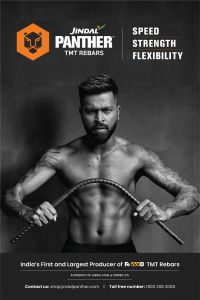- Home
- ज्ञान विज्ञान
-
नयी दिल्ली. एक अध्ययन में दावा किया गया है कि पौधों में पाया जाने वाला एक तत्व ‘साइटिसिन', प्लसीबो की तुलना में सफलतापूर्वक धूम्रपान छोड़ने की संभावना को दो गुना बढ़ा देता है और ‘निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी' से अधिक प्रभावी हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि कम लागत वाले एवं धूम्रपान रोकने में मददगार ‘साइटिसिन' का उपयोग पूर्वी यूरोप में 1960 के दशक से किया जा रहा है और इसके उपयोग के बाद कोई गंभीर सुरक्षा चिंताएं नहीं देखी गई हैं। प्लसीबो, ऐसी चिकित्सा को कहते हैं जिसका वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ऐसी चिकित्सा पद्धति या तो प्रभावहीन होती है, या फिर यदि कोई सुधार दिखता भी है तो उसका कारण अन्य होता है। साइटिसिन को मध्य और पूर्वी यूरोप के बाहर के अधिकतर देशों में लाइसेंस प्राप्त नहीं है और ना ही इसका विपणन किया जाता है, जिसके चलते यह दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उपलब्ध नहीं है। इस सूची में निम्न और मध्यम आय (एलएएमआई) वाले देश भी शामिल हैं, जहां यह वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। जर्नल ‘एडिक्शन' में प्रकाशित अध्ययन में लगभग 6,000 रोगियों पर प्लसीबो के साथ साइटिसिन की तुलना करने वाले आठ परीक्षणों के परिणामों को एकत्रित किया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक, संयुक्त परिणामों से पता चला है कि साइटिसिन, प्लसीबो की तुलना में धूम्रपान बंद करने की संभावना को दो गुना से अधिक बढ़ा देता है। उन्होंने यह भी पाया कि ‘निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी' की तुलना में साइटिसिन अधिक प्रभावी हो सकता है।
‘निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी' तंबाकू के अलावा अन्य माध्यमों से निकोटिन लेकर तंबाकू सेवन विकार वाले लोगों के इलाज के लिए एक चिकित्सकीय रूप से अनुमोदित तरीका है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स स्थित ‘सेंट्रो नेशनल डी इन्टॉक्सिकेशियंस' (सीएनआई) से जुड़े एवं शोधकर्ता ओ. डी. सैंटी ने कहा, ‘‘हमारा अध्ययन इस सबूत को पुख्ता करता है कि साइटिसिन धूम्रपान रोकने में एक प्रभावी और सस्ता तरीका है। यह एलएएमआई देशों में धूम्रपान की समस्या से निपटने में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, जहां धूम्रपान छोड़ने वाली किफायती दवाओं की तत्काल आवश्यकता है। -
गक्बेरहा (दक्षिण अफ्रीका)। पिछले 15 वर्षों में, चिन्हों और निशानों के हमारे वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से, हमने दक्षिण अफ्रीका के केप दक्षिणी तट से 350 से अधिक जीवाश्म कशेरुकी ट्रैकसाइट्स की पहचान की है। अधिकांश सीमेंटेड रेत के टीलों में पाए जाते हैं, जिन्हें एओलियनाइट्स कहा जाता है, और सभी प्लेइस्टोसिन युग के हैं, जिनकी उम्र लगभग 35,000 से 400,000 वर्ष तक है। उस दौरान हमने अपने पहचान कौशल को निखारा है और ट्रैकसाइट्स को खोजने और उनकी व्याख्या करने के आदी हो गए हैं - एक क्षेत्र जिसे इच्नोलॉजी कहा जाता है। और फिर भी, कभी-कभार, हमारा सामना किसी ऐसी चीज़ से होता है जिसके बारे में हमें तुरंत पता चलता है कि यह इतना अनोखा है कि यह पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाया गया है।
अप्रत्याशित खोज का ऐसा क्षण 2019 में केप टाउन से लगभग 200 किमी पूर्व में डी हूप नेचर रिजर्व के समुद्र तट पर हुआ। जीवाश्म हाथियों के ट्रैक के समूह से दो मीटर से भी कम दूरी पर 57 सेमी व्यास वाली एक गोल संरचना थी, जिसमें संकेंद्रित वलय विशेषताएं थीं। इस सतह से लगभग 7 सेमी नीचे एक और परत उजागर हुई। इसमें कम से कम 14 समानांतर खांचे थे। खांचे छल्लों के पास पहुंचकर उनकी ओर थोड़ा सा मुड़ गए थे। इस संरचना को देखकर हमने जिन दो निष्कर्षों की परिकल्पना की थी, वे एक-दूसरे से जुड़े हुए थे और एक ही मूल के प्रतीत होते थे। हाथी ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़े, भारी जानवर हैं। वे बड़े, गहरे, आसानी से पहचाने जाने योग्य निशान छोड़ते हैं। हमने अपने अध्ययन क्षेत्र में 35 जीवाश्म हाथी ट्रैक साइटों का दस्तावेजीकरण किया है, साथ ही जीवाश्म हाथी ट्रंक-ड्रैग इंप्रेशन का पहला सबूत भी प्राप्त किया है। हाथियों को, विशाल भूमि प्राणियों के एक अन्य समूह, डायनासोर की तरह, भूवैज्ञानिक इंजीनियरों के रूप में देखा जा सकता है जो जिस जमीन पर चलते हैं, उस पर छोटे-मोटे पृथ्वी-चालित बल बनाते हैं। इसे हाथियों की एक उल्लेखनीय क्षमता से भी जोड़ा जा सकता है: भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करके संचार करना। ये ऊर्जा का एक रूप है जो पृथ्वी की सतह के नीचे यात्रा कर सकता है। 2019 में हमें जो निशान मिले, वह ऐसी ही एक घटना को प्रतिबिंबित करते प्रतीत हुए: एक हाथी जो लहरों को ट्रिगर कर रहा था जो बाहर की ओर तरंगित हो रही थी। अतिरिक्त जांच और वैकल्पिक स्पष्टीकरणों की गहन खोज के बाद, हम हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारा मानना है कि हमें हाथियों के बीच भूकंपीय, भूमिगत संचार का दुनिया का पहला जीवाश्म निशान मिला है।
1980 के दशक के बाद से, साहित्य के एक निरंतर बढ़ते समूह ने इन्फ्रासाउंड के माध्यम से ‘‘हाथी भूकंपीयता'' और भूकंपीय संचार का दस्तावेजीकरण किया है। मानव श्रवण की निचली सीमा 20एचजैड है; उससे नीचे, कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को इन्फ्रासाउंड के रूप में जाना जाता है। हाथी की ‘‘गड़गड़ाहट'', जो स्वरयंत्र से उत्पन्न होती है और अंगों के माध्यम से जमीन में संचारित होती है, इन्फ्रासोनिक रेंज के अंतर्गत आती है। उच्च आयाम पर इन्फ्रासाउंड (थोड़ी अधिक आवृत्ति पर यह हमें बहुत तेज़ लगेगा) उच्च आवृत्ति ध्वनियों की तुलना में 6 किमी तक की दूरी तक यात्रा कर सकता है। यहां हाथियों को फायदा है। हल्के जीव आवाज के माध्यम से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि लंबी दूरी का भूकंपीय संचार हाथियों के समूहों को पर्याप्त दूरी तक संवाद करने का अवसर दे सकता है, और यह दिखाया गया है कि रेतीले इलाके संचार को सबसे दूर तक यात्रा करने में मदद देते हैं।
वैज्ञानिकों के लिए हाथी की भूकंपीयता अध्ययन का एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। हालाँकि, जो लोग हाथियों के करीब रह चुके हैं उन्हें जानवरों के कंपन के माध्यम से संचार करने के विचार पर आश्चर्य नहीं होगा। वास्तव में, हाथियों की गड़गड़ाहट से होने वाले कंपन को कभी-कभी चतुर पर्यवेक्षक द्वारा महसूस किया जा सकता है (सुनने के बजाय)। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह ज्ञान एकदम नया नहीं है। हमारी टीम के रॉक कला विशेषज्ञों ने रॉक कला की पहचान की है और उसकी व्याख्या की है, जिससे पता चलता है कि हजारों साल पहले स्वदेशी सैन लोगों ने दक्षिणी अफ्रीका में इस ज्ञान का पता लगाया था। सैन के लिए हाथियों का अत्यधिक महत्व था और उनकी कला कृतियों में इन्हें प्रमुखता से दर्शाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कई शैल कला स्थलों में ध्वनि या कंपन के संबंध में हाथियों के चित्र मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, सेडरबर्ग में मोंटे क्रिस्टो साइट पर कलाकार ने कई समूहों में 31 हाथियों को चित्रित किया है। वे एक यथार्थवादी व्यवस्था में हैं. प्रत्येक हाथी को महीन लाल रेखाएँ घेरती हैं; टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ पेट, कमर, गले, धड़ और विशेष रूप से पैरों को छूती हैं। कई टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ हाथी को ज़मीन से जोड़ती हैं। बेहतरीन रेखाएँ हाथियों के सबसे करीब होती हैं, और प्रत्येक हाथी रेखाओं के इस सेट से जुड़ा होता है। ये बदले में हाथी समूह के आसपास की व्यापक रेखाओं से जुड़े होते हैं, जो संकेंद्रित वलय के रूप में हाथियों से बाहर और दूर तक विकीर्ण होते हैं। इसकी व्याख्या सैन कलाकार द्वारा हाथियों के बीच भूकंपीय संचार के संभावित चित्रण के रूप में की गई है। झटकों और कंपन की अनुभूति, जिसे सैन थारा एन|ओम कहते हैं, हाथी गीत और हाथी नृत्य सहित सैन उपचार नृत्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की रेखाएँ, जिन्हें एन|ओएम कहा जाता है, एक जीवंत जीवन देने वाली शक्ति के रूप में मानी जाती हैं जो सभी जीवित प्राणियों को अनुप्राणित करती हैं और सभी प्रेरित ऊर्जा का स्रोत हैं। हमारा मानना है कि हाथियों की भूकंपीयता को समझने के लिए ज्ञान के तीन निकायों के एकीकरण की आवश्यकता है: मौजूदा हाथियों की आबादी पर शोध, पैतृक ज्ञान (अक्सर रॉक कला में प्रकट) और ट्रेस जीवाश्म रिकॉर्ड। हाथी का भूकंपीय संचार एक ऐसा निशान छोड़ सकता है जिसका जीवाश्म रिकॉर्ड पहले कभी रिपोर्ट नहीं किया गया था, या यहां तक कि अनुमान भी नहीं लगाया गया था। हमारे निष्कर्षों में इस क्षेत्र में बहु-विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की क्षमता हो सकती है। इसमें आधुनिक गड़गड़ाते हाथियों के आसपास रेत में उप-सतह पैटर्न की एक समर्पित खोज शामिल हो सकती है। -
स्मार्टफोन के बिना अब जिंदगी की कल्पना करना संभव नहीं। स्मार्टफोन हैं, तो तरह-तरह के ऐप हैं। अपने इस नए कॉलम के जरिए हम आपको देंगे, ऐसे ही उपयोगी ऐप्स की जानकारी। ताकि आपकी जिंदगी बन सके, पहले से कुछ ज्यादा आसान, कुछ ज्यादा मजेदार!
ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए फायदेमंद 'AUTISMBASICS'-
जो काम एक्सपर्ट कर सकते हैं, वह काम हम आम लोगों के लिए कर पाना कई गुना मुश्किल हो जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की परवरिश ऐसी ही एक चीज है। बच्चों की परवरिश यूं ही मुश्किल भरा काम है, उस पर बच्चे को अलग से थेरेपी की जरूरत हो तो चुनौती कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को नियमित रूप से मनोविशेषज्ञ, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। हर अभिभावक की इन तक पहुंच हो, यह संभव नहीं। ऐसे में अपने खास बच्चे की परवरिश को थोड़ा आसान बनाने और उनमें सभी जरूरी स्किल्स को विकसित करने के लिए आप इस ऐप की मदद ले सकती हैं। इसकी मदद से ना सिर्फ आपके लिए अपने बच्चे को नियमित रूप से विभिन्न थेरेपी देना आसान होगा बल्कि यहां अपने जैसे अभिभावकों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को देखकर भी काफी कुछ सीख सकेंगी।
करियर से जुड़ा सही निर्णय लेने के लिए 'AMBITIONBOX'-
अच्छी पढ़ाई, बेहतरीन करियर और खुशहाल जिंदगी...अधिकांश लोगों के सपनों का क्रम अमूमन यही होता है। पर, कई दफा अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद करियर की राह इतनी आसान नहीं होती। योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती है, तो सैलरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती। नौकरी तलाशने की आपकी राह को आसान करने में यह ऐप एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यहां ना सिर्फ आप नौकरी की तलाश कर सकती हैं, बल्कि करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी तैयारियों की रूपरेखा भी तय कर सकती हैं। ऐप पर 32 लाख से ज्यादा कंपनियों के रिव्यू उपलब्ध हैं। कंपनियों द्वारा दिए जा रहे वेतनमान की जानकारी यहां है, साथ ही इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी जानकारी भी आप ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। अपने करियर के बारे में सही निर्णय लेने में यह ऐप आपके लिए मददगार साबित हो सकता है।
स्ट्रेस फ्री रहने के लिए LEVELSUPERMIND-
मन की शांति की तलाश में हम सब हैं, पर बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो अपने इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। मन की शांति पाने में गूगल द्वारा 2023 के सबसे अच्छे ऐप्स में चुना गया यह ऐप आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। यह ऐप ध्यान, नींद और रिलैक्सेशन तकनीकों की मदद से मानसिक शांति पाने में आपकी मदद करेगा। आज के समय में तनाव, एंग्जाइटी और जिंदगी की दैनिक जिम्मेदारियां साथ मिलकर कभी-कभार हम पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। यह ऐप ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, सकारात्मक बातें, अच्छी नींद व अपनों की बातों को एक जगह लिखने के लिए आपको प्रेरित कर मन की उथल-पुथल को शांत करने में आपकी मदद करेगा। यह ऐप अभी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा पांच अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
-
नयी दिल्ली. एक अध्ययन से पता चला है कि चीन, जापान और भारत जैसे देशों में मिलने वाले शाकाहारी और पारंपरिक भोजन अल्जाइमर रोग के खतरे को कम कर सकते हैं, खासकर पश्चिमी देशों के भोजन की तुलना में। अमेरिकी संस्था ‘सनलाइट, न्यूट्रीशन और हेल्थ रिसर्च सेंटर' के शोधकर्ताओं ने पाया कि इन देशों में पोषण युक्त भोजन को पश्चिमी भोजन में बदल दिया जाता है तो इससे अल्जाइमर रोग भी बढ़ जाता है। ‘जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिजीज' में प्रकाशित अध्ययन में अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम करने में आहार की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस अध्ययन में मनोभ्रम के जोखिम के कारकों की पहचान की गई है, जिसमें संतृप्त वसा, मांस, विशेष रूप से हैम्बर्गर तथा बारबेक्यू जैसे कच्चे मांस, साथ ही हॉट डॉग जैसे प्रसंस्कृत मांस और अधिक मात्रा में चीनी तथा परिष्कृत अनाज वाले अत्याधिक-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन करना शामिल हैं। अध्ययन में इस बात का भी विशेलषण किया गया है कि आखिर क्यों कुछ खाद्य पदार्थ अल्जाइमर रोग के खतरे को बढ़ाते या कम करते हैं। उदाहरण के लिए, मांस का सेवन सूजन-जलन, इंसुलिन प्रतिरोध, ऑक्सीडेटिव तनाव, संतृप्त वसा, उन्नत ग्लाइकेशन अंत उत्पाद और ट्राइमेथिलैमाइन एन-ऑक्साइड जैसे जोखिम कारकों को बढ़ाकर मनोभ्रम के खतरे को और अधिक तेज कर देता है। यह भी बताया गया कि शाकाहारी भोजन जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फलियां (जैसे बीन्स), बादाम, और साबुत अनाज अल्जाइमर रोग से हमें एक तरीके से बचाने का काम करते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि अत्याधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ मोटापे और मधुमेह के खतरे को बढ़ा सकते हैं, जो अल्जाइमर रोग के लिए जोखिम कारक हैं।
- किसी भी प्राणी के लिए जीवित रहने से लेकर हेल्दी और फिट रहने तक खून की सही मात्रा बेहद जरूरी है। दुनियाभर में मौजूद सभी लोगों के खून का रंग लाल ही होता है। खून के लाल होने के बावजूद लोगों की नसें नीली और जामुनी रंग की दिखाई देती हैं। लेकिन चोट लगने या इंजरी होने पर हर व्यक्ति के शरीर से निकलने वाला ब्लड या खून लाल रंग का ही होता है। खून में दो तरह की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, एक सफेद रक्त कणिकाएं और दूसरी लाल रक्त कणिकाएं। लेकिन हमें दिखने वाले खून के रंग की बात करें तो वह लाल रंग का ही होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर खून का रंग लाल होने के पीछे क्या कारण है और किस वजह से शरीर में मौजूद ब्लड या खून का रंग लाल ही होता है। आइये इस लेख में विस्तार से जानते हैं खून का रंग लाल क्यों होता है इसे कारण के बारे में।खून का रंग लाल क्यों होता है?साइंस के मुताबिक बिना ऑक्सीजन वाला खून लाल नहीं बल्कि नीले रंग का होता है। हम सभी जानते हैं कि खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स खून की मात्रा को पूरा करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं या रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन ऑक्सीजन होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। शरीर में खून की कमी होने को हीमोग्लोबिन की कमी के नाम से भी जाना जाता है। खून का रंग लाल होने के पीछे ब्लड में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं का अहम रोल होता है। दरअसल ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है।"हीमोग्लोबिन में आयरन के चार अणु मौजूद होते हैं। जब इनपर लाइट पड़ती है, तो इनका रंग लाल हो जाता है। यही कारण है कि जब भी हम खून देखते हैं, तो यह लाल रंग का दिखाई देता है। खून में ऑक्सीजन की कमी होने पर इसके रंग में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, जो आयरन अणु के सतह मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनता है और शरीर में ऑक्सीजन के अणु का प्रवाह मैनेज करता है।शरीर में खून की कमीएनीमिया को शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी भी कहते हैं। यह समस्या कई कारणों से किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकती है। कारणों के आधार पर एनीमिया की बीमारी को अलग-अलग तरह से देखा जाता है। कुछ लोगों में एनीमिया की समस्या आनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है। इस स्थिति में जांच और इलाज दोनों ही अलग तरीके से होता है।एनीमिया की जांच आमतौर पर सीबीसी से हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में यह समस्या एडवांस स्टेज पर होती है। ऐसे में इनका पता लगाने के ये टेस्ट किये जा सकते हैं। एनीमिया होने पर शरीर में थकान, भूख कम लगना, कमजोरी के साथ चक्कर आना और उल्टी व पतली की समस्या हो सकती है।
-
ह्यूस्टन. बैक्टीरिया यानि जीवाणु ऐसी यादों की रचना कर सकते हैं कि कब ऐसी रणनीतियां बनाई जाएं, जो लोगों में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध जैसे खतरनाक संक्रमण पैदा कर सकती हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है। अमेरिका के ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ताओं ने कहा कि ये रणनीतियां जीवाणु को एक ऐसी समूह की रचना में भी मदद करती हैं, जहां लाखों की तादाद में इस तरह के सूक्ष्मजीव एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित निष्कर्षों में बैक्टीरियाल संक्रमण से लड़ने व उन्हें रोकने और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया की समस्या को हल करने की क्षमता दिखाई देती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज एक ऐसे सामान्य रासायनिक तत्व से जुड़ी हुई है, जिसका उपयोग जीवाणु कोशिकाएं यादों को बनाने और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कर सकती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि ई. कोली नाम का जीवाणु अलग-अलग व्यवहारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आयरन के स्तर को एक तरीके के रूप में उपयोग करते हैं, जो कुछ विशिष्ट प्रकार की उत्तेजना होने पर सक्रिय हो जाते हैं। अध्ययन के मुख्य शोधकर्ता सौविक भट्टाचार्य ने कहा, ''जीवाणु का दिमाग नहीं होता लेकिन वे अपने अनुकूल माहौल से जानकारी इकठ्ठा कर सकते हैं और अगर वे बार-बार उस माहौल के संपर्क में आते रहेंगे तो वे जानकारियां संग्रहित कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए बाद में उस तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं।'' शोधकर्ताओं ने चिन्हित किया कि इन सबकी वजह आयरन ही है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्वों में से एक है। हर बैक्टीरिया में आयरन का स्तर अलग-अलग होता है। उन्होंने पाया कि जिन जीवाणु में आयरन का स्तर निम्न था उनमें समूह में रहने की प्रवृति दूसरे जीवाणुओं के मुकाबले ज्यादा बेहतर थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसके विपरीत जो जीवाणु बायोफिल्म बनाते हैं उनकी कोशिकाओं में आयरन का स्तर अधिक होता है। वे बैक्टीरिया, जिनमें एंटीबायोटिक को सहन करने की क्षमता होती है उनमें भी आयरन का स्तर संतुलित पाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, आयरन के स्तर से जुड़ी ये यादें कम से कम चार पीढ़ियों तक बनी रहती हैं और सातवीं पीढ़ी तक नष्ट हो जाती हैं।
-
नयी दिल्ली. अमेरिका में दस लाख से अधिक लोगों के जीनोम विश्लेषण में दर्जनों ऐसे अनुवांशिक जीन स्वरूप मिले हैं जिनसे गांजे के इस्तेमाल से होने वाले विकार पैदा होने का अधिक खतरा है। येल यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में कराए गए इस अध्ययन में ये अनुवांशिक स्वरूप व्यवहार और स्वास्थ्य संबंधी अनेक मुद्दों से जुड़े पाए गए जिनमें फेफड़े का कैंसर भी शामिल है। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि कैनबिस या मारिजुआना (गांजे) का उपयोग करने वाले लगभग एक-तिहाई लोगों में कैनबिस यूज डिसऑर्डर विकसित होता है, जिसे कैनबिस के उपयोग के एक समस्याग्रस्त पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैनबिस में भांग के पौधे की सूखी पत्तियां होती हैं और इसका धूम्रपान करके या चबाकर इस्तेमाल किया जाता है। नेचर जेनेटिक्स पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में यह दावा किया गया है।
मनोविज्ञान, अनुवांशिकी और तंत्रिका विज्ञान के प्रोफेसर जोएल गेलेर्नटर ने कहा, ‘‘यह कैनबिस यूज डिसऑर्डर का अब तक का सबसे बड़ा जीनोम अध्ययन है और जितने अधिक (अमेरिकी) राज्य मारिजुआना के उपयोग को वैध या अपराधमुक्त करेंगे, ऐसे अध्ययन हमें इसके बढ़ते उपयोग के साथ होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को समझने में मदद कर सकते हैं। -
बेंगलुरु. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की है। नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) की निदेशक लॉरी लेशिन ने यहां इसरो मुख्यालय का दौरा किया और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस. सोमनाथ के साथ बैठक की। इसरो ने एक बयान में कहा,'' डॉ. लॉरी लेशिन ने इसरो के यूआर राव उपग्रह केंद्र (यूआरएससी) में जेपीएल और इसरो के अधिकारियों के एक टीम के रूप में संयुक्त प्रयासों पर खुशी प्रकट की, जो नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) को विकसित करने में जुटे हुए हैं।'' इसरो ने कहा कि लेशिन की 15 नवंबर को हुई यात्रा के दौरान निसार के प्रक्षेपण की तैयारी और तकनीकी क्षेत्रों एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में पेशेवरों का आदान-प्रदान सहित भविष्य के सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की गई। इसरो सूत्रों ने कहा कि निसार एक पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) वाला वेधशाला है जिसे ‘अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' (नासा) और इसरो संयुक्त रूप से विकसित कर रहा है। निसार का 2024 की पहली तिमाही में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किये जाने की उम्मीद है। इसरो के अनुसार, ''निसार 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का मानचित्रण करेगा और इसकी पारिस्थितिकी, ग्लेशियर के द्रव्यमान, वनस्पति जैव भार (बायोमास), समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदाओं के खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक डेटा प्रदान करेगा।'
-
बेंगलुरु. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक अंतरिक्ष प्रतियोगिता के जरिये युवाओं से भविष्य में भेजे जाने वाले रोबोटिक रोवर्स संबंधी मौलिक विचार और डिजाइन भेजने को कहा है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की सफल ‘सॉफ्ट लैंडिंग' और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अन्वेषण के बाद, इसरो ने कहा कि वह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए भविष्य के रोबोटिक अन्वेषण अभियानों की तैयारी कर रहा है। यहां स्थित मुख्यालय में इसरो ने कहा कि वह संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए शिक्षा जगत और उद्योगों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन ने कहा, ‘‘इस दृष्टिकोण के अनुरूप, यू आर राव उपग्रह केंद्र (यूआरएससी)/इसरो अंतरिक्ष रोबोटिक्स में विकास के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक अंतरिक्ष रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा आयोजित करेगा जिसके माध्यम से भारत के युवाओं से भविष्य के मिशन के लिए रोबोटिक रोवर्स के मौलिक विचारों और डिजाइन का आह्वान किया जाता है। इससे इसरो के अंतर-ग्रहीय मिशन के प्रति देश के युवाओं में रचनात्मक सोच विकसित करने का मौका मिलेगा।'' इसरो ने बयान में कहा कि अंतरिक्ष रोबोटिक्स के क्षेत्र में छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए, ‘इसरो रोबोटिक्स चैलेंज-यूआरएससी 2024 (आईआरओसी-यू 2024)' का आयोजन ‘आओ एक अंतरिक्ष रोबोट बनाएं' की टैगलाइन के साथ किया जाएगा। संगठन ने कहा कि अंतिम प्रतियोगिता अगस्त 2024 में यूआरएससी बेंगलुरु परिसर में आयोजित करने की योजना है।
-
नयी दिल्ली. आधुनिक विश्व में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण जल, थल और नभ में इस कदर व्याप्त हो गये हैं कि इनसे किसी भी प्राणी का अछूता रहना लगभग असंभव हो गया है। प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका ‘यूरोप एक्वाकल्चर' में छपे ताजा शोध पत्र के अनुसार हम जिस "टी-बैग" को गर्म पानी में डालकर चाय बनाते हैं, उसके माध्यम से भी ऐसे कण शरीर के भीतर रक्त में घुल रहे हैं। इस शोध पत्र के लेखक पद्मश्री से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक डॉ. अजय कुमार सोनकर ने कहा, ‘‘हमारी कल्पना के परे अनेक माध्यमों से माइक्रॉन व नैनो आकार के प्लास्टिक के कण हमारे खून में निरंतर पहुँच रहे हैं।'' अपने शोध का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि प्लास्टिक एक अप्राकृतिक पदार्थ है, जिसका एक सामान्य गुण होता है कि समय बीतने के साथ वह अपना लचीलापन खो देता है और भंगुर होकर टूटता है। उन्होंने कहा, ‘‘ इन कणों की भंगुर होने की प्रक्रिया धूप और संक्षारक (कोरोसिव) वातावरण में तेज हो जाती है, तो इसके कण ‘माइक्रॉन' और ‘नैनो पार्टिकल' में बदलकर पूरे वातावरण में फैल जाते हैं और बरसात के पानी के साथ हर जल स्रोत (नदी पोखर, सिंचाई के पानी) में पहुंचते हैं। वहां से ये कण वाष्पीकरण के बाद बादलों तक पहुंच जाते हैं और फिर बादलों के माध्यम से उन स्थानों तक भी पहुंच गये हैं, जिन्हें अछूता (वर्जिन) क्षेत्र (पहाड़ों, ग्लेशियर) समझा जाता रहा है। यानी यह हमारी भोजन श्रृंखला में शामिल हो गया है।'' उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक "टी-बैग" को गर्म पानी में घोलने के बाद उस चाय की एक बूंद का जब माइक्रोस्कोप में विश्लेषण किया, तो यह बात सामने आयी कि अनगिनत संख्या में माइक्रॉन साइज के प्लास्टिक के कण उस एक बूंद चाय में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चाय के माध्यम से यह सूक्ष्म कण मनुष्य के खून में पहुँच जाते हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘यह हमारे खून में प्लास्टिक के कण भेजने वाला अकेला माध्यम नहीं है'' तथा विभिन्न माध्यम से ये कण मनुष्य के रक्त में पहुंच रहे हैं। डॉ. सोनकर ने कहा कि जो लोग "सिंगल यूज प्लास्टिक" के प्रतिबंधित होने से खुश हो रहे हैं, उन्हें प्लास्टिक की भयावहता के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘समस्या इतनी विकट है कि यह सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से खत्म नहीं हो सकती।'' एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि एक सामान्य व्यक्ति करीब पांच ग्राम प्लास्टिक के कण हर सप्ताह अपने शरीर में पहुँचा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘ये प्लास्टिक हमारे शरीर में जाकर करता क्या है? प्लास्टिक में बिस्फेनाल-ए, बी़.पी.ए., थैलेट्स, ‘परपालीफ्लोरोअल्काइल सब्सटांस' (पीएफएएस) जैसे तमाम जहरीले रसायन होते हैं, जो कैंसर जैसे गम्भीर रोगजनक रसायन हैं।'' उन्होंने बताया, ‘‘प्रयागराज के अपने सूक्ष्म जीव विज्ञान व टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में एक प्रयोग के दौरान मैं अंडमान के समुद्री सीप के ‘मेंटल टिश्यू' का सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) में विश्लेषण कर रहा था, तभी मुझे टिश्यू में कुछ अज्ञात कणों की उपस्थिति दिखी। अध्ययन करने पर पता चला कि वो माइक्रॉन साइज के प्लास्टिक के कण थे। मैं हतप्रभ था कि ये समुद्री सीप के टिश्यू में कहाँ से आया? स्वाभाविक था कि खून से आया होगा, खून में भोजन से आया होगा। मैंने समुद्र के पानी व उसके शैवालों का गहन परीक्षण किया। मुझे पानी व शैवालों के हर नमूने में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मिले। शैवाल या प्लवक, भोजन श्रृंखला में प्रथम पायदान पर है। वहीं से ये समुद्री सीपों के खून में पहुचा। खून में प्लास्टिक के कण पहुँचने की प्रक्रिया में मनुष्य का खून अपवाद नहीं है।" डॉ. सोनकर ने बताया कि उन्होंने जल के हर सम्भव स्रोतों से नमूने लिये और परीक्षण में हर नमूने में प्लास्टिक के कण मिले। प्लास्टिक के गंभीर खतरों के प्रति चौतरफा मुहिम की वकालत करते हुए डॉ. सोनकर ने कहा, ‘‘आज हमारे हर तरफ प्लास्टिक है। घरों के पानी के पाइप, छत पर रखी पानी की टंकी, भोजन के बर्तन, हमारे रसोई में नमक से लेकर लगभग हर खाद्य पदार्थ प्लास्टिक से दूषित है।'' उन्होंने कहा कि ये प्लास्टिक शरीर में जाकर तमाम जैविक क्रियाओं को बाधित कर मनुष्य के लिवर, गुर्दे सहित तमाम अंगों को नष्ट कर रहा है।
- नयी दिल्ली. एक नए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 12 साल तक की उम्र के कम से कम 42 प्रतिशत बच्चे हर दिन औसतन दो से चार घंटे अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से चिपके रहते हैं जबकि इससे अधिक आयु के बच्चे हर दिन 47 फीसदी वक्त मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बिताते हैं। वाईफाई पर चल रहे ‘ट्रैफिक' पर नजर रखने वाले उपकरण ‘हैप्पीनेट्ज' कंपनी द्वारा कराए सर्वेक्षण के अनुसार, जिन घरों में कई उपकरण हैं वहां अभिभावकों के लिए अपने बच्चों के स्क्रीन पर बिताने वाले वक्त को नियंत्रित करना और उन्हें आपत्तिजनक सामग्री देखने से रोकना एक चुनौती है। यह सर्वेक्षण 1,500 अभिभावकों के बीच किया गया जिसमें पाया गया कि 12 साल और उससे अधिक आयु के 69 प्रतिशत बच्चों के पास अपने टैबलेट या स्मार्टफोन हैं जिससे वह इंटरनेट पर बिना किसी रोकटोक के कुछ भी देख सकते हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘...उनमें से 74 प्रतिशत बच्चे यूट्यूब की दुनिया में खो जाते हैं जबकि 12 साल और उससे अधिक आयु के 61 प्रतिशत बच्चे गेमिंग की ओर आकर्षित होते हैं।'' इसमें कहा गया है, ‘‘स्क्रीन पर आधारित मनोरंजन के कारण उनका स्क्रीन पर बिताया वक्त बढ़ जाता है जिससे 12 साल तक की उम्र के 42 प्रतिशत बच्चे हर रोज औसतन दो से चार घंटे स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहते हैं तथा 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे हर दिन 47 प्रतिशत वक्त स्क्रीन पर बिताते हैं।'' हैप्पीनेट्ज की सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋचा सिंह ने कहा, ‘‘जब शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो स्मार्ट उपकरण आज बच्चों के लिए एक सहायक बन गया है। बच्चे अच्छा-खासा वक्त अपने गैजेट्स पर बिताते हैं चाहे वे स्कूल से मिला होमवर्क करना हो, दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ चैट करना हो या पढ़ाई के लिए ऐप का इस्तेमाल करना हो।'' हैप्पीनेट्ज एक ‘पैरंटल कंट्रोल फिल्टर बॉक्स' उपलब्ध कराता है जो 11 करोड़ से अधिक वेबसाइट और ऐप पर नियमित नजर रखता है और उसने 2.2 करोड़ से अधिक आपत्तिजनक वेबसाइट और ऐप को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया है।
-
मंगल ग्रह अतीत में कभी रहने योग्य रहा होगा: वैज्ञानिक
नयी दिल्ली. वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर संभवत: किसी समय में शुष्क और आर्द्र मौसम चक्र रहा होगा और इस प्रकार, यह अपने अतीत में किसी समय रहने योग्य रहा होगा। नासा के ‘क्यूरियोसिटी' रोवर द्वारा मंगल ग्रह की प्रारंभिक सतह पर देखे गए मिट्टी की दरार के पैटर्न का विश्लेषण वहां पानी की अनियमित उपस्थिति की बात कहता है जिसका अर्थ है कि पानी कुछ समय के लिए मौजूद रहा होगा और फिर यह वाष्पित हो गया होगा। फ्रांस, अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में कहा कि मिट्टी में दरारें बनने तक इस प्रक्रिया की पुरावृत्ति हुई होगी। ‘क्यूरियोसिटी' रोवर पर लगे केमकैम उपकरण से संबंधित प्रमुख अन्वेषक और इस अध्ययन के लेखकों में से एक नीना लान्ज़ा ने कहा, "ये मिट्टी की दरारें हमें उस परिवर्ती समय को दिखाती हैं जब तरल पानी कुछ मात्रा में था।" इस प्रकार, ये निष्कर्ष इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि मंगल पर कभी पृथ्वी जैसी आर्द्र जलवायु रही होगी और लाल ग्रह किसी समय रहने योग्य रहा होगा। -
बेंगलुरु. भारत का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन 'चंद्रयान-3' बुधवार को कक्षा घटाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह के और नजदीक आ गया। 'चंद्रयान-3' का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और पांच अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘चंद्रमा की सतह के और नजदीक। आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 174 किमी x 1437 किमी रह गई है।'' इसने कहा कि अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को पूर्वाह्न 11:30 से अपराह्न 12:30 बजे के बीच निर्धारित है। महत्वाकांक्षी मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान-3 की कक्षा को धीरे-धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो द्वारा सिलसिलेवार कवायद की जा रही है।
-
नयी दिल्ली. मोनाश विश्वविद्यालय ने आनुवांशिक मॉडल का इस्तेमाल कर एक अध्ययन किया है, जिसमें पाया गया है कि अपनी गर्भावस्था की शुरुआत में सेब और जड़ी-बूटियों का सेवन करने वाली महिलाएं अपने बच्चों व पोते-पोतियों के मस्तिष्क के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं। यह अध्ययन एक परियोजना का हिस्सा है। अध्ययन में पाया गया कि एक गर्भवती महिला का आहार ना केवल उसके बच्चे के बल्कि उसके पोते-पोतियों के मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। ‘नेचर सेल बायोलॉजी' में प्रकाशित मोनाश बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के अध्ययन में पाया गया कि कुछ खाद्य पदार्थ मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में गिरावट को रोकने में मदद कर सकते हैं। इस अध्ययन में आनुवंशिक मॉडल के रूप में एक तरह के कीड़े ‘राउंडवॉर्म' (कैनोर्हाडाइटिस एलिगेंस) का उपयोग किया गया क्योंकि उनके कई जीन मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, जिससे मानव कोशिकाओं के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है।
अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि सेब और जड़ी-बूटियों जैसे तुलसी, गुलमेंहदी (रोजमेरी), अजवायन और तेजपात में मौजूद एक निश्चित अणु ने मस्तिष्क को ठीक से काम करने में मदद की। वरिष्ठ प्रोफेसर रोजर पोकॉक ने अपनी टीम के साथ मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं पर अध्ययन किया। ये कोशिकाएं एक दूसरे से करीब साढ़े आठ लाख किलोमीटर लंबी एक तरह की केबल से जुड़ी होती हैं जिसे ‘एक्सॉन' कहा जाता है। पोकॉक ने बताया कि किसी समस्या के कारण तंत्रिका कोशिकाएं ‘एक्सॉन' कमजोर हो जाती हैं, तो मस्तिष्क की शिथिलता और ‘न्यूरोडीजेनेरेशन' की समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने एक कमजोर ‘एक्सॉन' वाले आनुवंशिक मॉडल का उपयोग किया जो जानवरों की उम्र बढ़ने के साथ टूट जाते हैं। पोकॉक ने कहा, "हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या आहार में पाए जाने वाले प्राकृतिक उत्पाद इन कोशिकाओं को स्थिर करके टूटने से बचा सकते हैं।” उन्होंने कहा कि हमने अध्ययन में पाया कि सेब और जड़ी-बूटियों का सेवन करने वाली महिलाएं अपने बच्चों व पोते-पोतियों के मस्तिष्क के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं। पोकॉक ने कहा, ‘‘हमने सेब और जड़ी-बूटियों में पाए जाने वाले एक अणु की पहचान की है जो ‘एक्सॉन' को कमजोर होने से बचाता है...उर्सोलिक अम्ल। हमने पाया कि यह अम्ल खास तरह की वसा बनता है जो एक्सॉन को कमजोर होने से बचाता है। यह वसा स्फिंगोलिपिड के रूप में जानी जाती है जो मां की आंत से उसके अंडाणु में पहुंचती है और फिर दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है।
-
नयी दिल्ली. रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप केवल चार पांच मिनट इतनी कड़ी मेहनत वाला काम कर लें जिससे आपको पसीना आ जाए और आप हांफने लगें तो इस मेहनत से आपको कैंसर होने का खतरा 32 प्रतिशत तक कम हो जाता है । एक अध्ययन में यह बात कही गयी है। जामा ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में ऐसे 22000 लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनके शरीर पर विशेष उपकरण लगाये गये और जरूरी आंकड़े जुटाये गये जो कड़ी कसरत नहीं करते हैं। आस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने कैंसर पर नजर रखने के लिए करीब सात सालों तक इस समूह के स्वास्थ्य रिकार्ड का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बीच-बीच में चार या पांच मिनट की कड़ी शारीरिक मेहनत वाली जीवनशैली वाले लोगों में उन लोगों की तुलना में कैंसर का कम खतरा होता है जो ‘कड़ी मेहनत' नहीं करते हैं। पसीना बहा देने वाली चंद मिनट की गतिविधियों में कड़ी मेहनत वाला घरेलू कामकाज, किराने की दुकान से भारी सामान की खरीदारी, बहुत तेज कदमों से चलना, बच्चों के साथ थकाने वाला खेल खेलना आदि शामिल हैं। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि जो वयस्क इस तरह की पसीना बहा देने वाली मेहनत नहीं करते हैं उनमें छाती, कोलोन जैसे अंगों का कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है । इस अध्ययन के लेखक प्रोफेसर इमैन्युअल स्टामैटाकिस ने कहा, हम जानते हैं कि अधेड़ उम्र के लोग नियमित रूप से कसरत नहीं करते हैं जिससे उनमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है लेकिन गतिविधि ट्रैकर जैसे पहनने वाले उपकरणों के आने के बाद हम रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक की जाने वाली मेहनत संबंधी गतिविधियों का प्रभाव देख पाये।'' उन्होंने कहा कि यह देखना बहुत ही शानदार है कि रोजमर्रा की जिंदगी में महज चार या पांच मिनट की कड़ी मेहनत और कैंसर का जोखिम कम होने के बीच संबंध है।
-
नयी दिल्ली. लद्दाख स्थित हिमालयी पार्काचिक ग्लेशियर के पिघलने की गति तेज होने से तीन झीलों का निर्माण हो सकता है जिनकी औसत गहराई 34 से 84 मीटर तक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि संभव है कि ये झील हिमालीय क्षेत्र में बाढ़ लाने का कारण बनें। पार्काचिक ग्लेशियर सुरु नदी घाटी के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है और यह पश्चिमी हिमालय की दक्षिण जन्स्कार श्रृंखला का हिस्सा है। जन्स्कार श्रृंखला हिमालय में अवस्थित है और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। पत्रिका ‘एन्नल्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी' में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर के पिघलने की दर का पता लगाने के लिए 1971 से 2021 के बीच उपग्रह आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसके मुताबिक 1971 से 1999 (28 साल) के मुकाबले 1999 से 2021 (इक्कीस साल) में छह गुना अधिक गति से ग्लेशियर पिघला। अध्ययन के मुताबिक, हिमनदों के पीछे हटने का कारण जलवायु परिवर्तन है, जो ग्लेशियरों की सतह में बदलाव या भूवैज्ञानिक परिवर्तनों का भी कारण बनता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि तेजी से पीछे हटते हिमनद के साथ भू सतह में बदलाव की वजह से झील बन रही हैं और इनका विस्तार हो रहा है जो हिमालय में बाढ़ का कारण बन सकती हैं। ग्लेशियर से झील तब बनती है जब घर्षण से सतह गहरी होती है और वह पिघल जाती है।
अध्ययन के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने तीन स्थानों की पहचान की है जहां पर ग्लेशियर से झील बन सकती है और इनका आकार 43 से 270 हेक्टेयर हो सकता है। - बेंगलुरु. भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और निगाता विश्वविद्यालय, जापान के वैज्ञानिकों ने हिमालय में करीब 60 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जल की खोज की है। समुद्री जल की ये बूंदें खनिज भंडारों के बीच थीं। बेंगलुरु स्थित आईआईएससी ने बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। विज्ञप्ति के अनुसार वहां एकत्र निक्षेपण में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों थे। इसमें कहा गया है कि निक्षेपण के विश्लेषण से टीम को उन संभावित घटनाओं की जानकारी मिली जिनके कारण पृथ्वी के इतिहास में एक बड़ी ऑक्सीजनिकरण की घटना हुई होगी। बयान के अनुसार, वैज्ञानिकों का मानना है कि 70 से 50 करोड़ वर्ष पहले, पृथ्वी बर्फ की मोटी चादरों से ढकी थी। इसमें कहा गया है कि इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई जिससे जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ। आईआईएससी ने कहा कि वैज्ञानिक अब तक, यह ठीक से नहीं समझ पाए हैं कि अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्मों की कमी और पृथ्वी के इतिहास में मौजूद सभी पुराने महासागरों के लुप्त होने की वजह का आपस में क्या संबंध था। उसने कहा कि हिमालय में ऐसी समुद्री चट्टानों का पता चलने से कुछ उत्तर मिल सकते हैं। सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज (सीईएएस), आईआईएससी के शोधार्थी और 'प्रीकैम्ब्रियन रिसर्च' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के पहले लेखक प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा, ‘‘ हम पुराने महासागरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। वे वर्तमान महासागरों की तुलना में कितने अलग या समान थे? क्या वे अधिक अम्लीय या क्षारीय, पोषक तत्वों से भरपूर, गर्म या ठंडे थे, उनकी रासायनिक और समस्थानिक संरचना क्या थी?" उन्होंने कहा कि इस तरह के विश्लेषण से पृथ्वी पर प्राचीन जलवायु के बारे में जानकारी मिल सकती है।
- नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 38 फीसदी लोग गैर-अल्कोहलिक वसायुक्त यकृत (फैटी लीवर) की बीमारी से पीड़ित हैं। यानी यह बीमारी उन लोगों को होती है जो मदिरा का उपयोग नहीं करते या न के बराबर करते हैं। यह बीमारी केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे करीब 35 फीसदी बच्चे भी प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट में भारत में गैर-अल्कोहलिक ‘फैटी लीवर' रोग पर प्रकाशित विभिन्न रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन रिपोर्ट जून, 2022 में ‘जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी' में प्रकाशित हुई। गैर-अल्कोहलिक वसायुक्त यकृत रोग (एनएएफएलडी) अकसर पकड़ में नहीं आता क्योंकि शुरुआती चरण में इसके लक्षण नहीं दिखते, लेकिन कुछ मरीजों में यह यकृत के गंभीर रोग के रूप में दिख सकता है। उदर रोग विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. अनूप सराया ने कहा, ‘‘वसायुक्त यकृत या ‘स्टीटोहेपेटाइटिस' का कारण हमारे आहार का हालिया पश्चिमीकरण है जिसमें फास्ट फूड का बढ़ता सेवन, स्वास्थ्यवर्धक फलों और सब्जियों का कम सेवन और एक अस्वास्थ्यकर तथा गतिहीन जीवन शैली शामिल है।'' उन्होंने कहा कि ‘फैटी लीवर' के उपचार के लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित दवा नहीं है, लेकिन बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सराया ने कहा, ‘‘इस बीमारी को हराने का केवल एक तरीका है कि हम स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली अपनाएं और मोटापे से पीड़ित लोगों को पर्याप्त आहार मुहैया कराते हुए उनका वजन घटाएं।'' विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में वसायुक्त यकृत का एक आम कारण मदिरा का सेवन है। डॉ. सराया ने कहा, ‘‘यकृत की गंभीर क्षति के अधिकतर मामले शराब के कारण होते हैं। 'एक्यूट क्रॉनिक लीवर फेल्योर' के ऐसे मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है, तो इनमें मृत्यु दर अधिक होती है।'' उन्होंने कहा कि जो चीज इस मामले को बदतर बनाती है, वह है इस बीमारी से ठीक हुए रोगियों के दोबारा इस बीमारी से पीड़ित होने की उच्च दर। उन्होंने कहा कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। सराया ने कहा कि इस घातक बीमारी से बचने का एकमात्र तरीका शराब के सेवन से बचना है क्योंकि कोई भी शराब यकृत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तपेदिक के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, एंटीबॉयोटिक, एंटीपाइलेप्टिक दवाओं और कीमोथेरेपी से भी यकृत को नुकसान पहुंचता है। तपेदिक रोधी दवा से संबंधित ‘तीव्र यकृत विफलता' वाले रोगियों में 67 प्रतिशत की मौत हो जाती है।
-
नयी दिल्ली. बिग-बैंग के बाद नवजात ब्रह्मांड आज के मुकाबले पांच गुना धीमा था। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। इस अध्ययन में आइंस्टीन की ब्रह्मांड के विस्तारित होने की पहेली को सुलझा लेने का दावा भी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय में कार्यरत और अध्ययन के प्रमुख लेखक के. गेरेंट लुईस ने कहा, ‘‘उस समय पर नजर डालें जब ब्रह्मांड सिर्फ एक अरब वर्ष से अधिक पुराना था, तो हमें समय पांच गुना धीमी गति से गुजरता दिखाई देता है।'' आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु को जितना अधिक दूरी से देखा जाता है, जैसे कि एक पुरातन ब्रह्मांड, वह वर्तमान दिन के मुकाबले धीमी गति से चलता है। दो दशकों में प्रारंभिक आकाशगंगाओं के केंद्रों पर 190 क्वासर या अतिसक्रिय विशाल ब्लैक होल के विवरण की जांच करते हुए खगोलविदों ने समय पटल को वर्तमान चरण के दसवें हिस्से तक पीछे किया और पुष्टि की कि ब्रह्मांड उम्र बढ़ने के साथ-साथ तेज होता जा रहा है। यह अध्ययन ‘नेचर एस्ट्रोनॉमी' नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में आइंस्टीन को यह बताने के लिए धन्यवाद दिया गया है कि समय और ‘स्पेस' आपस में जुड़े हुए हैं और बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। -
नयी दिल्ली. आर्कटिक महासागर अनुमान से लगभग दस साल पहले ही यानी 2030 के दशक तक समुद्री बर्फ से मुक्त पहली गर्मी का सामना कर सकता है। ‘नेचर कम्युनिकेशन्स' पत्रिका में प्रकाशित एक नये अनुसंधान में यह दावा किया गया है। इससे आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी बढ़ेगी, समुद्री गतिविधियों में बदलाव आएगा और आर्कटिक कार्बन चक्र प्रभावित होगा, जिससे आर्कटिक क्षेत्र और उसके बाहर, दोनों ही जगहों पर मानव समाज तथा परिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा। दक्षिण कोरिया, कनाडा और जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन परिदृश्य से इतर आर्कटिक महासागर में बर्फ रहित पहली गर्मी पूर्व में लगाए गए अनुमान से एक दशक पहले ही देखने को मिल सकती है। अनुसंधान में कहा गया है कि आर्कटिक महासागर में बर्फ का दायरा हाल के दशकों में लगातार पूरे साल सिकुड़ता जा रहा है। जबकि, इस महासागर में साल की अलग-अलग अवधि में बर्फ का दायरा घटता या बढ़ता है। सर्दियों में आर्कटिक महासागर में अतिरिक्त बर्फ जमने से बर्फ का दायरा बढ़ जाता है, जो मार्च में उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। वहीं, गर्मियों में बर्फ पिघलने के कारण सितंबर में इस महासागर में बर्फ का दायरा न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। अनुसंधान में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि, आर्कटिक क्रायोस्फीयर में मानव गतिविधियों में इजाफे और 1980 के दशक में अल चिचोन ज्वालामुखीय विस्फोट के बाद एयरोसोल के उत्सर्जन में कमी को आर्कटिक में पूरे साल बर्फ पिघलने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अनुसंधान के दौरान, अनुसंधानकर्ताओं ने उपग्रह डेटा और उन्नत जलवायु मॉडल के अध्ययन के अलावा 1979 से 2019 के बीच आर्कटिक महासागर में हर महीने बर्फ के दायरे में आने वाले बदलावों का विश्लेषण किया। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा, “हमारा आकलन संकेत देता है कि आर्कटिक महासागर अगले एक या दो दशक में पहली बार बर्फ रहित गर्मी का गवाह बन सकता है, वो भी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में होने वाले बदलावों के इतर।” उन्होंने आगाह किया, “इससे आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी बढ़ेगी, समुद्री गतिविधियों में बदलाव आएगा और आर्कटिक कार्बन चक्र प्रभावित होग, जिससे आर्कटिक क्षेत्र और उसके बाहर, दोनों ही जगहों पर मानव समाज तथा परिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा।”
-
नयी दिल्ली. अस्वास्थ्यकर आहार का सेवन करने से गहरी नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। यह बात एक अध्ययन में कही गई है। गहरी नींद यानी नींद का तीसरा चरण स्मृति, मांसपेशियों की वृद्धि और प्रतिरक्षा जैसी आवश्यक चीजों को दुरुस्त और पुनर्स्थापित करता है। स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने यह विश्लेषण किया कि नींद को ‘जंक फूड' कैसे प्रभावित करता है। अध्ययन में शामिल स्वस्थ लोगों ने अनियमित क्रम में अस्वास्थ्यकर और स्वास्थ्यकर आहार का सेवन किया। अध्ययन रिपोर्ट हाल में ‘ओबेसिटी' पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसमें कहा गया कि जंक फूड खाने के बाद प्रतिभागियों की गहरी नींद की गुणवत्ता खराब हो गई, जबकि स्वास्थ्यकर आहार के सेवन के बाद ऐसा नहीं हुआ। उप्साला विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर जोनाथन सेडर्नैस ने कहा, "खराब आहार और खराब नींद दोनों से ही स्वास्थ्य के लिए जोखिम को बढ़ता है।" अध्ययन के दो सत्रों में सामान्य वजन वाले कुल 15 स्वस्थ युवकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को बेतरतीब ढंग से स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर आहार दिया गया। दोनों आहारों में कैलोरी की मात्रा समान रखी गई।
-
-मदर्स डे 14 मई पर विशेष
हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व भर में मदर्स डे मनाया जाता है. मां को समर्पित ये दिन इस बार 14 मई को मनाया जाएगा. आखिरकार मां ही वो इंसान है, जो जन्म देने से लेकर हर सुख-दुख में अपने बच्चे के साथ हमेशा खड़ी रहती है. इसी वजह से मां की अहमियत को शब्दों में बयां कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है.
वैसे तो किसी एक दिन को मां के नाम समर्पित करना, किसी के लिए भी काफी नहीं होता है. इसके बावजूद मां के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. तो आइए मदर्स डे के इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि आखिर मातृत्व दिवस मनाने के पीछे की वजह क्या है और इसको कब से मनाया जा रहा है.
मदर्स डे का इतिहास
मातृत्व दिवस मनाने की शुरुआत अमेरिकन महिला एना जॉर्विस ने की थी. एना जॉर्विस ने मदर्स डे की नींव रखी, लेकिन मदर्स डे को मनाने की शुरुआत औपचारिक रूप से 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने की थी. उस समय अमेरिकी संसद में कानून पास करके हर साल मई महीने के दूसरे संडे को मदर्स डे मनाने का फैसला लिया गया. तब से अमेरिका, यूरोप और भारत सहित कई देशों में मदर्स डे धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा.
मदर्स डे मनाने का उद्देश्य
अमेरिकन महिला एना जॉर्विस को अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार और लगाव था. एना अपनी मदर से बहुत इंस्पायर हुआ करतीं थीं और उन्होंने अपनी मां की मृत्यु के बाद शादी न करने का फैसला लिया था. एना ने अपना सारा जीवन अपनी मदर के नाम करने का संकल्प लिया और अपनी मां को सम्मान देने के उद्देश्य से मदर्स डे की शुरूआत की. इसके लिए एना ने इस तरह की तारीख चुनी कि वह उनकी मां की पुण्यतिथि 9 मई के आस-पास ही पड़े. यूरोप में इस दिन को मदरिंग संडे कहा जाता है, तो वहीं ईसाई समुदाय से जुड़े बहुत लोग इस दिन को वर्जिन मेरी के नाम से भी पुकारते हैं.
मदर्स डे का महत्व
वैसे तो हर कोई अपनी मां के महत्त्व को अच्छी तरीके से समझता है. लेकिन इस बात का अहसास मां को नहीं करवा पाता है. ऐसे में मां को उनकी अहमियत का अहसास करवाने और उनको स्पेशल फील करवाने के लिए मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है. भारत में हर कोई इस दिन को अपने अलग अंदाज में मनाने की कोशिश करता है. कुछ लोग मां को उनका फेवरेट तोहफा या ग्रीटिंग्स देकर मदर्स डे विश करते हैं. तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन मां को घर के कामों से छुट्टी देकर बाहर घुमाने भी ले जाते हैं. सोशल मीडिया पर भी मदर्स डे के सम्बन्ध में कई सारे कोट्स शेयर किए जाते हैं. -
नयी दिल्ली. मादक पदार्थ दुरुपयोग की समस्या अगले दशक में विकराल रूप ले सकती है और विशेष रूप से 10 से 17 साल की आयु के बच्चों को प्रभावित कर सकती है। एक अध्ययन के बुधवार को जारी प्राथमिक निष्कर्षों में यह बात सामने आई। स्वतंत्र थिंकटैंक ‘थिंक चेंज फोरम' के अध्ययन में सामने आया कि मानसिक सेहत से जुड़े मुद्दे, कामकाज का दबाव, बढ़ता खालीपन और बदलती सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का इस आयु वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है और ये नशे की लत की ओर बढ़ने लगते हैं। अध्ययन के अनुसार मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग का प्रभाव भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में होगा। भारत में कोरोना वायरस महामारी के बाद ऐसे पदार्थों की विशेष रूप से युवाओं और किशोरों में खपत चिंताजनक तरीके से बढ़ी है और इसके मद्देनजर ‘थिंक चेंज फोरम' ने इस तरह की लत की समस्या का विश्लेषण कर इसके समाधानों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों के परामर्श पर आधारित राष्ट्रीय अध्ययन शुरू किया है। प्रारंभिक नतीजों में तीन महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की ओर इशारा किया गया है जिनसे किशोरों और युवाओं के बीच नशीले पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है और इन्हें तत्काल कम करने के लिए तीन महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जरूरी बताये गये हैं। अध्ययन के अनुसार नशीले पदार्थों को लेकर चमक-दमक का माहौल भारत में इनका उपयोग बढ़ने की पहली अहम प्रवृत्ति है। टेडेक्स वक्ता और अभिभावकों को परामर्श देने वाले सुशांत कालरा ने कहा, ‘‘आज फिल्मी नायक, नायिकाएं नशे को चमक-दमक के साथ दिखाते हैं। बच्चे और किशोर अपने पसंदीदा अदाकारों को फिल्मों और वीडियो सीरीज समेत विभिन्न मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त देखते हैं। इस तरह का संदेश दिया जाता है कि ये गतिविधियां न केवल स्वीकार्य हैं बल्कि अत्यंत अपेक्षित हैं।'' अध्ययन के अनुसार दूसरी प्रवृत्ति ई-सिगरेट और ऐसे उत्पादों के उपयोग की है। तीसरी प्रवृत्ति कामकाज के बढ़ते दबाव और बढ़ते खालीपन के कारण मानसिक सेहत संबंधी मुद्दों से जुड़ी है। विशेषज्ञों ने इनकी रोकथाम के लिए तीन हस्तक्षेपों में संबंधित मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने को गिनाया है। बच्चों को यह बताने की भी आवश्यकता भी रेखांकित की गयी है कि ई-सिगरेट तंबाकू से बेहतर विकल्प नहीं है और इस तरह के उपकरण से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप अभिभावकों और प्रशिक्षकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस तरह के नशों के खिलाफ शिक्षा के प्रसार का है।
-
आपके फोन के बारे में गंदा सच ...!
बाथरूम में इसका इस्तेमाल बंद करने की आवश्यकता
लीसेस्टर. हम उसे हर जगह अपने साथ ले जाते हैं, उसे बिस्तर पर ले जाते हैं, बाथरूम में ले जाते हैं और कई लोगों के लिए वह पहली चीज हैं, जिसे वह सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले देखते हैं - दुनिया के 90 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास मोबाइल फोन है या वह इसका उपयोग करते हैं और हम में से कई इसके बिना रह नहीं सकते। फोन के उपयोग के बारे में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं अकसर ध्यान केंद्रित करती हैं कि वे ड्राइविंग करते समय ध्यान भटका सकते हैं, रेडियोफ्रीक्वेंसी एक्सपोजर के संभावित प्रभाव, या उनकी लत लगने जैसी चिंताएं। आपके फोन के माइक्रोबियल संक्रमण जोखिम की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है - लेकिन यह बहुत वास्तविक है। 2019 के एक सर्वे में पाया गया कि यूके में ज्यादातर लोग अपने फोन का इस्तेमाल टॉयलेट में करते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अध्ययन में पाया गया है कि हमारे मोबाइल फोन टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदे होते हैं। हम अपने फोन बच्चों को खेलने के लिए देते हैं (जो अपनी साफ-सफाई का ध्यान ठीक से नहीं रख पाते हैं)। हम अपने फोन का उपयोग करते समय खाते भी हैं और उन्हें हर तरह की (गंदी) सतहों पर रख देते हैं। इससे आपके फोन पर रोगाणु तो जमा होते ही हैं उन्हें खाने के लिए भोजन भी मिलता रहता है। यह अनुमान लगाया गया है कि लोग दिन में हजारों बार नहीं तो सैकड़ों बार अपने फोन को छूते हैं। और जबकि हम में से कई लोग बाथरूम जाने, खाना पकाने, सफाई करने, या बागवानी करने के बाद नियमित रूप से अपने हाथ धोते हैं, लेकिन हम अपने फोन को छूने के बाद अपने हाथों को धोने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। लेकिन यह देखते हुए कि फोन कितने गंदे और कीटाणुयुक्त हो सकते हैं, शायद यह समय मोबाइल फोन की स्वच्छता के बारे में अधिक सोचने का है।
कीटाणु, जीवाणु, विषाणु--
हाथ हर समय बैक्टीरिया और वायरस उठाते हैं और संक्रमण प्राप्त करने के मार्ग के रूप में पहचाने जाते हैं। इसी प्रकार हम जिन फ़ोनों को छूते हैं वह भी रोगाणु के वाहक ही हैं। मोबाइल फोन के सूक्ष्मजीवविज्ञानी उपनिवेशण पर किए गए कई अध्ययनों से पता चलता है कि वे कई अलग-अलग प्रकार के संभावित रोगजनक बैक्टीरिया से दूषित हो सकते हैं। इनमें डायरिया पैदा करने वाले ई. कोलाई (जो वैसे, मानव मल से आते हैं) और त्वचा को संक्रमित करने वाले स्टैफिलोकोकस, साथ ही एक्टिनो बैक्टीरिया शामिल हैं, जो तपेदिक और डिप्थीरिया, सिट्रोबैक्टर का कारण बन सकते हैं, जो दर्दनाक मूत्र पथ के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। और एंटरोकोकस, जो मेनिनजाइटिस का कारण बनता है। क्लेबसिएला, माइक्रोकोकस, प्रोटियस, स्यूडोमोनास और स्ट्रेप्टोकोकस भी फोन पर पाए गए हैं और सभी मनुष्यों पर समान रूप से बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। शोध में पाया गया है कि फोन पर कई रोगजनक अक्सर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी होते हैं, जिसका अर्थ है कि पारंपरिक दवाओं के साथ उनका इलाज नहीं किया जा सकता है। यह चिंताजनक है क्योंकि ये बैक्टीरिया त्वचा, आंत और श्वसन संक्रमण का कारण बन सकते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। शोध में यह भी पाया गया है कि भले ही आप अपने फोन को एंटीबैक्टीरियल वाइप्स या अल्कोहल से साफ करते हैं, फिर भी यह सूक्ष्मजीवों से अटा रहता है, यह दर्शाता है कि स्वच्छता एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए। फोन में प्लास्टिक होता है जो वायरस को शरण दे सकता है और प्रसारित कर सकता है, जिनमें से कुछ (सामान्य कोल्ड वायरस) प्लास्टिक की कठोर सतहों पर एक सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। अन्य वायरस जैसे कि कोविड-19, रोटावायरस (एक अत्यधिक संक्रामक पेट का बग जो आमतौर पर शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करता है), इन्फ्लूएंजा और नोरोवायरस - जो गंभीर श्वसन और आंतों के संक्रमण का कारण बन सकता है - कई दिनों तक संक्रामक रूप में बना रह सकता है। वास्तव में, कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मोबाइल फोन की सफाई और कीटाणुशोधन के लिए दिशानिर्देश पेश किए हैं - जो दरवाज़े के हैंडल, कैश मशीन और लिफ्ट बटन की तरह ही संक्रमण के भंडार माने जाते हैं। विशेष रूप से, इस भूमिका के बारे में चिंता व्यक्त की गई है कि मोबाइल फोन अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ स्कूलों में संक्रामक रोगाणुओं के प्रसार में भूमिका निभा सकते हैं।
अपना फ़ोन साफ़ करें--
यह स्पष्ट है कि आपको अपने फोन को नियमित रूप से साफ करना शुरू करना होगा। यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन वास्तव में आपके फोन और अन्य उपकरणों की दैनिक स्वच्छता की सिफारिश करता है - इससे कम नहीं क्योंकि हम अभी भी एक सक्रिय कोविड-19 महामारी के भीतर हैं और वायरस कठोर प्लास्टिक सतहों पर कई दिनों तक जीवित रह सकता है। फोन के केसिंग और टच स्क्रीन को कीटाणुरहित करने के लिए अल्कोहल-आधारित वाइप्स या स्प्रे का उपयोग करें। उनमें कम से कम 70% अल्कोहल होना चाहिए, और यदि संभव हो तो इसे हर दिन किया जाना चाहिए। सीधे फ़ोन पर सैनिटाइज़र का छिड़काव न करें और तरल पदार्थों को कनेक्शन बिंदुओं या फ़ोन के अन्य खुले स्थानों से दूर रखें। ब्लीच या अपघर्षक क्लीनर के उपयोग से बिल्कुल बचें। और सफाई पूरी करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। आप अपने फोन को कैसे रखते हैं, इसके बारे में सोचने से भी कीटाणुओं से बचने में मदद मिलेगी। जब आप घर पर न हों, तो अपने फ़ोन को अपनी जेब या बैग में रखें और लगातार अपने फ़ोन को देखते रहने की आदत छोड़ दें।
अपने फ़ोन को साफ़ हाथों से स्पर्श करें -
साबुन और पानी से धोएँ या अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र से कीटाणुरहित करें। अपने फोन को वायरस का स्रोत बनने से बचाने के लिए आप और भी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कोई संक्रमण है, या पहले इसे साफ नहीं किया है, तो अपना फोन दूसरों के साथ साझा न करें। यदि बच्चों को खेलने के लिए अपना फोन देते हैं तो देने से पहले इसे साफ कर लें। और जब उपयोग में न हो तो फोन को दूर रखने की आदत डाल लें, फिर अपने हाथों को सेनेटाइज करें या धो लें। जब आप अपना फ़ोन साफ़ कर रहे हों तो कभी-कभी अपने फ़ोन चार्जर को भी साफ़ करते रहे। -
लोवेल. किंवदंती है कि प्रत्येक इंद्रधनुष के अंत में सोने का एक घड़ा छिपा होता है। लेकिन क्या वास्तव में एक इंद्रधनुष का "अंत" होता है, और क्या कभी यह हमें मिल सकता है? हम में से अधिकांश लोग आकाश में इंद्रधनुष को रंगों के मेहराब के रूप में देखते हुए जीवन गुजारते हैं, लेकिन यह वास्तव में रंगों का एक चक्र है, इसका केवल आधा हिस्सा हम देख पाते हैं। आम तौर पर, जब आप एक इंद्रधनुष को देखते हैं, तो आपके सामने पृथ्वी का क्षितिज वृत्त के निचले आधे हिस्से को छुपा देता है। लेकिन अगर आप एक पहाड़ पर खड़े हैं जहां आप अपने ऊपर और नीचे दोनों देख सकते हैं, और सूरज आपके पीछे है और धुंध है या अभी बारिश हुई है, तो संभावना अच्छी है कि आप इंद्रधनुष के घेरे को और बड़ा देखेंगे। हालांकि, पूरे घेरे को देखने के लिए, आपको बादलों के ठीक ऊपर एक हवाई जहाज में जाना होगा। या आप अपना खुद का इंद्रधनुष बना सकते हैं। मैं एक भौतिक विज्ञानी हूं, और मैं इसे एक मिनट में समझाऊंगा। इंद्रधनुष कैसे बनता है
इंद्रधनुष तब बनते हैं जब आपके पीछे से सूरज की रोशनी आपके सामने पानी की लाखों छोटी-छोटी गोल बूंदों से टकराती है और आपकी आंखों पर वापस आती है। जैसे सूरज की किरण किसी छोटी बूंद पर एक कोण से टकराती है, वह पानी में झुक जाती है और रंगों के स्पेक्ट्रम में अलग हो जाती है। वैज्ञानिक प्रकाश के मुड़ने को "अपवर्तक" कहते हैं। रंग अलग हो जाते हैं क्योंकि प्रकाश का प्रत्येक "रंग" पानी में एक अलग गति से यात्रा करता है, या उस स्थिति में, कोई भी पारदर्शी सामग्री जिसके माध्यम से प्रकाश यात्रा कर सकता है, जैसे प्रिज्म में कांच। जब रंग पानी की बूंद की पिछली दीवार से टकराते हैं, तो कोण अब इतना उथला हो जाता है कि वे हवा में बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए वे पानी की बूंद में वापस परावर्तित होते हैं और इसकी प्रवेश दीवार पर लौट आते हैं। वहां से, रंग फिर से हवा में मुड़ सकते हैं और आपकी आंखों तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप इन बूंदों को देखते हैं, अलग-अलग रंग थोड़े अलग कोण पर एकत्रित होते हैं, और प्रत्येक रंग एक शंकु के गोलाकार रिम का निर्माण करता है, जिसमें आपकी आंख शंकु की नोक पर होती है। और ये लीजिए, आपके पास अपना निजी इंद्रधनुष है। आपकी आंखों में रंग भेजने वाली बूंदें उन्हें किसी और को नहीं भेज सकती हैं, भले ही आपके आस-पास के सभी लोग एक ही इंद्रधनुष को देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में अपने स्वयं के थोड़े अलग इंद्रधनुष को देखता है। यह सब देखने वाले की नजर में है। इंद्रधनुष बनने के लिए, पानी की बूंदों का आकार एक गोले के बहुत करीब होना चाहिए ताकि वे सभी मुड़ सकें और रंगों को प्रतिबिंबित कर सकें। यह बहुत छोटी बूंदों के लिए होता है, जैसे कि महीन धुंध, या बारिश की फुहार के ठीक बाद जब हवा सिर्फ नम होती है। जैसे-जैसे बूंदें बड़ी होती जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण उनके आकार को विकृत करता जाता है और इंद्रधनुष गायब हो जाता है। एक इंद्रधनुष भौतिक रूप से वहां मौजूद नहीं होता है जहां यह दिखाई देता है, जैसे कि दर्पण में आपकी छवि। इसलिए, मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप वास्तव में कभी भी अपने इंद्रधनुष तक नहीं पहुंच सकते। और, अफसोस, कोई भी उस सोने के बर्तन को कभी नहीं ढूंढ़ पाएगा। लेकिन आप अपना खुद का इंद्रधनुष बना सकते हैं।
गोलाकार इन्द्रधनुष कैसे बनाएं और देखें
एक प्रयोग जो आप गर्मियों में आजमा सकते हैं, आप पानी का छिड़काव करने वाले किसी पंप को पानी की बहुत महीन बूंदों की फुहार करने की सेटिंग पर रखें। याद रहे कि आपके पीछे सूरज हो। यदि आप अपने सामने फुहार की एक परत बनाते हैं और अपनी छाया को देखते हैं, तो आपको इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। रंगों को देखना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक पूरा चक्र देखने के लिए आपको वैज्ञानिकों की तरह थोड़े धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होगी। तो अगली बार जब आप हवाई जहाज में हों तो खिड़की वाली सीट पकड़ लें। यदि आप बादलों के आवरण से थोड़ा ऊपर उड़ रहे हैं, तो बादलों पर अपने विमान की छोटी छाया की तलाश करें। इसका मतलब है कि सूरज आपके पीछे है। बादल पानी की छोटी-छोटी बूंदें हैं, इसलिए संभावना है कि आप हवाई जहाज की छाया के चारों ओर रंग का एक छोटा सा घेरा देख सकते हैं। और अगर आप वास्तव में यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि यह कैसा दिखता है, तो इंटरनेट हमेशा मौजूद है।







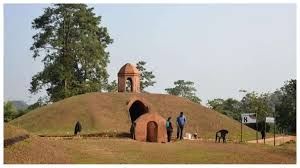
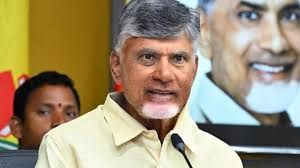
.jpeg)
.jpeg)



.jpg)



.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)



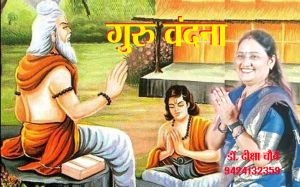
.jpg)

.jpeg)


.jpg)
.jpg)





.jpg)



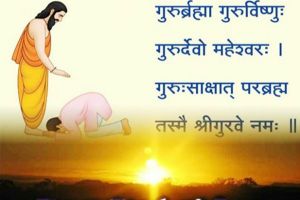








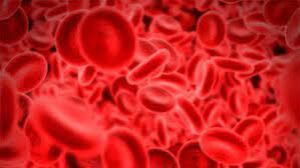





.jpeg)

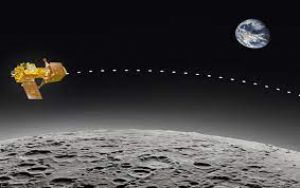



.jpeg)
.jpeg)








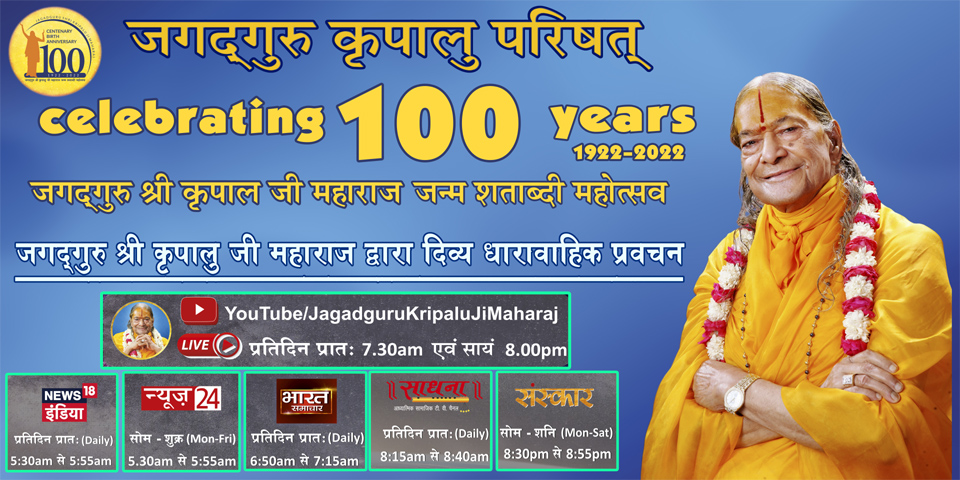

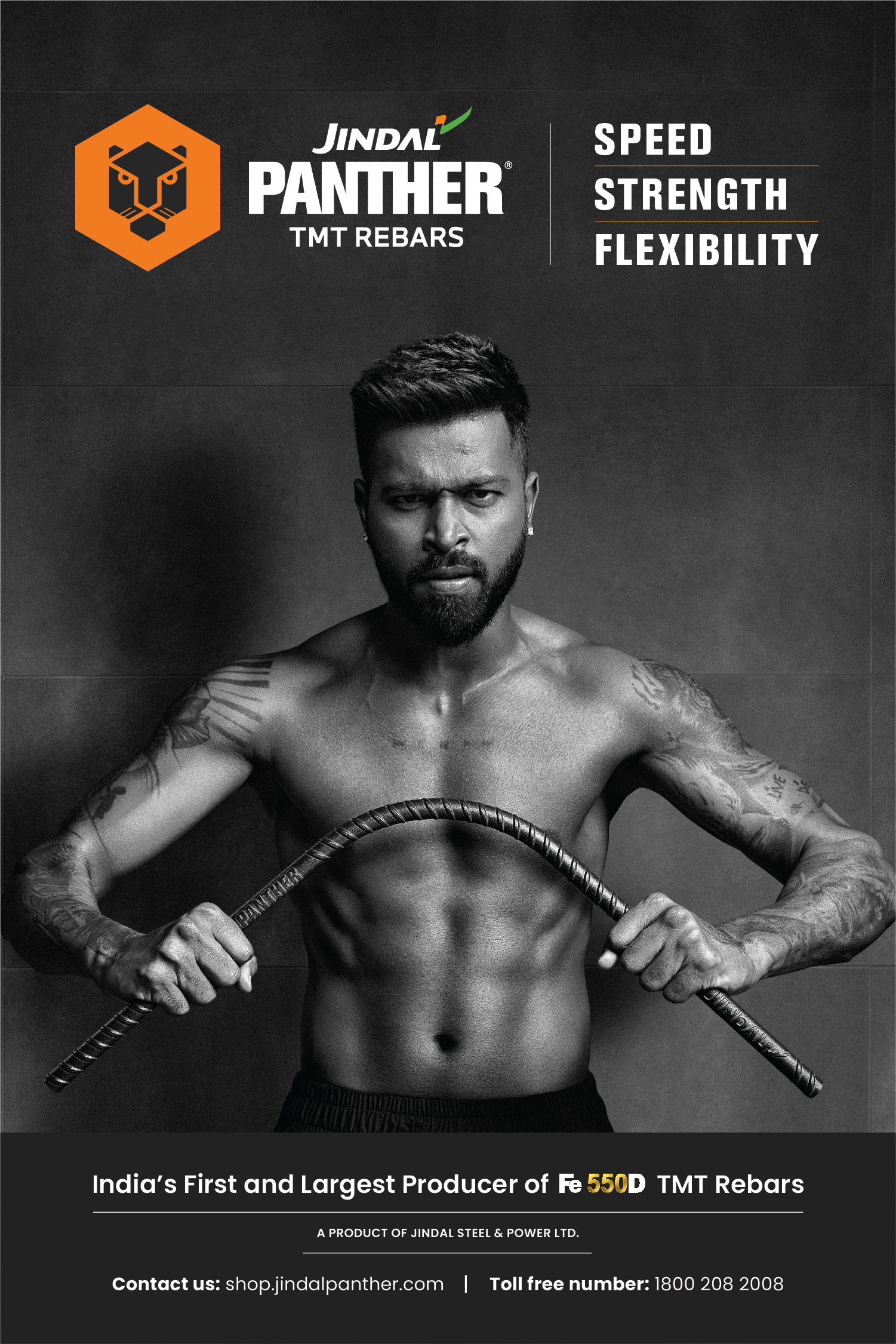
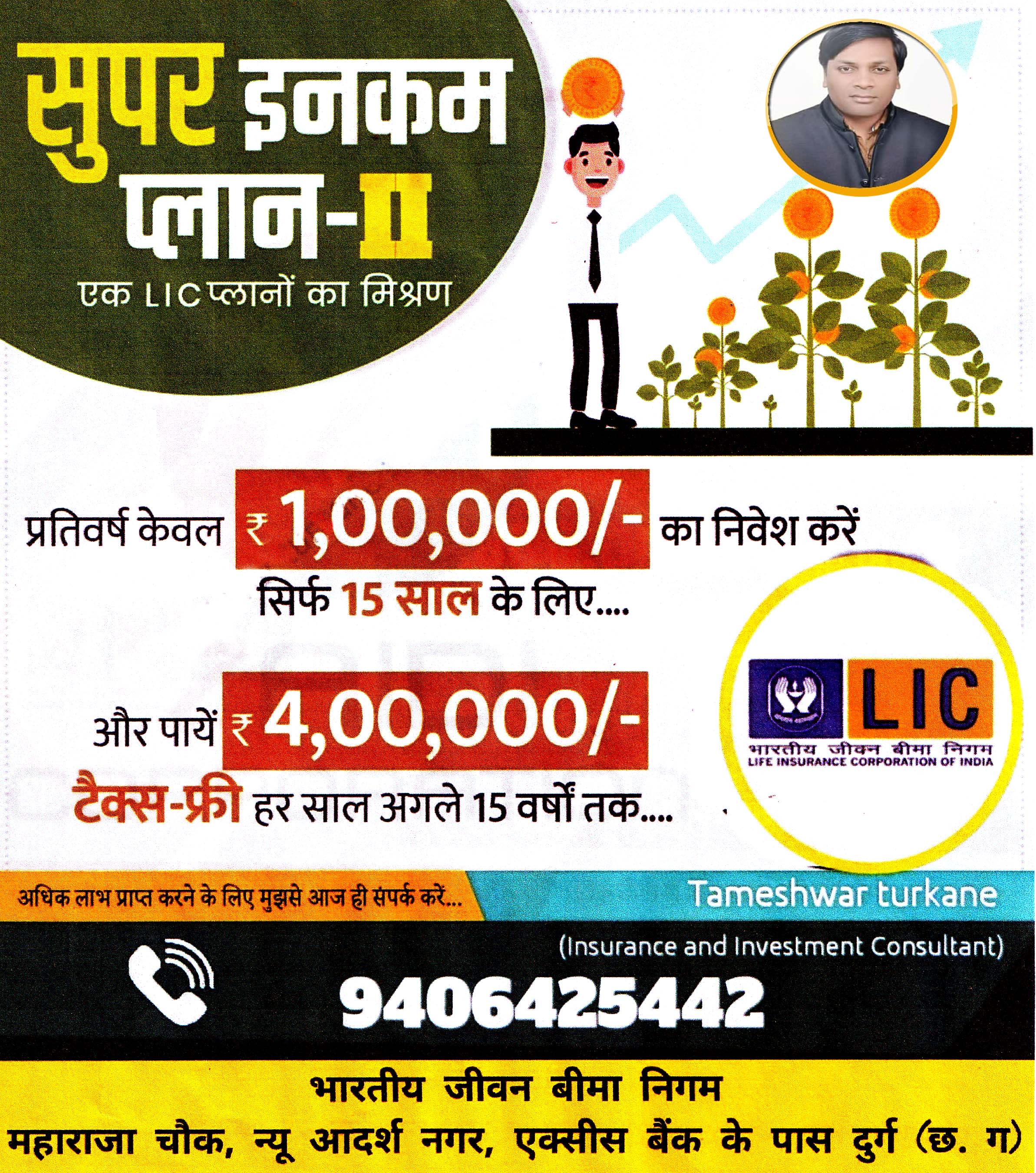
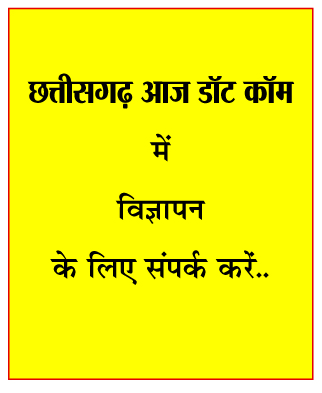
.jpg)
.jpg)