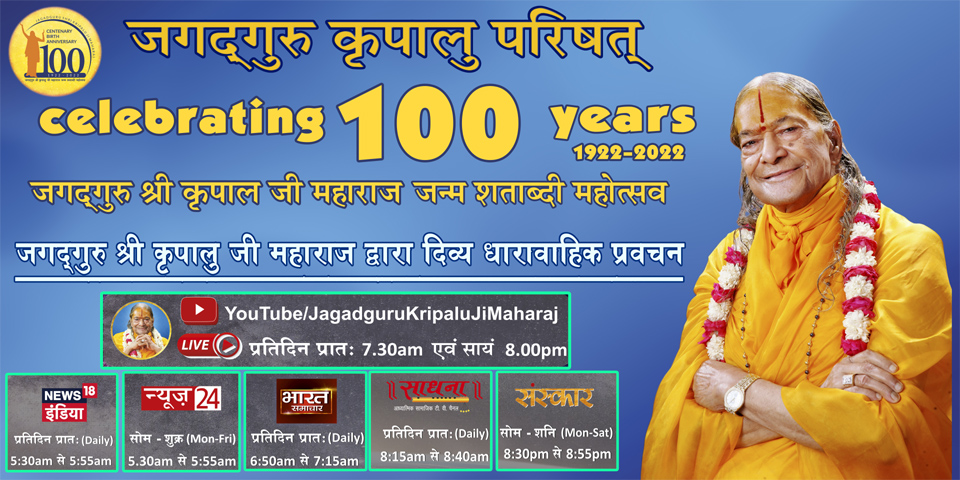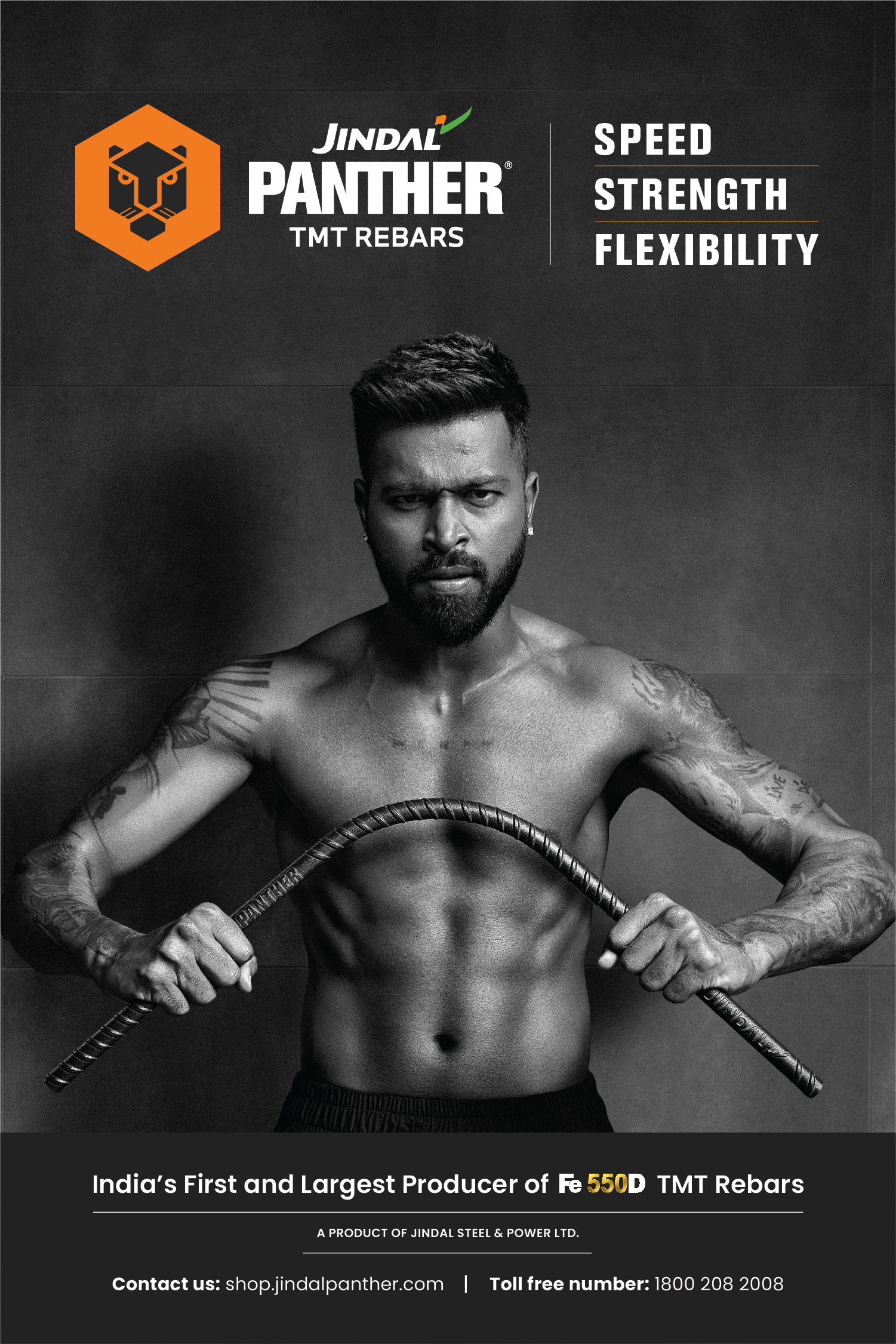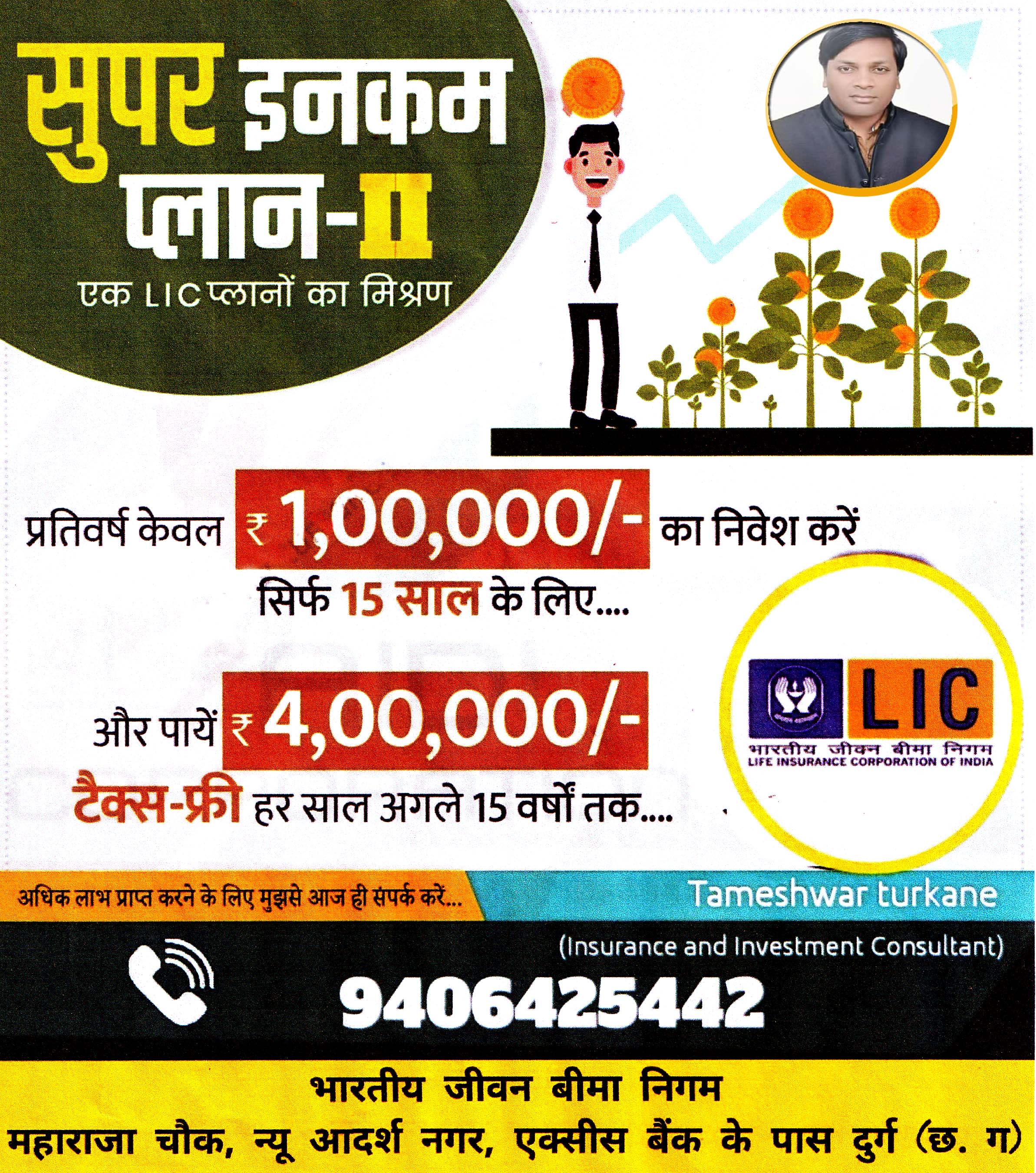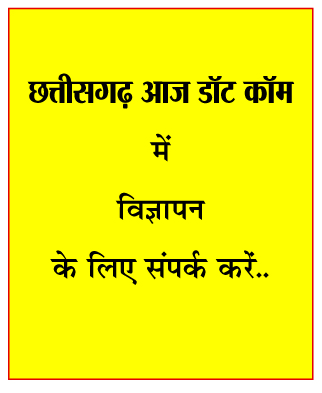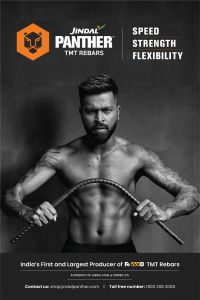- Home
- आलेख
- -लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)मात सम नहीं पावन दूजा ।माँ की सब करते हैं पूजा ।।माँ बिन घर सूना हो जाता ।माँ से घर में सब सुख आता ।।माँ सब कुछ संभव कर जाती ।माँ से ही सब खुशियाँ आती ।।माँ निज सुत पर वारी जाती ।चाहत उसकी मारी जाती ।।निज दुख सबसे मात छुपाती ।मन की बात दबी रह जाती ।।गाँठ यही तन- मन को खाती ।पीर हृदय का रोग लगाती ।।आदर ममता देना सीखो ।माँ की पीड़ा हरना सीखो ।।जीवनपथ में साथ निभाना ।चाहत पूरी करते जाना ।।मंदिर की मूरत के जैसी ।माँ होती है पावन वैसी ।।पूजन व्रत सब उनसे होते ।देव-मनुज पद उनके धोते ।।
- -लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)स्कूल का वह प्रांगण सुहाना।यादों का अनमोल खजाना।।खेल पढ़ाई सखी सहेली,ख्वाबों में सितारे सजाना।।प्रथम बेंच से अंतिम कोना,रहस्यों की लड़ियाँ पिरोना।अंतिम पन्ना बना डाकिया,लिख-लिख करते रोना-धोना।बीच पढ़ाई चुपके-चुपके,मित्रों की उलझन सुलझाना।।यादों का अनमोल खजाना।।शशि मैडम की सुंदर आँखें,चंचल मन को देतीं पाँखें।अँकुराते थे सपन-सलोने,फली बढ़ी यौवन की शाखें।।सुखद कल्पनाओं ने सीखा,उम्मीदों के पंख लगाना।।यादों का अनमोल खजाना।।आगे बढ़ने की अभिलाषा,पढ़े मित्रता की परिभाषा।झूठ-मूठ की रूठारूठी,मौन मुखर जीवन प्रत्याशा।चाक श्यामपट की लिखावटें,जैसी कड़वाहटें मिटाना।।यादों का अनमोल खजाना।।---शासकीय कन्या स्कूल बेमेतरा, बैच-1988 से 2003.... वो दिन भी क्या दिन थे...
- -लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)स्वर्ण मृगा मन को भटकाए, समझा देना यह है छल।जब भी मैं कमजोर पड़ूँ प्रिय, बन जाना मेरा संबल।हृदय सुकोमल करुण भावना,दिशा भ्रमित होतीं आँखें।मन में सोयी दबी चाहतें, फैला देती हैं पाँखें।कभी-कभी संयम खो देता,चितवन है थोड़ी चंचल ।।जब भी मैं….पक्षपात से दुखता है मन, अन्याय साथ में हो जब।बेलगाम हो जाती रसना, उगल पड़े कड़ुवाहट तब।कलुषित सोच नहीं रखती पर, मन है मेरा गंगाजल।।जब भी…साहचर्य विश्वास भरा दिन, प्रीति पगी हों शुचि रातें।आँखों की पीड़ा पढ़ लें, समझ सकें मन की बातें।साथ चलें हम हँसते गाते, सुखद सुनहरा होगा कल।।जब भी मैं…
- ▪ नसीम अहमद खान, उप संचालक, जनसंपर्कमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहा सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक तीन चरणों में आयोजित यह अभियान पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसंवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य शासन को जन-केंद्रित बनाना, जन सरोकार, जन विश्वास को मजबूत करना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करना है।पहले चरण में जनता जनार्दन से उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में 8 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी, ऑनलाइन पोर्टल और शिविर के माध्यम से आवेदन एकत्र प्राप्त किये गए। सुशासन तिहार के पहले चरण में मिले 40 लाख 94 हजार 495 आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है, जिसमें मांग से संबंधित 40 लाख 12 हजार 746 आवेदन और शिकायत से संबंधित मात्र 81 हजार 749 आवेदन शामिल हैं। द्वितीय चरण में इन आवेदनों का जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है, जबकि तृतीय चरण में 5 से 31 मई तक समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता से रूबरू होंगे। यह अभियान न केवल समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि राज्य के मैदानी इलाके से लेकर बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जनता का विश्वास जीत रहा है।इस अभियान का उद्देश्य स्पष्ट और व्यापक हैं। जनता की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना और जनता-शासन के बीच संवाद का सेतु बनाना। विशेष रूप से सुकमा, बीजापुर नारायणपुर, दंतेवाड़ा जिले के सुदूर क्षेत्रों में, जहां प्रशासन की पहुंच सीमित थी, यह अभियान जनता की आवाज को न केवल सुन रहा है, बल्कि त्वरित कार्रवाई के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।नारायणपुर के मुरियापारा में जीवन राम साहू की मांग पर वहां का वार्ड क्रमांक 10 स्ट्रीट लाइट्स से जगमगाने लगा है, जिससे रात में सुरक्षा और सुविधा बढ़ी है। बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में मंगल सिंह बैगा को 24 घंटे में ट्राइसाइकिल मिली और दिव्यांग पेंशन की पात्रता सुनिश्चित हुई है। मोहला-मानपुर चौकी जिले केे तेलीटोला में जर्जर स्कूल भवन के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की निर्मला जोगी को राशन कार्ड मिला, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। बस्तर के शम्भूनाथ कश्यप के राशन कार्ड में एक सप्ताह में पत्नी और बेटे का नाम जोड़ा गया, जिससे उनके परिवार को राशन की पूरी सुविधा मिल गई है।सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणाम समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। यह अभियान न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि सामुदायिक विकास को भी गति दे रहा है। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर बस्तर जैसे क्षेत्रों में फौती नामांतरण, निःशक्तजनों ट्राइसायकिल, पात्र लोगों को जॉब कार्ड, श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेजों का वितरण इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है। यह अभियान प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता का प्रतीक है, जिसने जनता में यह विश्वास जगाया है कि उनकी छोटी-बड़ी हर मांग सुनी जाएगी। जनता में उत्साह है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहां समाधान पेटी ने ग्रामीणों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया है। जनता की प्रतिक्रिया कि हमारी समस्याएं सुनी गईं, इसकी सफलता को रेखांकित करती हैं। सुशासन तिहार वास्तव में छत्तीसगढ़ के विकास, जन सरोकार और जनकल्याण का नया आयाम स्थापित कर रहा है।
-
- 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विशेष
विशेष लेख- छगन लोन्हारे, उप संचालक , (जनसंपर्क)मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। श्रम विभाग के तीनों मंडल - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं।प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि प्रदेश में विष्णु देव सरकार के सुशासन में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के श्रम मंत्री श्री देवांगन का कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर हाथ को काम इस दिशा में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।मजदूर दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए संकल्प लेना है। यह दिन श्रमिकों के योगदान को याद करने और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की याद में मनाया जाता है, जहां अनेक श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी। सन् 1889 में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज बुलंद करना है। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1923 में चेन्नई (मद्रास) से हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई।श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 125 करोड़ 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वर्ष 2025-26 में पंजीकृत 2 लाख 26 हजार संगठित श्रमिकों के लिए राज्य शासन के अनुदान हेतु 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि विष्णु देव सरकार की सोच है कि हर हाथ को काम मिले उसका उचित दाम मिले और हर पेट को अन्न मिले यह हमारी सरकार की आदर्श नीति है। इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके परिपालन में इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिसका विस्तार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समस्त जिलों में किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु विकासखण्ड स्तर पर मोबाईल कैम्प लगाए जाने की पहल विभाग द्वारा की गई है। अब तक 4 हजार 705 मोबाईल कैम्प लगाए जा चुके हैं।औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं का मुख्य दायित्व श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए 64 करोड़ 18 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। - - छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से आ रहे बदलावविशेष लेख - डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर , सहायक संचालक (जनसंपर्क)हर वर्ष 1 मई को हम श्रमिक दिवस मनाते हैं। यह एक ऐसा दिन जो श्रमिकों के अथक परिश्रम, संघर्ष और योगदान को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य की आर्थिक प्रगति में महिला श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाना जाता है।कृषि, खनन, वनों से प्राप्त उत्पादों और छोटे उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में महिलाएँ खेती-बाड़ी, तेंदूपत्ता संग्रहण और हस्तशिल्प निर्माण जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य, घरेलू सेवाएँ और छोटे व्यापारों में उनकी भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। महिला श्रमिकों की भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में, फिर भी उनकी मेहनत को अब भी उचित मान्यता और पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। महिला श्रमिकों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। जिनमें समान वेतन का अभाव, समान कार्य के बावजूद वेतन असमानता, खनन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में असुरक्षित परिस्थितियाँ, प्रसूति लाभों और स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित पहुँच, कम पढ़ाई और तकनीकी प्रशिक्षण के कारण सीमित अवसर, पारंपरिक सोच और घरेलू जिम्मेदारियाँ उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं।छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिसमें मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए विशेष सहायता दी जा रही है। नई श्रमिक नीति द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाया गया है। महिला शक्ति केंद्रों के विस्तार से प्रत्येक जिले में महिला शक्ति केंद्र स्थापित कर महिला श्रमिकों को कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर महिला स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सखी वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए त्वरित सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था। मनरेगा में महिलाओं के भागीदारी बढ़ाने रोजगार दिवसों में महिलाओं के न्यूनतम 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल शामिल हैं।छत्तीसगढ़ में महिला श्रमिकों कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से मिनीमाता महतारी जतन योजना है, जो पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता प्रदान करती है।इस योजना के तहत बच्चे के जन्म के बाद पंजीकृत महिला श्रमिकों को 20 हजार की एकमुश्त राशि मिलती है। इसके अलावा राज्य सरकार विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम और सहायता योजनाएं भी चलाती है, जो महिला श्रमिकों को सशक्त बनाने में मदद करती हैं।मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु के बीच की पंजीकृत महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण के लिए सहायता प्रदान करती है।छत्तीसगढ़ महिला कोष महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जिसमें वित्तीय सहायता प्रशिक्षण और अन्य संसाधन शामिल हैं।घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना,घरेलू महिला श्रमिकों, ठेका श्रमिकों और हमाल श्रमिकों के कौशल विकास और परिवार को सशक्त बनाने के लिए योजना है। सक्षम योजना छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत संचालित एक योजना है जो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। महतारी वंदन योजना से महिलाओं को 1 हजार रूपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।छत्तीसगढ़ सरकार महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है, प्रशिक्षण के बाद उनके रोजगार का प्रबंध भी कर रही है, ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती मिल सके, सरकार माताओं-बहनों तक जनहितैषी योजनाओं के शत प्रतिशत लाभ की पहुंच भी सुनिश्चित कर रही है। जबकि स्वयं सहायता समूहों के जरिए आर्थिक स्वतंत्रता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय सरकार में प्रदेश के विकास में महिला श्रमिकों के योगदान को सम्मान मिला है।
- - केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगनभारत ने सदैव कहानी कहने की कला में उत्कृष्टता हासिल की है। रामायण और महाभारत जैसे कालातीत महाकाव्यों ने पीढ़ियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हमारी कथाएं इन गाथाओं से आगे बढ़ती हैं और सांस्कृतिक आधारशिला के रूप में कार्य करते हुए उन्हें यह आकार देती हैं कि हम दुनिया को किस तरह से देखने के साथ-साथ रचनात्मकता व्यक्त करते हुए कलाकारों एवं दूरदर्शी लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। कहानी कहने का यह अंतर्निहित उत्साह एक सशक्त रचनात्मक आकांक्षा के रूप में विकसित हुआ है और अब यह भारत को वैश्विक मीडिया पावरहाउस के रूप में उभरने में भी सहायता कर रहा है।1 से 4 मई 2025 तक आयोजित होने वाला प्रथम विश्व श्रव्य-दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) भारत को वैश्विक रचनात्मकता के केंद्र में रखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित, वेव्स एक परिवर्तनकारी आंदोलन है और यह मीडिया तथा मनोरंजन (एमएंडई) परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगा। भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग 2.7 ट्रिलियन रुपये के करीब पहुंच चुका है, ऐसे में वेव्स 2025 रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता में अग्रणी होने के हमारे संकल्प का संकेत देता है।भारत का विषय निर्माण परिदृश्य अब पारंपरिक मीडिया से एक संपन्न डिजिटल-प्रथम इकोसिस्टम में परिवर्तित हो चुका है। इसके साथ-साथ अब यह स्ट्रीमिंग सेवाओं, सोशल मीडिया और उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वैश्विक संपर्क का भी विस्तार कर रहा है। भारत में विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन, सह-निर्माण समझौते और फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) जैसी सरकारी पहल वैश्विक रचनाकारों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती है।मीडिया और मनोरंजन का बदलता परिदृश्यवेव्स 2025 भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक नए युग के शुभारंभ का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर के अभिनवकर्ताओं, नीति निर्माताओं, कलाकारों और उद्योग जगत प्रमुखों को एक साथ लाकर, शिखर सम्मेलन सहयोग के वातावरण को बढ़ावा देता है। इसके साथ-साथ यह मनोरंजन के निर्माण, वितरण और अनुभव को एक नया रूप देगा।इस परिवर्तन के केंद्र में वेवैक्स 2025 और वेव्स बाज़ार जैसी पहल हैं। वेवैक्स 2025 गेमिंग, एनिमेशन, एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्सआर), जनरेटिव एआई और नेक्स्ट-जेन कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म जैसी उभरती हुई तकनीकों में कार्य करने वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाता है। यह पहल स्टार्टअप के लिए अपने विचारों को प्रदर्शित करने, मेंटरशिप हासिल करने और उद्यम पूंजीदाता और सेलिब्रिटी एंजेल निवेशकों के साथ वार्तालाप के माध्यम से सुरक्षित वित्त पोषण के लिए एक आधार तैयार करती है। दूसरी ओर, वेव्स बाजार एक गतिशील ई-मार्केटप्लेस के रूप में कार्य करता है जिसे रचनाकारों, खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। 5,500 से अधिक खरीदारों, 2,000 विक्रेताओं और फिल्म, टेलीविज़न, गेमिंग, विज्ञापन के अलावा 1,000 पंजीकृत परियोजनाओं के साथ यह बाज़ार सहज सहयोग और अवसर खोज के लिए एक स्थल है। एआई-संचालित मैचमेकिंग यह सुनिश्चित करती है कि परियोजना और पेशेवरों को सही कनेक्शन, नवाचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा मिले। ये प्लेटफ़ॉर्म एक कार्यक्रम के संचालन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ एक परिवर्तनकारी इकोसिस्टम हैं जो वेव्स के समापन के बाद भी मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को प्रभावित करता रहेगा। यह भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एक और महत्वपूर्ण उपलबिध सिद्ध होगा।युवाओं के लिए एक स्वर्णिम मंचहमारा सबसे बड़े जनसांख्यिकीय लाभ के रूप में भारत के युवा, वेव्स पहल से अत्यंत लाभान्वित होंगे। 29 वर्ष की औसत आयु के साथ, भारत न केवल दुनिया का सबसे युवा देश है बल्कि रचनात्मकता और नवाचार के मामले में सर्वाधिक जीवंत राष्ट्र भी है। वेव्स 2025 युवाओं को अपने दृष्टिकोण में अग्रणी रखने के साथ-साथ कौशल विकास, उद्यमिता और वैश्विक सहयोग के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है।क्रिएट इन इंडिया चैलेंज इस प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। 1,100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित लगभग 1,00,000 पंजीकरणों के साथ इस चुनौती ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक प्रतिभाओं के एक विविध समूह को आकर्षित किया है। क्रिएटोस्फीयर के हिस्सा के रूप में फाइनल प्रतिभागियों को उद्योग प्रमुखों से जुड़ने, मास्टरक्लास में भागीदारी करने और वैश्विक प्रदर्शन हासिल करने के शानदार अवसर प्राप्त होंगे।इसके अलावा, मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) की स्थापना भारत के युवाओं के भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतीक है। कौशल विकास और नवाचार के लिए उत्कृष्टता के एक वैश्विक केंद्र के रूप में, आईआईसीटी रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी के बीच के अंतर को दूर करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि युवा भारतीयों के पास मीडिया और मनोरंजन उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने से जुड़ी विशेषज्ञता हासिल हो।सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोगशिखर सम्मेलन में वैश्विक मीडिया संवाद भी शामिल होगा, जिसमें वैश्विक प्रमुखों, नीति निर्माताओं, कलाकारों और उद्योग जगत के पेशेवर एकसाथ भागीदारी करेंगे। यह संवाद केवल चर्चाओं के संदर्भ में ही नहीं है अपितु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नैतिक कार्य प्रणालियों और नवाचार के लिए रणनीति विकसित करने से जुड़ी कार्यवाही के लिए भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्योग हितधारकों के साथ निर्धारित संवाद से प्रभावशाली साझेदारी शुरू होने की आशा है, जिससे आने वाले वर्षों में भारत लाभान्वित होगा।विकसित भारत के लिए दृष्टिकोणवेव्स 2025 केवल एक आयोजन नहीं है, यह विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो एक विकसित राष्ट्र के तौर पर रचनात्मकता और नवाचार में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। विविधता को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और युवाओं को सशक्त बनाने के माध्यम से, वेव्स 2025 भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सतत विकास में सक्षम प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करता है।वेव्स 2025 रचनात्मक उद्योग की अनंत संभावनाओं का सुदृढ़ीकरण है। यह अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा, तकनीकी कौशल और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। यह परंपरा और प्रौद्योगिकी के संगम के माध्यम से वैश्विक रचनात्मक इकोसिस्टम को फिर से परिभाषित करने के भारत के दृष्टिकोण का प्रमाण भी है।
-
-लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे
- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
मार निहत्थे लोगों को तुम, ताकत अपनी दिखलाते हो।
दीनोईमान के नाम पर, नादानों को बहकाते हो ।।
बीज नफरतों के बोते हो, मानवता चढ़ती बलि-वेदी।
छुपकर अपनों पर घात किए,लंका ढाए घर के भेदी।
बचपना छीन कर बच्चों का,असला बंदूक थमाते हो ।।
मार निहत्थे लोगों को तुम, ताकत अपनी दिखलाते हो।।
भ्रष्टाचारी शीश उठाए, जयकार करे अन्यायी का।
न्याय धर्म के मंदिर दूषित, व्यवहार करें व्यवसायी का ।।
चरण वंदना स्वार्थ साधने,धन बल को बाप बनाते हो ।।
मार निहत्थे लोगों को तुम, ताकत अपनी दिखलाते हो।।
हिंसा नहीं सिखाता कोई, हर धर्म सिखाता समरसता।
पहचान यही इंसानों की, सहयोग दया करुणा ममता।
जाति वर्ग में बाँट सभी को , वैमनस्यता फैलाते हो ।।
मार निहत्थे लोगों को तुम, ताकत अपनी दिखलाते हो।। - ▪️नसीम अहमद खान, उपसंचालक जनसंपर्करायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में इन दोनों ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार एक अभिनव अभियान मोर दुवार- साय सरकार के माध्यम से गरीब ,वंचित और आवासहीन परिवारों के यहां दस्तक देकर उन्हें सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का अधिकार देने में जुटी है।मुख्यमंत्री श्री साय ने बीते दिनों जगदलपुर प्रवास के दौरान घाटपदमपुर ग्राम से इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । इस बात को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के दूसरे दिन ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर स्पष्ट कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास देने के अपने संकल्प को पूरा कर रही है।छत्तीसगढ़ में चल रही ग्रामीण आवास क्रांति का ही यह परिणाम है कि अब गांवों में विशेषकर पिछड़े और गरीब तबके की बस्तियों में मिट्टी के जीर्णशीर्ण घरों और बांस- बल्ली के सहारे टिकी घास-फूंस की झोपड़ी की जगह अब साफ-सुथरे पक्के मकान बने हुए अथवा बनते दिखाई देने लगे हैं। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर सुदूर वनांचल का कोई ऐसा गांव अथवा मजरा- टोला नहीं, जहां 8-10 पक्के घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हाल- फिलहाल में न बने हों। यह योजना न केवल लाखों गरीब परिवारों को छत दे रही है, बल्कि रोजगार, व्यापार और उद्योगों को भी गति प्रदान कर रही है। इससे सीमेंट, ईट, सरिया और निर्माण सामग्री से जुड़े व्यवसाय में तेजी आयी है। यह जनकल्याण और आर्थिक विकास का एक संतुलित मॉडल है।छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कुल 11,50,315 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसमें से अब तक 9,41,595 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ प्रवास दौरान राज्य को अतिरिक्त 3 लाख आवासों की स्वीकृति देने से यह प्रयास और भी व्यापक हो गया है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ग्रामीण आवासीय पहल है।राज्य सरकार समाज के सभी वर्ग के पात्र परिवारों के साथ-साथ बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध करा रही है। महासमुंद जिले के धनसुली गांव की कमार बस्ती में 15 से अधिक कमार परिवारों को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इससे इन जनजातीय परिवारों के जीवन में स्थायित्व आया है और वे शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं।छत्तीसगढ़ सरकार का मोर दुवार- साय सरकार अभियान 30 अप्रैल तक तीन चरणों में संचालित है, जिसमें पात्र हितग्राहियों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना और ग्राम सभाओं के माध्यम से सूची का वाचन और शत-प्रतिशत पात्र परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के साथ ही सर्वेक्षण पूर्ण करने वाले कर्मियों का सार्वजनिक सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा गांव में जाकर सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ करना और हितग्राहियों से उनके बारे में जानकारी लेना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और संकल्पित है।इस अभियान को जन अभियान का स्वरूप देने के लिए जनप्रतिनिधियों, जनसेवियों और स्थानीय कलाकारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पीएम आवास पंचायत एम्बेसडर के रूप में नामित व्यक्तियों द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। गृह पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता एवं जानकारी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त, राज्य में जरूरत मंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 47,090 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 38,632 आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार की विशष पहल पर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ितों परिवारों के लिए 15,000 विशेष आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनका निर्माण कराया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए 42,326 आवास के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब तक 27,778 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 6,482 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। नियद-नेल्ला-नार योजना के अंतर्गत अब तक 477 आवास पूर्ण कराए गए हैं।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बिलासपुर से 3 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराना इस योजना की सफलता है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 18 लाख पात्र हितग्राहियों को आवास से वंचित रखा गया। छत्तीसगढ़ सरकार अब हर हितग्राही को उसका अधिकार दिलाने की दिशा में काम कर रही है। मोर दुवार- साय सरकार महाअभियान शासन की संवेदनशीलता, नीति की पारदर्शिता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह अभियान केवल योजना की सफलता नहीं, बल्कि एक मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
-
गीत
-लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे
- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
कोलाहल से दूर कहीं चल, आलय एक बनाएँ ।
नीले छत पर टाँग सितारे, सुंदर महल सजाएँ ।।
सरिता की हो निर्मल धारा, चिड़ियों की मीठी धुन।
क्या कह गई पवन कानों में, चुपके हम लेवें सुन।
नाजुक बेलों की दीवारें, कोमल पात बिछौने।
हरियाली की चादर ओढ़े, जाएँ हम नित सोने ।
मद्धिम स्वर में लोरी गाते,मलयानिल के झोंके,
निंदिया से बोझिल पलकों को,छू शबनम सहलाएँ।।
उषा किरण आ हमें जगाती, कर स्नेहिल आलिंगन।
मधुरिम रंगोली से सज्जित, अंबर दे आमंत्रण।
नित्य दिवाकर भरे प्राण में, उम्मीदों के मोती।
स्वर्ण-पालकी अभिलाषा की, धीरज कभी न खोती।
चहकें अँगनाई में आकर, विहग-वृंद खुशियों के,
प्रीति-पताका सुखद सदन में, हम तुम मिल फहराएँ ।।
रचें रुचिर संसार स्नेह का, सुंदर सुरुचि मनोहर ।
मनभावन रमणीय दृश्य ज्यों,नीरज खिले सरोवर।
निश्छलता लेती अँगड़ाई, शुचिता गान प्रभाती।
दृग बनकर संवदिया पढ़ लें, प्रिय के मन की पाती।
अंतर्भासित प्रांजल दीपक, दिवस-निशा का सहचर,
निकल कलह तम की छाया से, सुख उज्ज्वल हम पाएँ ।। -
-सजल
-लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे
- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
गीत कोई नया गुनगुनाते रहें।
जिंदगी को खुशी से सजाते रहें ।।
भूलते जा रहे मूल्य को आज सब।
मार्ग सच्चा सभी को सुझाते रहें।
सामना हम करें मुश्किलों का सदा।
हार को जीत अपनी बनाते रहें।।
कुछ नया हम करें याद दुनिया रखे ।
राह आसान सबको दिखाते रहें ।।
आपदा में नहीं साथ छोड़ें कभी।
हौसला साथियों का बढ़ाते रहें।।
कोशिशें हों सुखी सब रहें आपसे।
नित्य गिरते हुए को उठाते रहें।। -
आलेख - जीएस केशरवानी
एक समय मध्यप्रदेश का हिस्सा रहे छत्तीसगढ़ को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने नए राज्य का दर्जा दिया तब उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे, हर स्तर पर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन हो। उनकी इसी कल्पना को साकार करने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के लोगों की सेवा के लिए सुशासन की स्थापना को लक्ष्य बनाया है।लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ है पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, इसी लक्ष्य को लेकर सत्ता में आयी विष्णुदेव साय की सरकार ने पिछले एक साल में मोदी की गारंटी को तेजी से पूरा किया है। इसके साथ ही इस सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नालाजी ड्रिवन एप्रोच को अपनाया है। सुशासन की इसी अवधारणा को जमीनी धरातल में उतारने के लिए राज्य सरकार ने सुशासन तिहार शुरू किया है। लगभग दो माह में चलने वाले इस राज्यव्यापी अभियान में लोगों की समस्याओं के निराकरण के साथ ही लोगों की जनाकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को दिशा दी जाएगी।सुशासन तिहार के इस राज्य व्यापी अभियान के पहले चरण में आम जनता से उनकी मांगों समस्याओं के संबंध में आवेदन 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में लगभग एक माह तक आवेदनों का निराकरण होगा। तीसरे और अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन होगा। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और अधिकारी राज्य के विभिन्न हिस्सों में आकस्मिक निरीक्षण कर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगें और जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। इस पूरे अभियान का उद्देश्य प्रशासन को और अधिक जवादेह और पारदर्शी बनाना है।राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही सुशासन और अभिसरण का गठन किया। इस नए विभाग के माध्यम से सभी स्तरों में पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था सुनिश्चित करने के कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंत्रीमण्डल के सभी सदस्यों को प्रबंधन के गुर सिखाने के लिए आई.आई.एम में प्रशिक्षण दिया गया। सुदुर वनांचल में सुशासन की राह में बाधा बने माओवादियों पर अब तक की सबसे कड़ा प्रहार इस सरकार ने किया है। केन्द्र सरकार के सहयोग से इस डबल इंजन की सरकार ने पिछले 15 महीनों में ही साढे तीन सौ से अधिक नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। लगभग दो हजार से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। माओवाद आतंक के कलंक को दूर करने के लिए देश की सबसे अच्छी पुनर्वास नीति लागू की है। इन सबका परिणाम यह निकल रहा है कि मार्च 2026 से पहले ही माओवाद की विदाई लगभग तय है।सुशासन लाने के लिए सरकार एक और परम्परागत तरीकों के साथ ही आईटी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में अधिकांश योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही है। इसके अलावा आफिस के काम-काज में तेजी लाने के लिए सभी विभागों में चरण बद्ध ढंग से ई-आफिस प्रणाली लागू की जा रही है। सरकारी काम काज में टेक्नालाजी ड्रिवन एप्रोज निश्चित रूप से सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ी भूमिका निभाएगा। आगे आने वाले दिनों में प्रशासन में काफी बदलाव नजर आएगा। - -लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)राम नाम जप ले रे मनवा, निशिदिन साँझ-सवेरे ।आशा का सूरज निकलेगा, मन से मिटे अँधेरे ।।काम क्रोध मद मोहक माया, मन को बहकाती है ।पाप- पंक में डूबी काया, जीवन भटकाती है ।पावन रखने मन की बगिया ,कर्म करें बहुतेरे ।राम नाम जप ले रे मनवा निशिदिन साँझ सवेरे ।।सुरभित सुंदर दलपुंजों सम, सदाचार शुचि रखना ।झंकृत हो जाए हृदवीणा, बोले मधुरिम रसना ।सुरसरिता सम निश्छल निर्मल, चितवन कुंज घनेरे ।राम नाम जप ले रे मनवा निशिदिन साँझ सवेरे ।।भवसागर में जीवन तरणी, डगमग - डगमग डोले ।मोह -भँवर में फँसी हुई यह, खाती है हिचकोले ।कुसुम-कंटकित पथ पर भटके, प्रेमिल पथिक चितेरे ।राम नाम जप ले रे मनवा निशिदिन साँझ सवेरे ।।
- आलेख- प्रशांत शर्माहिन्दी फिल्म जगत में जब भी देशभक्तिपूर्ण फिल्मों का जिक्र होता है, तो सबसे पहले भारत कुमार यानी मनोज कुमार ही याद किए जाते हैं। उनकी फिल्मों ने अपने दौर में एक अलग ही पहचान बनाई थी। मनोज कुमार की फिल्मों की कहानी , उसका संगीत ्आज भी कालजयी कहलाते हैं।हरिशंकर गिरि गोस्वामी यानी मनोज कुमार के नाम के साथ अनेक हिट फिल्में जुड़ी हुई है। भगत सिंह के जीवन पर आधारित शहीद फिल्म के बाद देशभक्ति आधारित फिल्मों में उनका खूब नाम हुआ। एक लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज करने वाले मनोज कुमार को उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपडा और मकान, क्रांति, नील कमल, हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, हिमालय की गोद में, दो बदन और शोर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत कुमार के नाम से अधिक पहचान मिली है, क्योंकि अपनी ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने अपना नाम भारत ही रखा।मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को ऐबटाबाद (पाकिस्तान) में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया और फिर मुंबई। जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो वे दिलीप कुमार साहब से बहुत प्रभावित थे। दिलीप कुमार से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी नाम हरिशंकर गिरि गोस्वामी से मनोज कुमार रखा और इसी नाम ने उन्हें अपार सफलता, लोकप्रियता दिलाई।मनोज कुमार ने अपने बॉलीवुड करिअर की शुरुआत डायरेक्टर लेखराज भाकरी की 1957 में आई फिल्म फैशन से की थी, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि लेखराज भाकरी असल जिंदगी में मनोज के रिश्तेदार ही थे। अपनी पहली फिल्म में मनोज ने 80 साल के एक भिखारी का किरदार निभाया था। फिल्म सफल नहीं रही तो मनोज कुमार को किसी ने खास नोटिस भी नहीं किया। आखिरकार फिल्म शहीद से उन्हें सही पहचान मिली । इस फिल्म में उन्होंने भगत सिंह के रोल में जैसे जान ही डाल दी थी। यह फिल्म सुपर हिट हुई और मनोज कुमार भी निर्माता-निर्देशकों की पसंद बन गए। यहां तक शहीद भगत सिंह की मां विद्यावती भी मनोज कुमार को भगत सिंह के रूप में देखकर बोली थीं कि मेरा बेटा ऐसा ही लगता था।मनोज कुमार के जीवन से जुड़ी खास बातें- मनोज कुमार हवाई जहाज में सफर नहीं करते हैं। फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के लिए हवाई जहाज में बैठने पर उनके मन में डर बैठ गया था, जिसके बाद से उन्होंने कभी दोबारा हवाई सफर नहीं किया ।- फिल्म उपकार की प्रेरणा मनोज कुमार को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिली थी। दरअसल शास्त्री जी को मनोज कुमार की फिल्म शहीद बेहद पसंद आई थी जिसे देखने के बाद उन्होंने मनोज कुमार को जय जवान,जय किसान पर फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। शास्त्री जी के सुझाव से मनोज इतने प्रभावित हुए कि शास्त्री जी से मुलाकात के बाद ट्रेन में दिल्ली से मुंबई लौटते वक्त ही उन्होंने फिल्म उपकार की कहानी तैयार कर ली थी। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ।- पूरब और पश्चिम से तो मनोज कुमार भारत कुमार के रूप में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए. इसका एक कारण यह भी था कि इस फिल्म के लिए इंदीवर ने एक गाना लिखा था- भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यह गीत उस समय इतना लोकप्रिय हुआ कि हर किसी की जुबान पर यह गीत चढ़ गया। आज भी यह गीत इतना लोकप्रिय है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस पर यह रेडियो टीवी सहित स्कूल, कॉलेज आदि के समारोह में खूब गाया, बजाया जाता है।- बॉलीवुड की 16 फिल्मों में साथ काम कर चुके अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को सबसे पहले स्क्रीन पर मनोज कुमार अपनी फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान में साथ लाए थे। इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन का करिअर ढलान पर आ गया था और वो मुंबई छोडऩे का मन बना चुके थे, लेकिन मनोज कुमार ने उन्हें मुंबई छोड़ कर जाने से रोका और अपनी फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान का ऑफर दिया। फिल्म सुपर हिट हुई।- भारत कुमार के रूप में लोकप्रियता हासिल करने के बाद मनोज कुमार को सार्वजनिक जीवन में सिगरेट पीने पर एक लडक़ी की डांट भी सुननी पड़ी थी। एक बार मनोज कुमार ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया- एक बार मैं परिवार के साथ किसी रेस्तरा में खाना खाने गया। खाने का ऑर्डर देने के बाद मैं सिगरेट पीने बैठ गया। तभी सामने बैठी एक लडक़ी बड़े गुस्से से मेरे पास आकर बोली- आप कैसे भारत कुमार हैं । भारत कुमार होकर सिगरेट पीते हैं। उस लडक़ी की यह बात सुन मैं और मेरा परिवार दंग रह गया लेकिन मैंने तभी सिगरेट फेंक दी थी।-मनोज कुमार ने देशभक्ति पूर्ण फिल्मों के अलावा ध्वनि प्रदूषण पर एक फिल्म बनाई थी- शोर। फिल्म में दिव्यांगों की जि़ंदगी की समस्याओं को भी बहुत ही संजीदगी से दिखाया गया था। फिल्म में संतोष आनंद के लिखे मधुर गीत एक प्यार का नगमा है, का जादू आज भी बरकरार है।-मनोज कुमार के पसंदीदा हीरो दिलीप कुमार थे, तो वहीं नायिकाओं में उन्हें कामिनी कौशल पसंद थी, जिनके साथ उन्होंने फिल्म शहीद में काम किया था।- मनोज कुमार को वर्ष 1992 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके साथ ही उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवॉर्ड भी मिल चुका है।
-
.jpg) आलेख -प्रशांत शर्माआज सुबह -सुबह एक बड़ी मनहूस खबर मिली... दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार नहीं रहे। आज तडक़े उन्होंने मुंबइ के अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पता नहीं क्यों कल रात से ही मैं उनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गाना - मैं ना भूलूंगा ...गुनगुना रहा था....यह गाना मुझे काफी पसंद है। मुकेश और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज से सजा यह गाना आज भी लोगों की जुबान पर है।आज पूरा देश अपने पसंदीदा नायक को श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहा है। उन्हीं के सम्मान में आज इस गाने के बारे में जिक्र कर रहा हूं। मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान 1974 में रिलीज हुई थी। फिल्म में मनोज कुमार के साथ जीनत अमान और मौसमी चटर्जी नजर आई। वहीं शशि कपूर और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म में यह भावुक गाना दो वर्जन में है- एक सामान्य और दूसरा सेड माहौल में रचा - बसा है। गाने को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत- प्यारेलाल की जोड़ी ने और लिखा संतोष आनंद ने।यह फि़ल्म सन 1974 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फि़ल्म बन गई, और इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। फि़ल्म को तीन फि़ल्मफ़ेयर पुरस्कार मिले, साथ ही ग्यारह अन्य पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया गया।फिल्म में छह गाने थेे और सभी 4 से 6 मिनट वाले थे। "मेहंगाई मार गई" कव्वाली जो लता मंगेशकर, नरेंद्र चंचल , मुकेश, जानी बाबू कव्वाल की आवाज में थी 8 मिनट 51 सेकंड लंबी थी। सभी गानों की एक खास बात ये थी कि लंबे होने के बाद भी वे कभी बोझिल नहीं लगे। फिल्म को लिखा मनोज कुमार ने और निर्देशित भी किया । फिल्म के निर्माता भी वहीं थे। फिल्म के लिए मनोज कुमार को सर्वेश्रे्ठ निर्देशक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वहीं गायक महेन्द्र कपूर ने -और नहीं बस और नहीं... गाने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसी तरह गीतकार संतोष आनंद को भी यह सम्मान मिला। फिल्म की झोली में एक और फिल्म फेयर अवार्ड गया जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का था।अब इस गाने के बारे में .....मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी....गीत मोहब्बत का एक हसीं वादा प्रस्तुत करता है। यह गाना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इससे निश्छल प्रेम-बंधन की भीनी-भीनी खूशबू महसूस होती है। इस पूरे गाने में प्रेमी और प्रेमिका अपने-अपने हिस्से के वादों में खोए हुए हैं। इसमें रस्मों और कसमों का बंधन दोनों को अपने मोहपाश में जैसे समेट लेता है।जैसे कि- मैं ना भूलूँगा, मैं ना भूलूँगीइन रस्मों को इन क़समों को इन रिश्ते नातों कोमैं ना भूलूँगा, मैं ना भूलूँगी
आलेख -प्रशांत शर्माआज सुबह -सुबह एक बड़ी मनहूस खबर मिली... दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार नहीं रहे। आज तडक़े उन्होंने मुंबइ के अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पता नहीं क्यों कल रात से ही मैं उनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गाना - मैं ना भूलूंगा ...गुनगुना रहा था....यह गाना मुझे काफी पसंद है। मुकेश और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज से सजा यह गाना आज भी लोगों की जुबान पर है।आज पूरा देश अपने पसंदीदा नायक को श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहा है। उन्हीं के सम्मान में आज इस गाने के बारे में जिक्र कर रहा हूं। मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान 1974 में रिलीज हुई थी। फिल्म में मनोज कुमार के साथ जीनत अमान और मौसमी चटर्जी नजर आई। वहीं शशि कपूर और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म में यह भावुक गाना दो वर्जन में है- एक सामान्य और दूसरा सेड माहौल में रचा - बसा है। गाने को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत- प्यारेलाल की जोड़ी ने और लिखा संतोष आनंद ने।यह फि़ल्म सन 1974 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फि़ल्म बन गई, और इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। फि़ल्म को तीन फि़ल्मफ़ेयर पुरस्कार मिले, साथ ही ग्यारह अन्य पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया गया।फिल्म में छह गाने थेे और सभी 4 से 6 मिनट वाले थे। "मेहंगाई मार गई" कव्वाली जो लता मंगेशकर, नरेंद्र चंचल , मुकेश, जानी बाबू कव्वाल की आवाज में थी 8 मिनट 51 सेकंड लंबी थी। सभी गानों की एक खास बात ये थी कि लंबे होने के बाद भी वे कभी बोझिल नहीं लगे। फिल्म को लिखा मनोज कुमार ने और निर्देशित भी किया । फिल्म के निर्माता भी वहीं थे। फिल्म के लिए मनोज कुमार को सर्वेश्रे्ठ निर्देशक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वहीं गायक महेन्द्र कपूर ने -और नहीं बस और नहीं... गाने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसी तरह गीतकार संतोष आनंद को भी यह सम्मान मिला। फिल्म की झोली में एक और फिल्म फेयर अवार्ड गया जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का था।अब इस गाने के बारे में .....मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी....गीत मोहब्बत का एक हसीं वादा प्रस्तुत करता है। यह गाना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इससे निश्छल प्रेम-बंधन की भीनी-भीनी खूशबू महसूस होती है। इस पूरे गाने में प्रेमी और प्रेमिका अपने-अपने हिस्से के वादों में खोए हुए हैं। इसमें रस्मों और कसमों का बंधन दोनों को अपने मोहपाश में जैसे समेट लेता है।जैसे कि- मैं ना भूलूँगा, मैं ना भूलूँगीइन रस्मों को इन क़समों को इन रिश्ते नातों कोमैं ना भूलूँगा, मैं ना भूलूँगी
चलो जग को भूलें, खयालों में झूलेंबहारों में डोलें, सितारों को छूलेंआ तेरी मैं माँग संवारूँ तू दुल्हन बन जायेमाँग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूँगीगाने के फिल्मांकन में उस समय के कैमरे की उम्दां तकनीक की झलक देखने को मिलती है। ऐसी ही तकनीक मनोज कुमार ने फिल्म शोर के गाने - एक प्यार का नगमा है... में इस्तेमाल की थी। यह गाना भी कालजयी है।मैं ना भुलूंगा.. गीत में एक पंक्ति आती है - 'इन रस्मों को, इन क़समों को'..तब कैमरा नायिका जीनत अमान की उंगली पर पहनी अंगूठी पर फोकस होता है जैसे नायिका कह रही हो- हां यही प्रेम- भाव है जो उसने पहन रखा है। गाने की अगली पंक्ति में जग को भूलने.... सितारों को छूने जैसी कल्पनाओं के बाद नायक का मांग भरने की बात कहना , उनके प्रेम को आजीवन निभाने का वादा है और नायिका कहती है कि मांग से दुल्हन का रिश्ता मैं ना भुलूंगी।इसी तरह से गीत की आगे की पंक्तियों में नायक- नायिका जीवन-सांसों के गठजोड़ के साथ कभी भी साथ न छोडऩे का वादा करते हैं। वहीं मंदिर से पूजा तक के पवित्र रिश्ते की बात करते नजर आते हैं। किसी ने सही कहा है कि यदि प्रिय साथी हमसफर हो तो जमाने की क्या चिंता करना। जहां कहीं बस जाएंगे और दिन कट जाएंगे। मोहब्बत की शिद्धत ही कुछ ऐसे होती है।गीतकार संतोष आनंद ने सच में इस पूरे गाने में ऐसा अनोखा भाव. प्रेम रस, वादा पिरोया है, जिसे निर्माता-निर्देशक , अभिनेता मनोज कुमार ने जीवंत किया है। ऐसे महान कलाकार को देश कभी नहीं भूलेगा।महान कलाकार , निर्देशक मनोज कुमार को शत शत नमन। -
-लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे
- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
चैत्र की नवरात्रि आई , मात आई आज द्वार ।
भोर शुभ नव वर्ष आया , रंग रंगोली पुष्प हार ।।
आ सजाएँ तोरणों से , अंबुजा कर श्वेत धार ।
दैत्य का संहार करती , बोझ धरती का उतार ।। 1 ।।
धारिणी जग तारिणी माँ , शेर पर होकर सवार ।
मारना लालच घृणा को , तोम तम मद को उतार ।।
भाव परिमल पावनी हों , लें सभी जीवन सुधार ।
भक्ति करते शक्ति देना , कीजिए भवसार पार ।। 2 ।।
श्वेत वसना पद्मजा तू , कालरात्री कर प्रहार ।
खेलते जो लाज से वो , नर्क में जाएँ सिधार ।।
शैलपुत्री विंध्य वासी , धारती कर असि त्रिशूल ।
कोप से बच शत्रु भागे , आसुरी निज कृत्य भूल ।। 3 ।। -
-लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे
- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
बेगानों की बस्ती में हम, आए हैं ठौर बनाने ।
जीत सकेंगे हृदय प्रेम से, सोचा करते दीवाने ।।
हाथ बढ़ाकर गले लगाया, केवल अपनापन चाहा।
द्वेष - दंभ के दावानल में, मूल्य हुए सारे स्वाहा ।
छल कर जाते मित्र बनाकर, छद्मवेष मानव देखा ।
सत्य - झूठ के बीच नहीं है, खिंची हुई कोई रेखा ।
भ्रष्ट आचरण के दलदल में, धँसते जाते मनमाने ।।
लेन-देन की आदी दुनिया ,पहले नजरों से तौले ।
लाभ-हानि का हिसाब करती , अपनाती हौले-हौले ।
हित देखे संबंधों में भी , स्वार्थ निजी देखा करते ।
देख सदा धन पद वैभव को, मृदुल बोल मुख से झरते ।
हम बनते जा रहे तंत्र के , हिस्से जाने-अनजाने ।।
कील चुभा जाता है पग में, राहों पर सच की निकले।
आँच सेंक कर आत्मबोध की, बर्फ जमी शायद पिघले।
जन्म लिया है मानव का तो, आन रखें मानवता की।
क्षुद्र सोच के तोड़ दायरे, बात करें अब समता की।
नीति जियो जीने दो वाली, अपनाएँ सब सुख पाने ।। - *आलेख - अमिताभ कांत *ट्रम्प प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ और ‘अमेरिका को फिर से महान बनाने’ की नीतियों पर दोगुना जोर दे रहा है। ट्रम्प प्रशासन अतीत के गठबंधनों को फिर से परिभाषित और पुनर्लेखन करने का काम भी कर रहा हैजिसकी गूंज यूरोप और एशिया में उनके सहयोगियों द्वारा महसूस की जा रही है। इन कदमों का उद्देश्य व्यापार संतुलन में सुधार और सार्वजनिक व्यय को कम करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अमेरिका ने पेरिस समझौते वविश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से खुद को अलग कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से भी वह पहले ही अलग हो चुका है। ये कदम वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था में एक शून्य पैदा कर रहे हैं। यह शून्य लंबे समय तक नहीं रहेगा-इसे प्रतिस्पर्धी शक्तियों द्वारा भरा जाएगा। अमेरिका सबसे शक्तिशाली बना हुआ है और हम एक बार फिर एक बहुध्रुवीय दुनिया का उदय देख रहे हैं। विखंडित वैश्वीकरण, तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई, ऊर्जा की भू-राजनीति और ढहता वैश्विक शासन विश्व को नया आकार देने वाले प्रमुख भू-राजनीतिक रुझान हैं जिनसे भारत को निपटना होगा।वैश्वीकरण का विखंडनजैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में हमने जो वैश्वीकरण का युग देखा था, वह समाप्त होने वाला है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से, हमने वैश्वीकरण का विखंडन देखा है। व्यापार युद्धों ने इस विखंडन को और तेज़ कर दिया है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारी व्यवधान पैदा कियाऔर इसके फलस्वरूप देशों और व्यवसायों को वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने के लिए प्रेरित किया। ट्रम्प प्रशासन द्वारा फिर से टैरिफ़ लगाने के साथ, व्यापार युद्धों का दूसरा युग हमारे सामने है। चाहे पारस्परिक हो या सभी टैरिफ़, व्यापार युद्ध विश्व व्यापार को बहुत ज़्यादा बाधित करेंगे। व्यापार युद्ध अब सिर्फ़ बिक्री की वस्तु ओं के बारे में नहीं रह गए हैं। वे प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और औद्योगिक नीति जैसे कारकों को प्रभावित करते हैं। देश ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्योगों में संरक्षणवाद और क्षमताओं का निर्माण करने का सहारा ले रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अधर में लटके होने के साथ, देश द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौतों की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फ्रेंड-शोरिंग का उदय और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने का लक्ष्य भारत के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। हम सही नीतियों, रणनीतिक द्विपक्षीय व्यापार सौदों और व्यापार सुगमता पर ध्यान केंद्रित करके विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर सकते हैं।प्रौद्योगिकी: वैश्विक शक्ति के लिए युद्ध का मैदानप्रथम औद्योगिक क्रांति से लेकर चौथी तक वैश्विक शक्ति गतिशीलता को आकार देने में प्रौद्योगिकी प्रमुख प्रेरक शक्ति रही है। आज के युग में, सेमीकंडेक्टपर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां प्रमुख प्रेरक शक्ति हैं। राष्ट्र तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए चिप निर्माण में अरबों रुपए डाल रहे हैं। एआईमें देशों और कंपनियों से समान रूप से बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। साथ ही, साइबर युद्ध और एआईद्वारा उत्पन्न जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साइबर युद्ध पूरे ऊर्जा ग्रिड को बाधित कर सकता है या भुगतान और बैंकिंग प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। एआईद्वारा संचालित भ्रामक सूचना चुनावों को बाधित कर सकते हैं और सामाजिक कलह को जन्म दे सकते हैं। एआईको दुनिया भर के समुदायों द्वारा आकार दिया जाना चाहिए, स्वामित्व में लिया जाना चाहिए और तैनात किया जाना चाहिए। हमें कुशलता से नवाचार करना चाहिए, कम से कम में अधिक करना चाहिए, ओपन सोर्स और सरल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना चाहिए और बहुभाषी और मल्टीमॉडल मॉडल बनाना चाहिए। वैश्विक समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रौद्योगिकी, नुकसान को सीमित करते हुए समावेशी हो। भारत मॉडल, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग विभाजन को बढ़ाने के बजाय उसे पाटने के लिए किया जाता है, दुनिया के लिए एक आदर्श हो सकता है।ऊर्जा की भू-राजनीति और ऊर्जा परिवर्तनस्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव शक्ति गतिशीलता को फिर से परिभाषित कर रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्वों) से समृद्ध राष्ट्र या इन महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को नियंत्रित करने वाले देश अधिक प्रभावशाली बन रहे हैं। आज, लगभग 70-80 प्रतिशत दुर्लभ मृदा तत्वों(आरईई) निष्कर्षण और प्रसंस्करण चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दुनिया के 80 प्रतिशतसौर सेल चीन द्वारा उत्पादित किए जाते हैंऔर इसी तरह लगभग 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी भी चीन द्वारा उत्पादित की जाती हैं। चीन पहले से ही तकनीकी अपनाने के मामले में आगे है, ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो गया है और इसके बजाय वह जीवाश्म ईंधन विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा जोखिम पैदा करता है। विकसित राष्ट्र पहले ही वैश्विक कार्बन बजट का 80 प्रतिशतहिस्सा खर्च कर चुके हैंऔर जी7 देशों से कोयले का चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन अब 2030 के बजाय 2035 तक होगा। इसके अलावा, विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी में विफल हो रहे हैं। इससे विकासशील देशों के लिए अपनी विकास महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत कम जगह बचती है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर हमारी दौड़ को वैश्विक गठबंधनों के नए रूपों की आवश्यकता है। देशों को अगली पीढ़ी के सौर पैनल, इलेक्ट्रोलाइज़र और वैकल्पिक सेल केमिस्ट्री (एसीसी) बैटरी जैसी तकनीक पर सहयोग करना चाहिए। भारत को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अपने घरेलू इकोसिस्टम का निर्माण जारी रखना चाहिए। हमें प्रसंस्करण और शोधन के लिए क्षमताओं का विकास करते हुए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापार साझेदारी भी सुरक्षित करनी चाहिए।बढ़ते वैश्विक संघर्ष के बीच ढहता वैश्विक शासनऐसे समय में जब वैश्विक सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, हमारे पास जो संरचनाएं हैं, वे विफल हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। वैश्विक तापमान पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस के सीमा को पार कर चुका है। ग्लोबल साउथ,अपने प्रतिनिधित्व और अपनी प्राथमिकताओं दोनों के मामले में हाशिये पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गतिरोध बना हुआ है, विश्व व्यापार संगठन में विवाद समाधान तंत्र का अभाव है और कॉप29बहुत जरूरी जलवायु वित्त पोषण प्रदान करने में विफल रहा है। यूक्रेन से लेकर गाजा और सूडान तक, दुनिया भर में संघर्ष बढ़ रहा है। जैसा कि पीएम मोदी ने बार-बार कहा है, जलवायु परिवर्तन, महामारी और वित्तीय अस्थिरता की आज की चुनौतियां राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं देखती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हम पुरानी संस्थाओं के साथ 21वीं सदी की चुनौतियों से नहीं लड़ सकते। एक नए वैश्विक शासन ढांचे की आवश्यकता है जो ग्लोबल साउथको अपने केंद्र में रखे और यह स्वीकार करे कि दुनिया अब कुछ चुनिंदा शक्तियों का क्षेत्र नहीं है। यह क्षण भारत के लिएएक वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक मॉडल को आकार देने और अधिक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की वकालत करने काएक अवसर है।आने वाला दशक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देगा। भारत उभर रहा है और वैश्विक मंच पर एक व्यावहारिक नेता के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है। हम ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने ला रहे हैं जबकि वैश्विक संघर्ष पर एक समझौतावादी रुख अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री का हालिया बयान कि हमें मतभेद के बजाय संवाद पर जोर देना चाहिए, ने वैश्विक स्तर पर एक गूंज पैदा की है। भारत का कूटनीतिक संतुलन इस युग की एक परिभाषित विशेषता बन रहा है।*लेखक भारत के जी20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।
- -लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)जग बनाने पुण्य पावन, प्रेम का विस्तार कर लें ।बाँध लें स्नेहिल पलों को, अक्षयी भंडार कर लें ।।है सुहानी शाम शीतल, भोर भी लगती भली- सी ।प्रिय तुम्हारी बाँह प्यारी, ठौर स्वप्निल सुख गली- सी ।बाग मनहर हो सुवासित, पुष्प घर संसार कर लें ।।आस की किरणें उजाला, भर रही हैं जिंदगी में ।मधुरिमा विश्वास की ले, आस बैठी बंदगी में ।कल्पनाओं को सजा कर, रूप हम साकार कर लें ।।भावनाओं की कलम से, हम लिखें अपनी कहानी ।रागिनी गूँजे मधुरतम, नाद हो पावन रुहानी ।साथ हो अपना हमेशा, ईश का आभार कर लें ।।
- सजल-लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)सृष्टि की रचयिता नारी, उसका मत अपमान करो ।श्रद्धा के पुष्प चढ़ाओ , नारी का सम्मान करो ।।अपना प्रतिरूप बनाकर ,माँ को ईश्वर ने भेजा ।पालन- पोषण वह करती , जग उनका गुणगान करो ।।दया क्षमा का संगम वह , बुद्धि शक्ति की धात्री है ।धैर्य त्याग की मूरत वह , क्षमता की पहचान करो ।।हृदय -सरोवर ममता का , सदा छलकता ही रहता ।नेह- नीर में पीर छुपी , अधरों पर मुस्कान करो ।।भार्या ,भगिनी और सुता , सारे दायित्व निभाती ।आदरणीय हर रूप में ,नारी पर अभिमान करो ।।
- आलेख--अश्विनी वैष्णवलेखक भारत सरकार के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं।महाराष्ट्र के बारामती में एक छोटा किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ कृषि के नियमों को फिर से निर्धारित करने में जुटा है। यह बात अपने-आप में अद्वितीय है। हम उर्वरक के इस्तेमाल में कमी, जल संसाधन के बेहतर इस्तेमाल से अधिक उपज के बारे में बात करते हैं, जो एआई समर्थित है।यह भारत की एआई-संचालित क्रांति की एक झलक मात्र है। तकनीक और नवाचार अब प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को बखूबी बदल रहे हैं। कई अर्थों में इस किसान की कहानी एक बहुत बड़े परिवर्तन का सूक्ष्म रूप है। यह सूक्ष्म रूप 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारे प्रस्थान का है।डिजिटल नियति का निर्धारणभारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), एआई, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर जोर देकर अपने डिजिटल भविष्य को आकार दे रहा है। दशकों से, भारत सॉफ़्टवेयर के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी रहा है, किंतु अब यह हार्डवेयर विनिर्माण में भी बड़ी प्रगति कर रहा है।पांच सेमीकंडक्टर संयंत्र निर्माणाधीन हैं, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हमारे शीर्ष तीन निर्यातों में शुमार हैं और जल्द ही हम एक प्रमुख मील के पत्थर यानी इस साल भारत की पहली “मेक इन इंडिया” चिप के लॉन्च तक पहुंच जाएंगे।एआई का निर्माण: कंप्यूट, डेटा और इनोवेशनसेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी रीढ़ हैं, जबकि डीपीआई भारत की तकनीकी क्रांति को आगे बढ़ाने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। भारत अपने तरह की एक एआई संरचना के माध्यम से इसे सभी के लिए सुलभ बनाकर एआई का लोकतंत्रीकरण कर रहा है।इस संबंध में एक प्रमुख पहल 18,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) के साथ भारत की कॉमन कंप्यूट सुविधा है। 100 रुपए प्रति घंटे से कम की रियायती लागत पर उपलब्ध, यह पहल सुनिश्चित करेगी कि अत्याधुनिक अनुसंधानकर्ताओं, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के लिए सुलभ हो। यह पहल मूलभूत मॉडल और अनुप्रयोगों सहित एआई -आधारित प्रणालियों को विकसित करने के लिए जीपीयू तक आसान पहुंच को सक्षम करेगी।भारत विविध और उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा पर एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर गैर-व्यक्तिगत अनाम डेटासेट भी विकसित कर रहा है। यह पहल पूर्वाग्रहों को कम करने और सटीकता में सुधार करने में मदद करेगी, जिससे एआई सिस्टम अधिक विश्वसनीय और समावेशी बनेंगे। ये डेटासेट कृषि, मौसम पूर्वानुमान और यातायात प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई-संचालित समाधानों को शक्ति प्रदान करेंगे।सरकार भारत के अपने आधारभूत मॉडलों के विकास में सहायता कर रही है, जिसमें बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या-विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं। एआई से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, कई उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।भारत का डीपीआई, डिजिटल नवाचार की रूपरेखाडीपीआई में भारत के अग्रणी कार्य ने वैश्विक डिजिटल परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। कॉर्पोरेट या राज्य-नियंत्रित मॉडल के विपरीत, भारत का सरल सार्वजनिक-निजी दृष्टिकोण का आधार, यूपीआई और डिजीलॉकर जैसे प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करता है। निजी क्षेत्र के दिग्गज डीपीआई के शीर्ष पर उपयोगकर्ता के अनुकूल, एप्लिकेशन-विशिष्ट समाधान बनाते हैं और नवाचार प्रस्तुत करते हैं।इस मॉडल को अब एआई के साथ सुपरचार्ज किया जा रहा है, क्योंकि यूपीआई और डिजीलॉकर जैसे वित्तीय और शासन प्लेटफॉर्म बुद्धिमान समाधानों को एकीकृत करते हैं। भारत की डीपीआई संरचना में वैश्विक रुचि जी20 शिखर सम्मेलन में स्पष्ट थी, जहां विभिन्न देशों ने मॉडल को दोहराने की इच्छा व्यक्त की थी। जापान ने भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है, जो इसकी व्यापकता का प्रमाण है।महाकुंभ, परंपरा और तकनीक का संगमभारत ने महाकुंभ 2025 के निर्बाध संचालन के लिए अपने डीपीआई और एआई-संचालित प्रबंधन का लाभ उठाया, जो अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम है। एआई -संचालित उपकरणों ने प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तत्क्षण रेलवे यात्रियों की आवाजाही की निगरानी की।भाषिणी, कुंभ सहायक चैटबॉट में एकीकृत, सभी के लिए आवाज आधारित खोया और पाया सुविधा, तत्क्षण अनुवाद और बहुभाषी सहायता सक्षम करती है। भारतीय रेल और उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे विभिन्न विभागों के साथ इसके सहयोग ने समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संचार प्रणाली को सुव्यवस्थित किया।डीपीआई का लाभ उठाकर, महाकुंभ 2025 ने तकनीक-सक्षम प्रबंधन के लिए एक वैश्विक मानदंड स्थापित किया है, जो इसे अधिक समावेशी, कुशल और सुरक्षित बनाता है।भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माणभारत का कार्यबल इसकी डिजिटल क्रांति के केंद्र में है। देश हर हफ्ते एक वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) जोड़ रहा है, जो वैश्विक आरएंडआई और तकनीकी विकास के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। हालांकि, इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार, एआई, 5जी और सेमीकंडक्टर डिजाइन को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बदलाव करके इस चुनौती का समाधान कर रही है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्नातक रोजगार के लिए तैयार कौशल के साथ कार्यबल में प्रवेश करें, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच का फासला कम हो।एआई को विनियमित करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोणभारत भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण कर रहा है। इसकी एआई नियामक संरचना को उत्तरदायी तैनाती सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। ‘कठोर’ नियामक संरचना के प्रतिकूल, जो नवाचार को दबाने का जोखिम उठाता है, या ‘बाजार संचालित शासन’, जो अक्सर कुछ लोगों के हाथों में शक्ति केंद्रित करता है, भारत एक व्यावहारिक, तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण का पालन कर रहा है।एआई से संबंधित जोखिमों को दूर करने के लिए केवल कानून पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार तकनीकी सुरक्षा से जुड़े उपायों में निवेश कर रही है। सरकार डीप फेक, गोपनीयता संबंधी सरोकारों और साइबर सुरक्षा के जोखिमों से निपटने के लिए उपकरण विकसित करने के क्रम में शीर्ष विश्वविद्यालयों और आईआईटी में एआई संचालित परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रही है।एआई वैश्विक उद्योगों को नया आकार दे रहा है। इसलिए भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। इसके तहत समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने वाली नियामक संरचना को बनाए रखना होगा, लेकिन नीतियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर से परे, यह परिवर्तन हमारे लोगों के बारे में है।
- -दीक्षा के दोहे-लेखिका-डॉ. दीक्षा चौबे, दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)मंद-मंद बहती हवा, पड़ती ओस फुहार।प्रेम प्रसारित हर हृदय, करती सुख-संचार ।।चंचल चितवन रूपसी, करते नैन कटाक्ष।पाती लेकर प्रेम की, झाँके हृदय-गवाक्ष।।काया कंचन कामिनी, अद्भुत मोहापाश।कदमों में सिमटी धरा, बाँहों में आकाश।।नवाचार का सूर्य ले, ढूँढें नवल वितान।कठिन प्रश्न को हल करें, सोचें सरल विधान।।बोझ नहीं हों पाठ सब, मनरंजन भरपूर।खेल-खेल में सीख दें, मुश्किल कर दें दूर।।
- -लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)बातें सुनना और सुनाना अच्छा लगता है।कभी-कभी खुद में खो जाना अच्छा लगता है ।।फिक्र सदा ही करते आए दुनिया वालों की।अपने को भी कभी मनाना अच्छा लगता है।।जिम्मेदारी के साये में भूल गए बचपन।उन गलियों में दौड़ लगाना अच्छा लगता है।।रेशम से रिश्तों के सारे रेशे हैं उलझे ।धीरे-धीरे सब सुलझाना अच्छा लगता है।।बुजुर्गों की दुआओं से ऐसे कुछ लोग मिले।कड़ी धूप में छाया पाना अच्छा लगता है।।
- लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)जीवन-पथ में चलो चलें हम, हँसते मुस्काते।पार करेंगे हर मुश्किल को, प्रेम गीत गाते।।मोती सच्चे अनमोल बड़े , हैं विश्वासों के ।वक्त-वृक्ष की शाखाओं में, फल हैं साँसों के।पूर्व टूटने के जगती को, खुशियाँ दे जाते ।।जीवन पथ में चलो चलें हम, हँसते मुस्काते ।।डगमग होती तूफानों में, जीवन की नैया ।धरे हाथ पर हाथ नहीं अब, बैठो खेवैया ।धैर्य कुशलता साहस संबल, गुण पार लगाते ।।जीवन पथ में चलो चलें हम, हँसते मुस्काते ।।सपन-पतंगें भरें उड़ानें, सीमा से आगे ।लक्ष्य-प्राप्ति की दृढ संकल्पित, डोरी झट भागे ।पथ से विचलित नहीं खिलाड़ी , अंबर छू पाते ।।जीवन-पथ में चलो चलें हम, हँसते मुस्काते ।।
- लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे- दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)नमन करूँ हे मात शारदे,मुझको नित ही ज्ञान मिले ।कलम करे शुचि कर्म निरंतर ,लेखन को पहचान मिले ।।द्वेष-दंभ छल कलुष भाव से ,अंतस मेरा दूर रहे ।गंगाजल सम निर्मल जीवन ,खुशियों से भरपूर रहे ।बढ़ती रहूँ सत्य के पथ पर ,राह नहीं तूफान मिले ।हृदय बने विशाल सागर सम ,लहरों-सा उत्थान मिले ।।अधरों पर मुस्कान सजाए ,मधुरिम मीठी वाणी हो ।शुभता का उजियारा मन में ,कर्म सदा कल्याणी हो ।स्नेह मिले मुझको अपनों का ,ज्ञानी मित्र सुजान मिले ।सुंदर , सरल , सहज हो जीवन ,कभी नहीं अपमान मिले ।।सुमन सरिस सुरभित सुंदर ,मृदुल मनोहर मन मेरा ।निशिगंधा-सी महकीं रातें ,सुखद प्रात का पग-फेरा ।साहस संबल सदा साथ हो ,प्यार , मान - सम्मान मिले ।क्षणिक सुखद यश-वैभव होते ,भक्ति-शक्ति वरदान मिले ।।





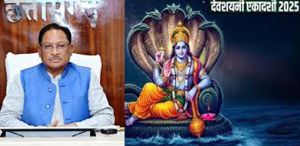


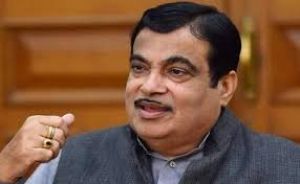













.jpg)









.jpg)
.jpg)



.jpg)








.jpg)
.jpg)
.jpg)




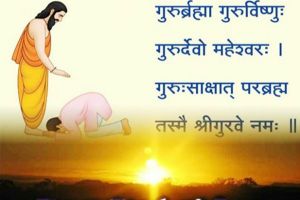












.jpg)

.jpg)
.jpg)